तुम्हारे इतिहासाभिमान और संस्कृति की क्षय
राहुल सांकृत्यायन
राहुल सांकृत्यायन सच्चे अर्थों में जनता के लेखक थे। वह आज जैसे कथित प्रगतिशील लेखकों सरीखे नहीं थे जो जनता के जीवन और संघर्षों से अलग-थलग अपने-अपने नेह-नीड़ों में बैठे कागज पर रोशनाई फि़राया करते हैं। जनता के संघर्षों का मोर्चा हो या सामंतों-जमींदारों के शोषण-उत्पीड़न के खिलाफ़ किसानों की लड़ाई का मोर्चा, वह हमेशा अगली कतारों में रहे। अनेक बार जेल गये। यातनाएं झेलीं। जमींदारों के गुर्गों ने उनके ऊपर कातिलाना हमला भी किया, लेकिन आजादी, बराबरी और इंसानी स्वाभिमान के लिए न तो वह कभी संघर्ष से पीछे हटे और न ही उनकी कलम रुकी।
दुनिया की छब्बीस भाषाओं के जानकार राहुल सांकृत्यायन की अद्भुत मेधा का अनुमान इस बात से भी लगाया जा सकता है कि ज्ञान-विज्ञान की अनेक शाखाओं, साहित्य की अनेक विधाओं में उनको महारत हासिल थी। इतिहास, दर्शन, पुरातत्व, नृतत्वशास्त्र, साहित्य, भाषा-विज्ञान आदि विषयों पर उन्होंने अधिकारपूर्वक लेखनी चलायी। दिमागी गुलामी, तुम्हारी क्षय, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दर्शन-दिग्दर्शन, मानव समाज, वैज्ञानिक भौतिकवाद, जय यौधेय, सिंह सेनापति, दिमागी गुलामी, साम्यवाद ही क्यों, बाईसवीं सदी आदि रचनाएं उनकी महान प्रतिभा का परिचय अपने आप करा देती हैं।
राहुल जी देश की शोषित-उत्पीड़ित जनता को हर प्रकार की गुलामी से आजाद कराने के लिए कलम को हथियार के रूप में इस्तेमाल करते थे। उनका मानना था कि ”साहित्यकार जनता का जबर्दस्त साथी, साथ ही वह उसका अगुआ भी है। वह सिपाही भी है और सिपहसालार भी।“
राहुल सांकृत्यायन के लिए गति जीवन का दूसरा नाम था और गतिरोध मृत्यु एवं जड़ता का। इसीलिए बनी-बनायी लीकों पर चलना उन्हें कभी गंवारा नहीं हुआ। वह नयी राहों के खोजी थे। लेकिन घुमक्कड़ी उनके लिए सिर्फ़ भूगोल की पहचान करना नहीं थी। वह सुदूर देशों की जनता के जीवन व उसकी संस्कृति से, उसकी जिजीविषा से जान-पहचान करने के लिए यात्रएं करते थे।
समाज को पीछे की ओर धकेलने वाले हर प्रकार के विचार, रूढ़ियों, मूल्यों-मान्यताओं-परम्पराओं के खिलाफ़ उनका मन गहरी नफ़रत से भरा हुआ था। उनका समूचा जीवन व लेखन इनके खिलाफ़ विद्रोह का जीता-जागता प्रमाण है। इसीलिए उन्हें महाविद्रोही भी कहा जाता है। जनता के ऐसे ही सच्चे सपूत महाविद्रोही राहुल सांकृत्यायन की एक पुस्तिका ‘तुम्हारी क्षय’ बिगुल के पाठकों के लिए हम धारावाहिक रूप से प्रकाशित कर रहे हैं। राहुल की यह निराली रचना आज भी हमारे समाज में प्रचलित रूढ़ियों के खिलाफ़ समझौताहीन संघर्ष की ललकार है। -सम्पादक
‘इतिहास’-‘इतिहास’ – ‘संस्कृति’-‘संस्कृति’ बहुत चिल्लाया जाता है। मालूम होता है, इतिहास और संस्कृति सिर्फ मधुर और सुखमय चीजें थीं। पचीसों बरस का अपने समाज का तजरबा हमें भी तो है। यही तो भविष्य की सन्तानों का इतिहास बनेगा? आज जो अन्धेर हम देख रहे हैं, क्या हजार साल पहले वह आज से कम था? हमारा इतिहास तो राजाओं और पुरोहितों का इतिहास है जो कि आज की तरह उस जमाने में भी मौज उड़ाया करते थे। उन अगणित मनुष्यों का इस इतिहास में कहाँ जिक्र है जिन्होंने कि अपने खून के गारे से ताजमहल और पिरामिड बनाये; जिन्होंने कि अपनी हड्डियों की मज्जा से नूरजहाँ को अतर से स्नान कराया, जिन्होंने कि लाखों गर्दनें कटाकर पृथ्वीराज के रनिवास में संयोगिता को पहुँचाया? उन अगणित योद्धाओं की वीरता का क्या हमें कभी पता लग सकता है जिन्होंने कि सन् सत्तावन के स्वतन्त्रता-युद्ध में अपनी आहुतियाँ दीं? दूसरे मुल्क के लुटेरों के लिए बड़े-बड़े स्मारक बने, पुस्तकों में उनकी प्रशंसा का पुल बाँधा गया। गत महायुद्ध में ही करोड़ों ने कुर्बानियाँ दीं, लेकिन इतिहास उनमें से कितनों के प्रति कृतज्ञ है?
इतिहास हमारे समाज की पुरानी बेड़ियों को मजबूत करता है। इतिहास हमारी मानसिक स्वतन्त्रता का सबसे बड़ा शत्रु है। इतिहास हमारी पुरानी दुश्मनी और अनबनों को ताजा करता रहता है। सहस्राब्दियों से मनुष्यता का घोर शत्रु सिद्ध हुआ धर्म, बहुत कुछ इतिहास के आधार पर टिका है। विश्वामित्र हों चाहें वशिष्ठ, मनु हों चाहे याज्ञवल्क्य, व्यास हों चाहे पतंजलि, नानक हों चाहे कबीर, मूसा हों चाहे ईसा – सभी पचासों बरस इस धरती पर जीते रहे। न जाने कितनों के दिल को उन्होंने दुखाया होगा, न जाने कितनों के हक को छीना होगा, न जाने कितने दास-दासी खरीदकर जिन्दगी भर उनसे पशु की तरह काम लेते रहे होंगे। अपने मालिकों और अन्नदाताओं की चापलूसी में जाने क्या-क्या कुकर्म उन्होंने किये होंगे। सफल लुटेरों और खूनियों को आसमान पर चढ़ाने की जो प्रवृत्ति देखी जाती है, उससे मालूम होता है कि इतिहास की वीरपूजा में भी इसका बहुत बड़ा अंश रहा होगा।
हिन्दुओं के इतिहास में राम का स्थान बहुत ऊँचा है। आजकल के हमारे बड़े नेता, गाँधीजी, मौके-ब-मौके रामराज्य की दुहाई दिया करते थे। वह रामराज्य कैसा होगा जिसमें कि बेचारे शूद्र शम्बूक का सिर्फ यही अपराध था कि वह धर्म कमाने के लिए तपस्या कर रहा था और इसके लिए राम जैसे अवतार और धर्मात्मा राजा ने उसकी गर्दन काट ली? वह रामराज्य कैसा रहा होगा जिसमें किसी आदमी के कह देने मात्र से राम ने गर्भिणी सीता को जंगल में छोड़ दिया? रामराज्य में दास-दासियों की कमी न थी। अट्ठारहवीं-उन्नीसवीं सदी तक दुनिया में दास-प्रथा कितनी क्रूरता के साथ प्रचलित थी, इसका हमें काफी ज्ञान है। उस वक्त स्वेच्छापूर्वक अपने को और अपनी सन्तान को बेचा ही नहीं जाता था, बल्कि समुद्र और बड़ी नदियों के किनारे के गाँवों में तो आदमियों को पकड़ ले जाने के लिए बाकायदा हमले हुआ करते थे। डाकू गाँव पर छापा मारते थे और धन के साथ-साथ वहाँ के काम करने लायक आदमियों को पकड़ ले जाते थे। हर साल हजारों इस तरह के गुलाम पोर्तुगीज डाकू पकड़कर बर्मा के अराकन प्रदेश में बेचा करते थे। रामराज्य में यदि इस तरह की लूट और डाकेजनी न रही होगी तो दास-प्रथा तो जरूर ही थी। अभी दस ही बारह साल हुए हैं जबकि हिन्दुओं के अभिमान की जगह नेपाल राज ने अपने यहाँ दास-प्रथा का अन्त किया। मिथिला में अब भी कितने घरों में वे कागज हैं जिनमें बहिया (दास) के क्रय-विक्रय दर्ज हैं। दरभंगा जिले के तरौनी गाँव (थाना बहेड़ा) में दिगम्बर झा के परदादा ने कुल्ली मँड़र के दादा को किसी दूसरे मालिक से खरीदा था और दिगम्बर झा के दादा ने पचास रुपये के फायदे के साथ उसे बेच दिया। अभी तीन ही पीढ़ी पहले अंग्रेजी राज तक में यह प्रथा मौजूद थी और सच्चे धार्मिक हिन्दू हों चाहे मुसलमान, दोनों जब अपनी मनुस्मृतियों और हदीसों में दासों के ऊपर मालिकों के हक के बारे में पढ़ते हैं तो उनके मुँह में पानी भर आये बिना नहीं रहता।
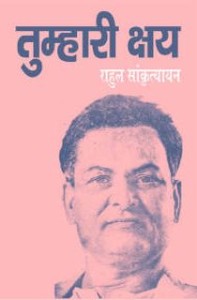
राहुल फाउण्डेशन, लखनऊ द्वारा राहुल का ये संकलन एक पुस्तिका की शक्ल में भी प्रकाशित हुआ है जिसे इस लिंक से खरीदा जा सकता है – http://janchetnabooks.org/product/tumhari-kshay/
आइये, रामराज्य की दास-प्रथा की एक झाँकी लीजिये। एक साधारण बाजार है जिसमें सिर्फ दास-दासियों की बिक्री होती है। लाखों वृक्षों का बाग है। खाने-पीने की चीजों की दूकानें सजी हुई हैं। भेड़-बकरियों और शिकार किये जानवरों के अतिरिक्त उच्च वर्ण के आर्यों के भोजन तथा मधुपर्क के लिए गोमांस खास तौर से तैयार करके बेचा जा रहा है। जगह-जगह सफेद दाढ़ी वाले ऋषि, दूसरे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य अपने पड़ाव डाले पड़े हुए हैं। कोई नया दास या दासी खरीदने आया है। किसी के दिन कुछ बिगड़ गये हैं, इसलिए वह अपने दासों या दासियों को बेचकर कुछ नकद जमा करना चाहता है। कुछ सिर्फ इस खयाल से अपने दास-दासियों को मेले में लाये हैं कि उन्हें बेच कर ‘नया’ कर लिया जाये। कुछ बड़े व्यापारी ऐसे भी हैं जो झटपट बेचकर चले जाने की इच्छा रखने वालों की आसानी के लिए सस्ते में दास-दासी खरीद लेते हैं और अधिक मुनाफे के साथ बेचते हैं। स्वामियों ने महीनों पहले मेले में चलने का निश्चय कर लिया था। उन्होंने अपने दास-दासियों को खूब अच्छा खाना देना शुरू किया था जिसमें कि मांस और चर्बी से उनकी हड्डियाँ ढक जायें और बाजार में अधिक दाम आ सके। उनके सफेद बालों को काला रंगा गया है और मेले में कपड़े-लत्ते से अच्छी तरह सँवारकर उनकी हाट लगायी गयी है। कहीं-कहीं आदमी अपने एकाध दास या दासी को लेकर बैठे हैं और कहीं-कहीं सौ-सौ, दो-दो सौ की पाँत लगी हुई है। खरीदारों की भीड़ है। खरीदने वाले कहते हैं – अबकी बाजार बहुत महँगा रहा, पिछले साल अठारह बरस की हट्टी-कट्टी सुन्दरी दासी दस रुपये में मिल जाती थी, अबकी बार तो तीस में भी हाथ धरने नहीं देते। एक आदमी को दासी खरीदनी है, लेकिन पैसे उसके पास कम हैं। वह एक चालीस बरस के सौदे के पास पहुँचता है। दासी के तिहाई बाल यद्यपि सफेद हो गये थे, लेकिन उन्हें रँगकर काला किया था। मालिक की खुशकिस्मती समझिए कि दासी के दाँत सभी मजबूत थे। खरीदार ने पास जाकर उसके दाँत देखे – बिल्कुल दुरुस्त। आँखों देखीं – कोई फर्क नहीं। कान देख-सुन सकती है। हाथों को उठा और ठोंक कर देखा – कमजोर नहीं है। चलाकर देखा – पैर भी दुरुस्त हैं। पूछा – “वाशिष्ठ जी! आपकी दासी बूढ़ी तो हो गयी है। लेकिन खैर, हमारे यहाँ काम हल्का है; बतलाइये तो मूल्य क्या है?”
वाशिष्ठ – “गौतमजी, आप गलत कह रहे हैं। अभी तो यह बीस बरस की छोकरी है। आपने देखा नहीं कि इसके हाथ पैर कितने मजबूत हैं, कितनी सुन्दरी है; दस साल में दस तो इसके लड़के पैदा हो जायेंगे। दूना दाम तो एक ही लड़के से निकल आयेगा। हम आपसे मोल-भाव करना नहीं चाहते। पचास रुपया हमें मिल रहा था। खैर, आप परिचित हैं, आपको दस रुपया कम करके दे देंगे।”
गौतम – “आप तो बहुत कड़ा दाम माँग रहे हैं। बालों को काला कर देने और दो महीने के खिलाने-पिलाने से— यह न समझिये कि मैं नहीं जानता— यह पचास साल की बूढ़ी है। मुझे हल्का सौदा लेना है, यदि आप दाम-काम ठीक करें तो इसे ले लूँ।”
वाशिष्ठ – “आप मेले के दूसरे आदमियों की तरह मुझे भी समझ रहे हैं? इसी की बहन को मैंने सौ रुपये में अयोध्या के महाराज रामचन्द्र के लिए बेचा है। आजकल महाराज यज्ञ कर रहे हैं, दक्षिण में वह हर एक ऋषि को एक-एक तरुण सुन्दरी दासी देना चाहते हैं। देखा नहीं, इस साल दासियों का भाव बहुत चढ़ गया है? अच्छा जाइये, तीस ही रुपये दे दीजिये; हमें भी घर लौटने की जल्दी है। यह दासी ऐसी-वैसी नहीं है, यह खूब नाचना-गाना जानती है। काली! जरा एक गीत तो सुना दे।”
काली ने एक गीत सुनाया और नाच के भी एक-दो तर्ज दिखलाये। अन्त में पन्द्रह रुपये पर सौदा पटा।
लोग अपने-अपने दासों को घर ले जा रहे हैं। कितनी दासियों के बच्चे बिककर सैकड़ों कोस दूर पहुँच गये हैं। कितनों के प्रेमी हमेशा के लिए छूट गये हैं। बच्चों और प्रेमियों के इस बिछोह के कारण किसी काम में उनका मन नहीं लग रहा है और नये मालिक उनसे काम लेने को उकता रहे हैं। दो-चार दिन जो नरमी देखी गयी, उसे खत्म करके अब जरा-जरा-सी शिकायत पर – दासियों पर कोड़े पड़ रहे हैं। दासों की जान तक मार डालने में मालिकों को कोई जबर्दस्त सजा पाने का भय नहीं है। मालिक उनके प्रति वही खयाल रखते हैं जो कि अपने पशुओं के लिए।
यह है रामराज्य में मनुष्यों के एक भाग का जीवन! और, यह है रामराज्य में मनुष्य का मोल! इसी पर हमको नाज है! ऋषियों की दया और सहृदयता का गुण गाते तो हम थकते नहीं जिन ऋषियों के आश्रमों के आस-पास मनुष्य इस प्रकार गुलाम बनाकर रखे जाते थे, जिन ऋषियों को स्वर्ग, वेदान्त और ब्रह्म पर बड़े-बड़े व्याख्यान और सत्संग करने की फुर्सत थी जो दान और यज्ञ पर बड़े-बड़े पोथे लिख सकते थे, क्योंकि इससे उनको और उनकी सन्तानों को फायदा था, परन्तु मनुष्यों के ऊपर पशुओं की तरह होते इन अत्याचारों को आमूल नष्ट करने के लिए उन्होंने किसी तरह के प्रयत्न की आवश्यकता न समझी। उन ऋषियों से आज के जमाने के साधारण आदमी भी मानवता के गुण से अधिक भूषित हैं।
संस्कृति का अंग कला है। कला में हमने कहाँ तक सारे समाज का खयाल रखा और पुराने जमाने में भी साधारण जनता उससे फायदा उठा सकती थी? सहस्राब्दियों से संगीत राजाओं और धनियों की कामुकता को उत्तेजित करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। संगीत की रुचि मनुष्य में स्वाभाविक होती है। सभ्यता के निम्न तल पर रहने वाली जातियों से लेकर सभ्यता के उत्कर्ष की चोटी तक पहुँची हुई जातियों तक सभी में नृत्य का प्रेम देखा जाता है। लेकिन यह हमारा ही देश है जो कि सभ्य कहलाने में दुनिया के सभी देशों से अपने को पहले रखना चाहता है; लेकिन इन दोनों ललित कलाओं को ऐसी निम्न श्रेणी में डाल रखा है कि जिनकी दुनिया में मिसाल नहीं। इंग्लैण्ड, अमेरिका और जापान के सुशिक्षित परिवार संगीत और नृत्य-कला को अपने सभ्य जीवन का एक अंग समझते हैं, लेकिन ये चीजें हमारे यहाँ वेश्याओं के लिए रख छोड़ी गयी हैं। इस श्रेणी के कारण संगीत और नृत्य-कलाएँ सम्भ्रान्त कुल की स्त्रियों से बहिष्कृत समझी जाती हैं।
हम संस्कृत हैं, हम सभ्य हैं – इस तरह अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनने से दुनिया हमें सभ्य नहीं मानेगी। हमारे जीवन का हर एक अंग जिस तरह कलुषित और दिखावट से भरा हुआ है, उस तरह की जाति दुनिया में शायद ही कोई हो। अभी तक तो हमने आदमी की तरह रहना भी नहीं सीखा। पास-पड़ोस की सफाई की अवहेलना में तो हम जानवरों से भी गये-बीते हैं। हिन्दुस्तान के गाँवों जैसे गन्दे गाँव दुनिया के किसी भी देश में खोजने से नहीं मिलेंगे। यह हमारे ही गाँव की खूबी है कि एक अन्धा आदमी भी एक मील पहले से ही हमारे गाँव को पहचान लेता है, जबकि उसकी नाक पाखाने की बदबू से फटने लगती है। सफाई के लिए अपने को लासानी समझने वाले हमारे देश के हिन्दू-मुसलमान पाखाने के लिए किसी प्रबन्ध की कोई जरूरत नहीं समझते। गाँव के पड़ोस के खेत तो इसके लिए हैं ही। कोई भी विदेशी जो एक बार हिन्दुस्तानी गाँव से गुजर जायेगा और पास के खेतों में अलग-अलग फैले हुए हवा और धूप में सूखते पाखानों को देखेगा, वह कैसे समझेगा कि हिन्दुस्तान में आदमी रहते हैं। एक बार मेरे एक जापानी मित्र को, जिनके स्नेहपूर्ण आतिथ्य को पाने का मुझे कई दिनों तक मौका मिला था, भारत आने के लिए लिखा। उन्होंने भी यह इच्छा प्रकट की थी कि मैं भारत के ग्रामीण जीवन को नजदीक से देखना चाहता हूँ। मुझे पत्र पाकर यह चिन्ता हुई कि किन गाँवों में मैं अपने मित्र को ले जाऊँ। सबसे बड़ी दिक्कत मुझे पाखाने और नहाने की मालूम पड़ती थी। हिन्दुस्तान के गाँवों में खुले खेतों के अतिरिक्त पाखाने का कोई इन्तजाम नहीं। गाँव ही क्या, शहर में भी पचास हजार लगाकर महल बनाने वाले पाखाने के लिए पचास रुपये का “सेप्टिक टैंक” लगाना दण्ड समझते हैं। गुसलखाना तो अंग्रेजों और क्रिस्तानों की चीज है। मेरे तरद्दुत को देखकर एक मित्र ने अपने यहाँ खास तौर से पाखाने और गुसलखाने तैयार करने का इरादा जाहिर किया। खैर, मेरे जापानी मित्र ने अपनी यात्रा स्थगित कर दी। लेकिन पत्र को पाकर जिस फिक्र में मैं महीनों रहा, उससे मुझे यह तो मालूम हो गया कि हम लोग कितने पानी में हैं। मुझे आश्चर्य होता है कि हमारे पूर्वजों ने स्वच्छता के लिए अत्यन्त आवश्यक इन चीजों की ओर क्यों नहीं ध्यान दिया? बल्कि जो ध्यान दिया भी है तो उल्टा; जिससे स्वच्छता में और बाधा पड़ती है। पाखाना उठानेवाले को हमारे देश में सबसे नीच समझा जाता है। अभी तो उन जातियों को हमने आर्थिक चक्की से पीस रखा है और पेट के आगे उन्हें इज्जत-आत्मसम्मान का खयाल ही नहीं आता। लेकिन किसी-न-किसी दिन वह आवेगा जरूर। फिर समाज की इस सबसे बड़ी सेवा के लिए सबसे जबर्दस्त लाँछना को सहने के लिए वे कैसे तैयार होंगे? और, यदि उन्होंने पाखाना साफ करना छोड़ दिया तो चन्द ही दिनों में क्या हमारे महल सूने नहीं हो जायेंगे? इंग्लैण्ड में चले जाइये, वहाँ जो व्यक्ति रसोई बनाता है, वह पाखाने में भी झाड़ू दे देता है। जापान में देखिये, वहाँ तो पाखाना बेचने वाले कितने सम्भ्रान्त व्यापारी हैं। किसी को पाखाना उठाने में घृणा नहीं है। हमारी दुनिया ही न्यारी है।
हर एक उपयोगी नयी चीज को ग्रहण करने में हम अपनी संस्कृति और सभ्यता की दुहाई देने लगते हैं। हैट, कोट, पतलून को देखकर हमारे कितने ही लोग नाक-भौं सिकोड़ते हैं। वित्त से अधिक खर्च करने का जहाँ तक सवाल है, वहाँ तक हम कुछ नहीं कहते; किन्तु ढीली-ढाली धोती या लम्बे-चौड़े सलवार क्या काम करने वाले आदमी के लिए उपयुक्त हो सकते हैं? अधबहियाँ कुर्ता, जाँघिया और सोला हैट (मोटा टोप) काम करने के लिए सबसे उपयुक्त पोशाक है। धूप से बचाने के लिए सोला हैट बड़े काम की चीज है। इन चीजों को पश्चिमी यूरोपीय या क्रिस्तानी कहकर हम दुत्कारते हैं। लेकिन क्या मालूम नहीं कि न ये पश्चिमी हैं, न यूरोपीय हैं और न क्रिस्तानी। दो सौ बरस पहले अंग्रेजों के पूर्वज भी सिर पर झोंटा रखते थे। उनकी पोशाक भी ऊल-जलूल थी। आधुनिक पोशाक पिछले दो सौ वर्षों के चिन्तन और परिवर्तन का परिणाम है। अभी महायुद्ध के आरम्भ तक यूरोप की स्त्रियाँ बड़े-बड़े बाल रखती थीं। उनकी पोशाक में आज से कई गुना ज्यादा कपड़ा लगता था। कमर अस्वाभाविक तौर पर कसकर पतली बनायी जाती थी। आज यूरोप की स्त्रियों ने बाल कटा लिए हैं, उनकी पोशाक हल्की हो गयी है। कमर पतली करने की वह पुरानी सनक अब उनमें नहीं रही।
स्त्री-पुरुष का ब्याह किसलिए होता है? सन्तान ही उसमें मुख्य बात नहीं है। अव्वल तो हमारे यहाँ विवाह का भार जबर्दस्ती माँ-बाप अपने ऊपर लेना चाहते हैं। सन्तान इसमें दस्तन्दाजी न करे, इसलिए बचपन में ही विवाह कर देना चाहते हैं। यह भी हमारी संस्कृति का एक बहुत ‘उज्ज्वल’ अंग है कि जिन्हें सारी जिन्दगी एक-दूसरे के साथ बितानी है, उन्हें एक-दूसरे की प्रकृति और दिलचस्पी से परिचय प्राप्त करने का मौका बिना दिये हमेशा के लिए गले में बाँध दिया जाये। इस तरह की स्वेच्छाचारिता ने लाखों पारिवारिक जीवनों को नरक के रूप में परिणत कर दिया है, तो भी कोई इससे शिक्षा लेने को तैयार नहीं है। माता-पिता विवाह कर देते हैं, लेकिन विवाहित जोड़े के लिए समाज की सख्त हिदायत है कि कम-से-कम जवानी भर वे एक-दूसरे से खुले तौर पर न मिलें। दुनिया के सभी भागों में विवाहित स्त्री-पुरुष की अलग चारपाई नहीं होती। वहाँ चारपाई अलग होने का मतलब है तलाक की तैयारी। लेकिन हमारे यहाँ तो चारपाई ही अलग नहीं, सोने की जगह भी अलग होनी चाहिए और शिष्टता का तकाजा है कि पति घर वालों की जानकारी में पत्नी के पास न जाये। विवाहित पुरुष अपनी पत्नी को अपने साथ नहीं रख सकता। चाहे वर्षों नौकरी या व्यापार में दूर-दूर रहना पड़े तो भी इस तरह की स्वतन्त्रता को शिष्टाचार के विरुद्ध समझा जाता है।
सारांश यह कि जिस अपने इतिहास और संस्कृति का अभिमान हम करते हैं, वह हमें साधारण मनुष्य-जैसा जीवन भी बिताने देना नहीं चाहती। खान-पान, रहन-सहन, शादी-ब्याह, स्वास्थ्य-सफाई और भाईचारा – सभी में वह हमें दुनिया की नजर में जलील बनाना चाहती है। हमारे लिए सबसे अच्छा यही है कि अपने इतिहास को फाड़कर फेंक दें और संस्कृति से अपने को वंचित समझकर दुनिया की और जातियों से फिर क, ख पढ़ना सीखें।















