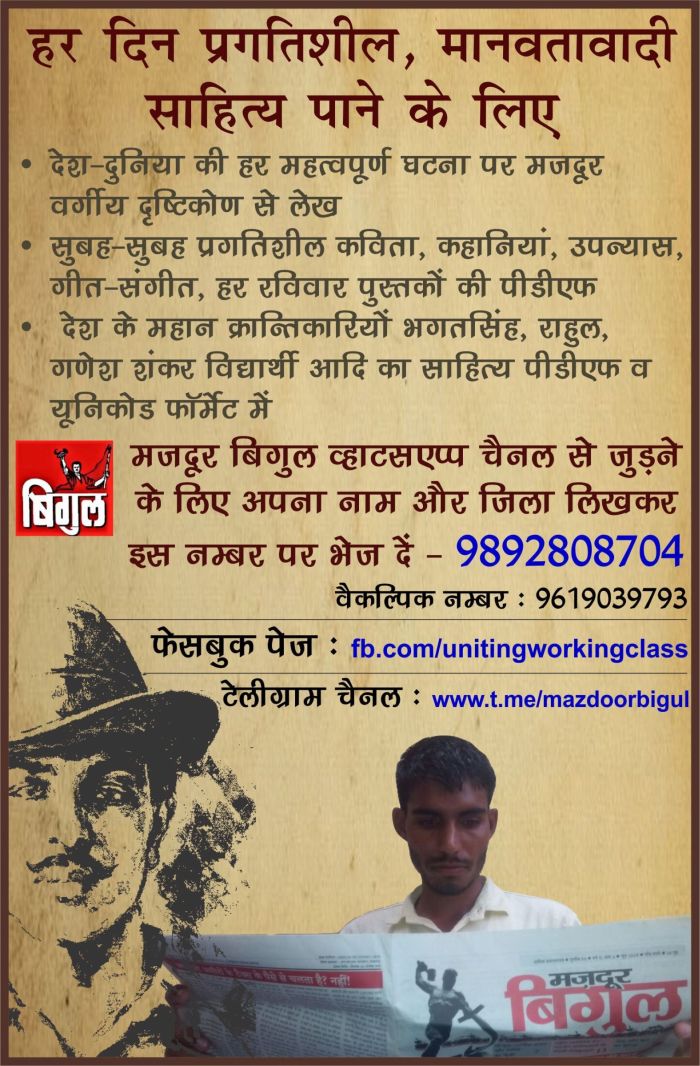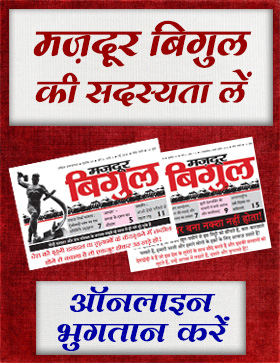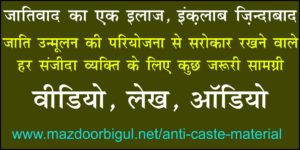मज़दूर वर्ग की पार्टी कैसी हो? (सातवीं किस्त)
सनी
इस लेखमाला की सभी किश्तें इस लिंक से पढें
एंगेल्स के अनुसार “हर सिद्धान्त…पहले अपने समक्ष उपलब्ध बौद्धिक सामग्री से ही जुड़ता है चाहे वह खुद कितना ही आर्थिक तथ्यों पर आधारित क्यों न हो।” मार्क्स-पूर्व समाजवादी सिद्धान्त फ़्रांसिसी क्रान्ति और प्रबोधन काल की वैचारिक सामग्री पर आधारित थे। मज़दूर वर्ग ने भी अपनी शैशवावस्था में समाजवाद के उन शैशव सिद्धान्तों को ही अपनाया जो उसके समक्ष उपलब्ध थे। कम्युनिस्ट घोषणापत्र के छपने से पहले वैज्ञानिक समाजवाद की जगह काल्पनिक समाजवाद की कई क़िस्मों का मिला-जुला खिचड़ी समाजवाद इंग्लैंड और फ़्रांस के मज़दूरों के मस्तिष्कों पर हावी था।
1840 के दशक के मध्य तक मार्क्स-एंगेल्स द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और ऐतिहासिक भौतिकवाद तक पहुँच चुके थे और काल्पनिक समाजवाद की बहुधा क़िस्मों की आलोचना कर वैज्ञानिक समाजवाद पेश कर रहे थे। यह दौर मार्क्स-एंगेल्स के क्रान्तिकारी व्यवहार के पहले प्रयोगों का भी दौर है जिसमें उन्होंने मज़दूर वर्ग के संगठन पर तथा उसकी रणनीति और आम रणकौशल पर भी कुछ बुनियादी अवधारणाएँ रखीं। मार्क्स और एंगेल्स अपने विचारों के इर्द-गिर्द मज़दूर वर्ग को संगठित करने के प्रयास के क्रम में ‘लीग ऑफ़ जस्ट’ से जुड़ते हैं और उसे ‘कम्युनिस्ट लीग’ में बदलते हैं।
मज़दूर वर्ग के संगठन के बारे में मार्क्स–एंगेल्स के विचारों का सन्दर्भ समझने के लिए हमें इस दौर की राजनीतिक परिस्थिति, मज़दूर वर्ग के आर्थिक विकास तथा समाजवाद के सिद्धान्त के विकास का अवलोकन करना चाहिए। मज़दूर वर्ग ने फ़्रांस में जून 1848 में पहली बार सत्ता पर धावा बोला हालाँकि वह पराजित हुआ। यूरोप के अन्य शहरों, बर्लिन, विएना और मिलान में भी विद्रोह भड़क उठा परन्तु अंततः पराजय में ही तब्दील हुआ। इस पराजय का समाहार करते हुए एंगेल्स लिखते हैं कि:
“जब फ़रवरी क्रान्ति भड़की, तब जहाँ तक क्रान्तिकारी आन्दोलनों की अवस्थाओं और प्रक्रम के बारे में हमारी धारणाओं का प्रश्न था, हम सब के मन पर पहले का ऐतिहासिक अनुभव, विशेषतः फ्रांस का अनुभव छाया हुआ था। वास्तव में 1789 से पूरा यूरोपीय इतिहास फ्रांस के अनुभव से आच्छन्न रहा था, और अब फिर इसी देश ने आम क्रान्तिकारी रद्दोबदल के लिए बिगुल बजाया था। इसलिए यह स्वाभाविक तथा अनिवार्य था कि पेरिस में फ़रवरी 1848 में घोषित “सामाजिक” क्रान्ति के, सर्वहारा की क्रान्ति के स्वरूप तथा प्रक्रम के बारे में हमारी धारणाएँ 1789 तथा 1830 के प्राक्-रूपों की स्मृतियों से प्रबल रूप से प्रभावित हों। इसके अलावा जब पेरिस का विद्रोह वियेना, मिलान और बर्लिन के विजयी विद्रोहों में प्रतिध्वनित हुआ, जब ऐन रूस की सरहद तक पूरा यूरोप आन्दोलन की लपेट में आ गया, जब इसके बाद जून में पेरिस में सत्ता के लिए सर्वहारा और पूँजीपति वर्ग की पहली लड़ाई लड़ी गयी; जब सभी देशों का पूँजीपति वर्ग स्वयं अपने वर्ग की विजय से इतना दहल गया कि उसने भाग कर राजतन्त्रवादी-सामन्ती प्रतिक्रियावाद का दामन पकड़ा, जिसका तख़्ता अभी हाल में उलटा गया था-तब उस वक़्त की परिस्थितियों में हम इस बात में सन्देह न कर सकते थे कि महान निर्णायक लड़ाई शुरू हो गयी है, कि यह लड़ाई क्रान्ति के एक ही लम्बे, उतार-चढ़ाव वाले काल में लड़नी होगी, पर अन्त में उसकी परिणति सर्वहारा की अन्तिम विजय में ही हो सकती है।
“उस समय यूरोपीय महाद्वीप में आर्थिक विकास की जो अवस्था थी, वह पूँजीवादी उत्पादन के निराकरण के लिए बहुत परिपक्व न थी; इतिहास ने यह उस आर्थिक क्रान्ति के द्वारा प्रमाणित किया है, जिसने 1848 से पूरे यूरोपीय महाद्वीप को अपनी लपेट में ले लिया है और जिसके फलस्वरूप बड़े पैमाने के उद्योग ने फ्रांस, आस्ट्रिया, हंगरी, पोलैण्ड और हाल में रूस में सचमुच जड़ पकड़ ली है, जबकि उसकी बदौलत जर्मनी निश्चय ही प्रथम कोटि का औद्योगिक देश बन गया है और यह सब हुआ है पूँजीवादी आधार पर, जिसमें फलतः 1848 में अभी भी विस्तरण की प्रचुर क्षमता मौजूद थी। लेकिन ठीक यही औद्योगिक क्रान्ति है जिसने वर्ग सम्बन्धों को सर्वत्र स्पष्ट किया है, मैन्युफैक्चर के युग से चले आते हुए और पूर्वी यूरोप में तो शिल्प-संघ के युग से चले आते हुए कई मध्यवर्ती रूपों को मिटा दिया है, असली पूँजीपति वर्ग को और असली, बड़े पैमाने के उद्योग-धन्धों में काम करने वाले सर्वहारा को जन्म दिया है और उन्हें खींचकर सामाजिक विकास के मंच पर पहुँचा दिया है। परन्तु इसी कारण इन दो महान वर्गों का संघर्ष, जो 1848 में इंग्लैण्ड को छोड़कर केवल पेरिस में और अधिक से अधिक कतिपय बड़े औद्योगिक केन्द्रों में चलता था, पूरे यूरोप में फैल गया है और उसमें ऐसी तेज़ी आ गयी है जो 1848 में अकल्पनीय थी। उस जमाने में अलग-अलग सम्प्रदायों के कितने ही ज्ञात-अज्ञात उपदेशक थे, अपने-अपने रामबाणी नुस्खे लिये हुए; आज मार्क्स का एक ही सामान्यतः स्वीकृत स्फटिक की तरह उज्ज्वल सिद्धान्त है, जिसमें संघर्ष के चरम लक्ष्यों को तीखे रूप में सूत्रबद्ध किया गया है।”
आधुनिक उद्योग के साथ सर्वहारा वर्ग इतिहास के रंग-मंच पर प्रवेश कर चुका था, हालाँकि 1848 की क्रान्ति तक इसका पश्चिमी यूरोप में रंग-मंच पर प्रमुख भूमिका में आना बाक़ी था। दूसरी तरफ़ “अलग-अलग सम्प्रदायों के कितने ही ज्ञात-अज्ञात उपदेशक” और उनके “अपने-अपने रामबाणी नुस्खे” यानी काल्पनिक समाजवाद की कई धाराएँ मज़दूरों के बीच मौजूद थी। केवल उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्ध में इतिहास ने एक तरफ़ सर्वहारा वर्ग को इतिहास के रंग मंच पर प्रमुख भूमिका में ला खड़ा किया, तो दूसरी तरफ़ मार्क्सवादी विचारधारा ने मज़दूर वर्ग के उन्नत तत्वों के बीच अपना प्राधिकार जमा लिया। इस प्रक्रिया में ही सर्वहारा वर्ग के संगठन के रूप में कम्युनिस्ट पार्टी की अवधारणा जन्मी जिसका पहला रूप कम्युनिस्ट लीग थी।
कम्युनिस्ट लीग के इतिहास को समझने से पहले हम पश्चिमी यूरोप में मज़दूर वर्ग के उद्भव और विकास तथा समाजवाद की सिद्धान्तिकी पर एक निगाह डाल लेते हैं। फ्रांसीसी क्रान्ति और 1848 के कालखण्ड में पश्चिम यूरोप के सभी देश औद्योगिक क्रान्ति के प्रभाव में बदले। हालाँकि छोटे पैमाने के उत्पादन का बड़े पैमाने के उत्पादन द्वारा विस्थापन इंग्लैण्ड की तुलना में पूरे महाद्वीप पर सापेक्षिक तौर पर काफ़ी कम हुआ था। स्वचालित मशीनरी एक-एक कर हर उद्योग में प्रवेश कर रही थी। मैनचेस्टर, लंकाशायर, यॉर्कशायर, लिवरपूल, लन्दन, पेरिस और ल्योन सरीखे औद्योगिक शहर खड़े हो रहे थे। मशीनरी और बड़ी फैक्ट्रियों के उद्भव तथा पूँजीवाद के कृषि में प्रवेश के साथ हर देश में वर्ग शक्ति समीकरण बदलना शुरू हुआ। खेतों और हस्तशिल्प से खदेड़े गये छोटे उत्पादक बड़ी संख्या में सर्वहारा की कतारों में शामिल हुए। मज़दूरों की जीवन स्थिति पहले से ही बदतर थी जो ख़ासकर 1825 के आर्थिक संकट के परिणामस्वरूप और भयावह हो रही थी। स्त्रियों व बच्चों के फैक्ट्री में सस्ती उजरत पर खटने के चलते मज़दूरी में गिरावट आयी। कार्यदिवस 12-14 घण्टे था। नये औद्योगिक कस्बों में रिहायशी स्थितियाँ असहनीय थी और मज़दूरों के ज़िले टाइफ़स और हैज़ा सरीखी महामारियों से ग्रस्त थे। मज़दूर वर्ग ने इस भयावह परिस्थिति का विरोध किया। चार्टिस्ट आन्दोलन, ल्योन के औद्योगिक दंगे और सिलेसियाई मज़दूरों की हड़तालें फूट पड़ीं। 1848 से पहले मज़दूरों के संघर्ष के यही मुख्य मील के पत्थर थे। 1836 में ‘लीग ऑफ़ जस्ट’ संगठन भी अस्तित्व में आया जिसका आधार पश्चिमी यूरोप के औद्योगिक शहरों में फैले जर्मन प्रवासी मज़दूर थे।
‘लीग ऑफ़ जस्ट’ का आधार जिन मज़दूरों के बीच था वे मुख्यतः दर्ज़ी और बढ़ई थे। लेकिन ये मज़दूर आधुनिक मज़दूर न होकर कारीगर थे। उनका चरित्र टुटपुँजिया वर्ग का था। एंगेल्स लिखते हैं:
“इसके सदस्य जब तक मज़दूर थे, तब तक वे विशेषतः कारीगर थे। यहाँ तक कि महानगरों के भीतर भी जो व्यक्ति उनका शोषण करता था, वह एक छोटा मालिक ही होता था। बड़े पूँजीपतियों के लिए हस्तशिल्प सिलाई को घरेलू उद्योग में बदलकर सिलाई के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर शोषण, जिसे आज रेडी-मेड कपड़ों के उत्पादन के रूप में जाना जाता है, लन्दन में भी उस दौर में बस शुरू ही हुआ था। जहाँ एक ओर इन कारीगरों के शोषक छोटे मालिक थे, वहीं दूसरी ओर ये सभी कारीगर इस बात के लिए आशान्वित रहते थे कि अन्ततः वे ख़ुद छोटे मालिक बन जायेंगे। इसके अतिरिक्त जर्मन कारीगरों के बीच विरासत में मिली गिल्ड धारणाएँ भी उनके बीच मौजूद थीं।”
आम तौर पर मज़दूरों के बीच काल्पनिक समाजवादियों और वाइटलिंग के विचारों का बोलबाला था। वाइटलिंग खुद दर्ज़ी था और ईसाइयत से भी प्रभावित था। वह कम्युनिज़्म और बाइबिल के उपदेशों को मिलाकर एक अलग क़िस्म के “कम्युनिज़्म” की वक़ालत कर रहा था। दूसरी तरफ़ कई मज़दूरों में ‘सच्चे समाजवाद’ का भी प्रभाव मौजूद था जिसका नारा था कि सभी इन्सान भाई हैं और प्रेम से इस दुनिया को बदला जा सकता है। इन विचारों का सम्बन्ध उन वर्ग स्थितियों और उस वैचारिक सामग्री से था जो उस काल के विचारकों के समक्ष उपलब्ध थी। छोटे उत्पादक व हस्तशिल्पी बर्बाद हो रहे थे और सर्वहारा वर्ग शिशु अवस्था में ही था और उसकी सैद्धान्तिक अवधारणाएँ भी आर्थिक विकास के अनुसार ही फ़िलहाल शिशुवत थीं। प्रबोधन और फ़्रांसिसी क्रान्ति के नारों को ही आगे बढ़ाते हुए ओवन, सेंट सिमों और फूरिये सरीखे लोगों ने काल्पनिक समाजवाद की अवधारणा रखी। उनके अनुसार समाजवाद राजनीतिक वर्ग संघर्ष के ज़रिये हासिल नहीं किया जाना था बल्कि शासक वर्ग के समक्ष उपदेश देकर किया जाना था। मज़दूरों के जिस प्रकार के संगठन मौजूद थे वे अधिकतर तख़्तापलट के संगठन थे। यही हो भी सकता था। ये संगठन नेतृत्व की राजनीतिक परिवर्तन की अवधारणा के अनुरूप थे। ब्लांकी ने पहली बार गुप्त संगठन के ढाँचे को सैन्य अनुशासन पर कसने की वक़ालत की और मज़दूर संगठनों के यूनियन सरीखे चरित्र की जगह एक गुप्त ढाँचे को पेश किया। लेकिन इस प्रकार के संगठन मज़दूर वर्ग और आम जन मानस में प्रचार पर ख़ास ज़ोर नहीं देते थे। यह इस कारण से ही था कि उनके बीच राजनीतिक वर्ग संघर्ष, सर्वहारा वर्ग की हिरावल भूमिका, राज्यसत्ता और क्रान्ति की ऐतिहासिक भौतिकवादी समझदारी का अभाव था। इनके लिए नयी सामाजिक व्यवस्था एक ऐसी आदर्श व्यवस्था थी जिसे तख़्तापलट कर हासिल किया जा सकता था। इस तरह इन संगठनों का प्रचार भी तख़्तापलट के ही मातहत होता था। ‘लीग ऑफ़ जस्ट’ का भी उद्भव इस प्रकार के एक संगठन से हुआ। एंगेल्स बताते हैं:
“1836 में गुप्त जनवादी-गणतान्त्रिक आउटलॉज़ लीग के सर्वोच्च उपांग, मुख्य रूप से सर्वहारा तत्व, जो 1834 में पेरिस शहर में जर्मन रिफ्यूजियों के द्वारा बनाया गया था, वह टूट गया और एक नये गुप्त ढाँचे ‘लीग ऑफ़ द जस्ट’ का निर्माण हुआ। पुरानी लीग, जिसमें जैकोबस वेनेडी जैसे ज़्यादातर तत्व बचे थे जो पहले से ही इस राह पर डगमगा रहे थे, उन्होंने जल्द ही क़दम पीछे हटा लिये। 1840 में पुलिस द्वारा जर्मनी के कुछ हिस्सों पर धावा बोलने के बाद पुरानी लीग की छाया भी बमुश्किल ही बची। वहीं इसके विपरीत नयी लीग सापेक्षतः काफ़ी तेज़ी से उभर कर आयी। मूल रूप से यह बाबूविज़्म सरीखा फ्रांसीसी कम्युनिज़्म का जर्मन आवरण था, जो इसी दौर में पेरिस में उभर रहा था। इस दौर में “समानता” के आवश्यक नतीजे के तौर पर कम्युनिटी ऑफ़ गुड्स की माँग की गयी। जर्मन गुप्त संगठन के उद्देश्य पेरिस के गुप्त संगठनों से कुछ अलग नहीं थे, जैसे: आधा प्रचार संघ, आधा षड्यन्त्र; पेरिस हमेशा से ही क्रान्तिकारी कार्रवाइयों का केन्द्र बिन्दु माना जाता था, यद्दपि जर्मनी के राज्य विध्वंस की कार्रवाइयों को भी नकारा नहीं जा सकता। लेकिन चूँकि पेरिस एक निर्णायक युद्धस्थल था, उस दौर में लीग फ्रांसीसी गुप्त संगठनों की जर्मन शाखा से अधिक कुछ भी नहीं था, ख़ास तौर पर ब्लांकि और बार्ब्स के नेतृत्व का संगठन सोसाइटी ऑफ़ सीजंस, जिसके साथ जर्मन संगठनों के अच्छे सम्बन्ध थे। फ्रांसीसी लोगों ने 12 मई, 1839 को, कार्रवाई को अंजाम दिया, जिसमें लीग के एक हिस्से ने आकर उनका साथ दिया, और जो अन्ततः पराजय का शिकार हुआ।”
इस तरह ‘लीग ऑफ़ जस्ट’ का उद्भव हुआ। ‘लीग ऑफ़ जस्ट’ अपना प्रचार शैक्षणिक संघ में करती थी या जहाँ परिस्थिति इसकी इजाज़त न दे वहाँ खेलकूद क्लब, संगीत टोली आदि के बीच करती थी। जन संगठन और पार्टी संगठन के तालमेल का पहला लेकिन अव्यवस्थित और बिखरा हुआ प्रयोग भी ‘लीग ऑफ़ जस्ट’ के क्रियाकलाप में देखा जा सकता है। एंगेल्स बताते हैं:
“लन्दन में स्विट्ज़रलैण्ड की तरह एक हद तक संगठन और सभा की आज़ादी थी। 7 फ़रवरी, 1840 की शुरुआत में क़ानूनी तौर पर मौजूदा कार्यरत जर्मन शैक्षणिक संघ का गठन हुआ था। इस संघ ने लीग के लिए भर्ती की ज़मीन तैयार की, और चूँकि हमेशा की तरह ही संघ के सबसे सक्रिय और बौद्धिक तौर पर बेहतर सदस्य कम्युनिस्ट थे, तो ज़ाहिरा तौर पर लीग के नेतृत्वकारी भूमिका उनके हाथों में थीं। लन्दन में इस लीग में बहुत कम वक्त में ही कई समुदाय साथ आने लगे, तब उन्हें वहाँ लॉज कहा जाता था। यही स्पष्ट रणनीति स्विट्ज़रलैण्ड और अन्य जगहों पर अपनायी जाने लगी। जहाँ पर इस प्रकार के मज़दूर संघ की स्थापना की जा सकती थी, वहाँ इस रूप में ही इसे इस्तेमाल किया गया। जहाँ इसपर क़ानूनी तौर पर रोक थी, वहाँ लोग कोरल सोसायटी, एथलेटिक क्लब इत्यादि के नाम पर शामिल होते थे। उन सदस्यों द्वारा बड़े स्तर पर सम्पर्कों को बनाये रखा गया, जो लगातार इधर-उधर आना जाना करते थे, ज़रूरत पड़ने पर वे दूत के रूप में भी काम कर रहे थे। दोनों ही मामलों में लीग को उन सरकारों की चतुराई की वजह से एक जीवन्त सहयोग मिला, जिसने निर्वासन का सहारा लेकर, किसी भी आपत्तिपूर्ण कार्यकर्ता को बदल दिया और दस में से नौ मामलों में वह लीग का सदस्य बनकर एक दूत बन गया।”
मार्क्स-एंगेल्स ने 1846 से मज़दूर संगठनों तथा लीग में मौजूद विजातीय प्रवृत्तियों के ख़िलाफ़ व्यवस्थित संघर्ष छेड़ दिया। इस दौरान उन्होंने ‘कम्युनिस्ट कॉरेस्पोंडेंस कमिटी’ का गठन किया जो लीग व अन्य मज़दूर संगठनों व कार्यकर्ताओं के बीच मार्क्स-एंगेल्स के विचारों का प्रचार कर रही थी। रिआज़ोनोव बताते हैं कि मार्क्स-एंगेल्स इस कमिटी को व्यवस्थित तौर पर चला रहे थे और लीग व मज़दूर संगठनों के साथ उनके बेहद घनिष्ठ सम्बन्ध थे। वाइटलिंग, प्रुधों से लेकर अन्य विजातीय प्रवृत्तियों के विरुद्ध मार्क्स-एंगेल्स के कुशल नेतृत्व में इस कमिटी ने विचारधारात्मक संघर्ष चलाया और ‘लीग ऑफ़ जस्ट’ को ‘कम्युनिस्ट लीग’ बनाने में भूमिका निभायी। मार्क्स और एंगेल्स ‘लीग ऑफ़ जस्ट’ से औपचारिक तौर पर 1847 में जुड़े और उसे एक कम्युनिस्ट संगठन में तब्दील कर दिया। इस संगठन की नियमावली में एक केन्द्रीकृत कमिटी, जिसके मातहत कई चक्रों और हर चक्र के मातहत दस से बीस कम्युनिटी का प्रावधान था। कम्युनिटी, चक्र, नेतृत्वकारी चक्र, केन्द्रीय अथॉरिटी और कांग्रेस में लीग संगठित थी। हालाँकि अभी यह लेनिन के “जनवादी केन्द्रीयता” के सिद्धान्त का सूत्रीकरण नहीं था। लीग में शामिल होने के लिए लीग के विचारों को स्वीकारना होता था हालाँकि लेनिनवादी पार्टी सदस्यता की अवधारणा अभी मौजूद नहीं थी। भ्रूण रूप में ज़रूर कम्युनिस्ट पार्टी के संगठन और ढाँचे के तत्व मौजूद थे परन्तु उनका सैद्धान्तिकरण नहीं था, यह लेनिन के दौर में ही हो सकता था। यह पार्टी संगठन और उसके ढाँचे का पहला प्रयोग था जिसने लेनिनवादी पार्टी अवधारणा के लिए पूर्वपीठिका तैयार की। यह भी हमें ध्यान में रखना होगा कि जिस दौर में लीग गठित हुई वह एक गुप्त संगठन के रूप में ही गठित हो सकती थी। ‘कम्युनिस्ट लीग’ के कई सांगठनिक उसूल राजनीतिक परिस्थितियों की वजह से उपजे थे। यही कारण है कि एंगेल्स ‘कम्युनिस्ट लीग’ को “प्रॉपगैण्डा करने वाला एक गुप्त संगठन” कहते हैं। एंगेल्स कहते हैं:
“फ़रवरी क्रान्ति के दौरान जर्मन “कम्युनिस्ट पार्टी” (जैसा कि हमने इसे नाम दिया है) का ‘कम्युनिस्ट लीग’ के रूप में एक छोटा कोर मौजूद था, जो कि प्रॉपगैण्डा करने वाले एक गुप्त संगठन के रूप में बना था। यह लीग गुप्त केवल इसलिए था क्योंकि उस वक़्त जर्मनी में किसी भी क़िस्म के संघ बनाने या सभा करने की आज़ादी नहीं थी। उन विदेशी मज़दूर संगठनों के अलावा, जहाँ से भर्तियाँ हो रही थीं, केवल जर्मनी में ही 30 समुदाय या सेक्शन मौजूद थे। साथ ही कुछ जगहों पर बिखरे-बिखरे तौर पर संगठन के कई सदस्य भी मौजूद थे। हालाँकि इस छोटी-सी जुझारू ताक़त के पास एक लीडर थे: मार्क्स, जिनके प्राधिकार को कई लोगों ने स्वीकार किया था, जो प्रथम श्रेणी के लीडर थे, और जिनकी वजह से उसूलों और रणकौशलों के कार्यक्रम के रूप में कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणापत्र हम तक पहुँच पाया, जिसकी प्रासंगिकता आज भी कम नहीं हुई है।”
वह सामान्यीकरण जो आज भी कम्युनिस्ट पार्टी के लिए प्रासंगिक है, वह मार्क्स-एंगेल्स के इन शब्दों में अभिव्यक्त किया जा सकता है:
“कम्युनिस्ट दूसरी मज़दूर पार्टियों के विरुद्ध अपनी कोई अलग पार्टी नहीं बनाते। समग्र रूप में सर्वहारा के हितों के अलावा और पृथक उनके कोई हित नहीं हैं।
“वे सर्वहारा आन्दोलन को ख़ास नमूने पर ढालने या विशेष रूप प्रदान करने के लिए अपने कोई संकीर्ण सिद्धान्त नहीं स्थापित करते।
“कम्युनिस्ट दूसरी मज़दूर पार्टियों से सिर्फ़ इस लिहाज़ से भिन्न हैं 1. विभिन्न देशों के सर्वहाराओं के राष्ट्रीय संघर्षों में वे राष्ट्रीयता से सर्वथा निरपेक्षतः समस्त सर्वहारा के सामान्य हितों को इंगित करते और सामने लाते हैं। 2. बुर्जुआ वर्ग के ख़िलाफ़ मज़दूर वर्ग के संघर्ष को जिन विभिन्न मंज़िलों से होकर गुज़रता होता है, उनमें वे हमेशा और हर कहीं समूचे तौर पर आन्दोलन के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
“अतः एक ओर, व्यावहारिक दृष्टि से, कम्युनिस्ट हर देश की मज़दूर पार्टियों के सबसे उन्नत और कृतसंकल्प हिस्से होते हैं, ऐसे हिस्से जो औरों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं; दूसरी ओर, सैद्धान्तिक दृष्टि से, सर्वहारा वर्ग के विशाल जन-समुदाय की अपेक्षा वे इस अर्थ में उन्नत हैं कि वे सर्वहारा आन्दोलन के आगे बढ़ने के रास्ते की, उसके हालात और सामान्य अन्तिम नतीजों की सुस्पष्ट समझ रखते हैं।”
यह कम्युनिस्ट पार्टी का सर्वहारा वर्ग के हिरावल के रूप में सैद्धान्तिकीकरण है। एंगेल्स बताते हैं कि “1847 के दौरान ‘कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणापत्र’ में कम्युनिस्ट लीग के बैनर के तले लाये गये सैद्धान्तिक उसूलों ने आज के दौर में यूरोप और अमेरिका दोनों के ही पूरे सर्वहारा वर्ग के आन्दोलन को अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर मज़बूती देने का काम किया है।” घोषणापत्र ने सभी भ्रान्तिपूर्ण ‘काल्पनिक समाजवादी’ शिक्षाओं को हटाकर इस बात को स्थापित कर दिया कि इतिहास की चालक शक्ति वर्ग-संघर्ष है और वर्ग-संघर्ष की जड़ें समाज की आर्थिक बुनियाद में निहित हैं। कम्युनिस्ट घोषणापत्र सर्वहारा क्रान्ति के उद्देश्यों और लक्ष्यों का सर्वप्रथम और संक्षिप्ततम सूत्रीकरण भी है। कोलोन मुक़दमे के बाद ‘कम्युनिस्ट लीग’ को भंग कर दिया गया। यह यूरोप के 1848-52 के क्रान्तिकारी दौर का भी समापन था। अगले अंक में हम प्रथम इण्टरनेशनल के प्रयोग तथा यूरोप की पहली सामाजिक जनवादी पार्टियों के उद्भव पर बातचीत करेंगे।
मज़दूर बिगुल, जून 2024
‘मज़दूर बिगुल’ की सदस्यता लें!
वार्षिक सदस्यता - 125 रुपये
पाँच वर्ष की सदस्यता - 625 रुपये
आजीवन सदस्यता - 3000 रुपये
आर्थिक सहयोग भी करें!
 बुर्जुआ अख़बार पूँजी की विशाल राशियों के दम पर चलते हैं। मज़दूरों के अख़बार ख़ुद मज़दूरों द्वारा इकट्ठा किये गये पैसे से चलते हैं।
बुर्जुआ अख़बार पूँजी की विशाल राशियों के दम पर चलते हैं। मज़दूरों के अख़बार ख़ुद मज़दूरों द्वारा इकट्ठा किये गये पैसे से चलते हैं।
मज़दूरों के महान नेता लेनिन