पश्चलेख – फासीवाद क्या है और इससे कैसे लड़ें?
अभिनव सिन्हा
2009 में कांग्रेस-नीत ‘संयुक्त प्रगतिशील गठबन्धन’ की अप्रत्याशित चुनावी जीत के ठीक बाद मज़दूर अख़बार “नयी समाजवादी क्रांति का उद्घोषक बिगुल” में जून 2009 से दिसम्बर 2009 के बीच छह किश्तों में “फासीवाद क्या है और इससे कैसे लड़ें?” शीर्षक से लेख प्रकाशित हुए थे। राहुल फाउण्डेशन ने इन लेख़ों को बाद में एक पुस्तिका के रूप में भी प्रकाशित किया। तब संसदीय वामपंथियों और संशोधनवादियों समेत क्रान्तिकारी वाम का भी एक हिस्सा इस बात पर जश्न मना रहा था कि भाजपा की चुनावों में भारी हार हुई थी। कई तो इसे फासीवाद की निर्णायक पराजय भी क़रार दे रहे थे! इस तरह के दावे केवल यही दिखला रहे थे कि एक मज़दूर-विरोधी राजनीतिक और सामाजिक आन्दोलन के तौर पर फासीवाद की उनकी समझदारी कितनी दरिद्र है। हमने तब भी लिखा था कि चुनावी पराजय को फासीवाद की पराजय मानना एक भारी भूल है। और सर्वहारा वर्ग के प्रतिरोध की रणनीति को बनाने के लिए ऐसी सोच विशेष तौर पर नुकसानदेह है। 2014 के लोकसभा चुनावों में फासीवादी शक्तियों की अभूतपूर्व जीत ने इस बात को सिद्ध भी किया। एक ऐसे दौर में हमने इस पुस्तिका के साथ एक पश्चलेख जोड़ा है। इसमें कुछ अहम छूटे हुए नुक्तों को जोड़ा गया है जो मोदी सरकार और फासीवाद के इस नये उभार के समकालीन सन्दर्भ में ज़रूरी महसूस हुए। हम उम्मीद करते हैं कि इससे हम इस पुस्तिका में पेश अपनी समझदारी को और विस्तार के साथ व्याख्यायित कर पाये होंगे और साथ ही उसे विस्तार दे पाये होंगे।
यह पुस्तिका 2009 में कांग्रेस-नीत ‘संयुक्त प्रगतिशील गठबन्धन’ की अप्रत्याशित चुनावी जीत के ठीक बाद लिखी गयी थी। तब संसदीय वामपंथियों और संशोधनवादियों समेत क्रान्तिकारी वाम का भी एक हिस्सा इस बात पर जश्न मना रहा था कि भाजपा की चुनावों में भारी हार हुई थी। कई तो इसे फासीवाद की निर्णायक पराजय भी क़रार दे रहे थे! इस तरह के दावे केवल यही दिखला रहे थे कि एक मज़दूर-विरोधी राजनीतिक और सामाजिक आन्दोलन के तौर पर फासीवाद की उनकी समझदारी कितनी दरिद्र है। हमने तब भी लिखा था कि चुनावी पराजय को फासीवाद की पराजय मानना एक भारी भूल है। और सर्वहारा वर्ग के प्रतिरोध की रणनीति को बनाने के लिए ऐसी सोच विशेष तौर पर नुकसानदेह है। इसके कई कारण हैं।
पहली बात तो यह है कि एकाधिकारी पूँजीवाद के दौर में पूँजीवादी आर्थिक ‘जनवाद’ के ख़त्म होने के साथ राजनीतिक बुर्जुआ जनवाद का भी क्षरण होता है; ऐसे में, तथाकथित उदार व ‘सेक्युलर’ बुर्जुआ शक्तियाँ भी सत्ता में होने पर मज़दूर वर्ग के लिए कमोबेश उतनी ही दमनकारी सिद्ध होती हैं, जितनी के फासीवादी बुर्जुआ ताक़तें और यही कारण है कि भाजपा की हार पर आनन्दातिरेक में जाने का कोई विशेष कारण नहीं था। यह बात ‘संयुक्त प्रगतिशील गठबन्धन’ के एक दशक के शासन में सिद्ध भी हुई जब मज़दूर-विरोधी और कम्युनिज़्म-विरोधी दमनकारी कानूनों जैसे कि ‘आतंकवाद-निरोधक कानून’ के पारित होने के साथ-साथ ‘ऑपरेशन ग्रीन हण्ट’ और सलवा जुडूम जैसी कुत्सित मुहिमें और प्रयास भी हुए। निश्चित तौर पर, इसका यह अर्थ नहीं है कि हम फासीवादी बुर्जुआ पार्टियों, जैसे कि भाजपा, शिवसेना आदि में और अन्य बुर्जुआ पार्टियों में कोई फ़र्क नहीं करते। कहने की आवश्यकता नहीं है कि इन दोनों में गहरा फर्क है और सत्ता में आने पर ये दो भिन्न प्रकार की बुर्जुआ राज्यसत्ताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन इतना निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि अन्य ‘उदार’ बुर्जुआ पार्टियों में भी आज के एकाधिकारी पूँजीवाद के चरण में कोई विशेष जनवादी सम्भावना शेष नहीं रह गयी है।
 दूसरी बात जो ग़ौर करने लायक है वह यह कि आज के अभूतपूर्व रूप से मानवद्रोही, पतनशील और परजीवी पूँजीवाद के दौर में फासीवाद के सत्ता में रहने या न रहने से उसके अस्तित्व पर परिमाणात्मक रूप में ही असर पड़ता है। हालाँकि यह बात पहले भी एक हद तक लागू होती थी मगर आज के दौर में यह बात पहले हमेशा से ज़्यादा लागू होती है, जबकि फासीवाद वैश्विक संकट के ज़्यादा संरचनागत बनने के साथ पतनशील बुर्जुआ समाज की एक स्थायी और ढाँचागत परिघटना बन चुका है। फासीवादी शक्तियों का जीवित रहना या उनकी सतत् मौजूदगी आज पूँजीवादी व्यवस्था की एक अपरिहार्यता है। वैश्विक संकट के दौर में मज़दूर आन्दोलनों के सरकारी दमन के अलावा ग़ैर-सरकारी दमन और आतंक की रणनीति का शासक वर्गों के लिए एक भारी महत्व है। ऐसे में, शासक वर्ग विशेष तौर पर फासीवाद को ‘ज़ंजीर से बँधे कुत्ते’ के समान इस्तेमाल करता है और पहले से भिन्न उसे इस कुत्ते की ज़रूरत अब लगभग हर वक़्त है। यह अकारण नहीं है कि कांग्रेस के शासन-काल के दौरान भी हिन्दुत्ववादी आतंकवाद पर कोई सख़्त कार्रवाई नहीं की गयी; भोंसले सैन्य विद्यालय से लेकर संघ परिवार की तमाम संस्थाओं को खुलेआम चलते रहने की इजाज़त दी गयी; संक्षेप में कहें तो कांग्रेस या संयुक्त मोर्चे जैसे चुनावी गठबन्धनों की सरकार ने भी संघ परिवार के घृणित षड्यन्त्रों, दंगे फैलाने, हिन्दुत्ववादी आतंकवाद को शह देने आदि जैसी हरक़तों पर कभी भी प्रभावी ढंग से लगाम नहीं कसी। इसका कारण कोई अज्ञान या उपेक्षा के कारण हुई ग़लती नहीं थी। बल्कि यह भारतीय शासक वर्गों की एक सुचिन्तित नीति रही है। मुम्बई में शिवसेना के उभार की कहानी एक मिसाल है। जब शिवसेना सत्ता में नहीं भी थी तो उसे मुम्बई के मज़दूर आन्दोलन को कुचलने के लिए एक गुण्डा शक्ति के रूप में इस्तेमाल किया गया जो कि आतंक की रणनीति अपना कर मज़दूर आन्दोलन पर प्राणान्तक चोट करती रही। यह एक दीगर बात है कि इसका वामपंथी शक्तियों ने संशोधनवाद और सुधारवाद का शिकार होने के कारण कभी कोई अर्थपूर्ण प्रतिरोध ही नहीं किया। बहरहाल, अगर भारतीय इतिहास पर एक सरसरी निगाह भी डाली जाये तो साफ़ हो जाता है कि फासीवादी ताक़तें सत्ता में रहें या न रहें, शासक वर्गों ने हमेशा उनका मज़दूर वर्ग के आन्दोलन पर चोट के लिए इस्तेमाल किया है। फासीवाद मज़दूर वर्ग का सबसे बड़ा शत्रु है और वह सत्ता के अन्दर और बाहर से मज़दूर आन्दोलन पर हमेशा हमले करता रहा है और करता रहेगा। यह बात भी उतनी ही सच है कि किसी भी किस्म का नेहरू-ब्राण्ड मानवतावाद, सर्वधर्म सम्भाव, ‘सेक्युलरिज़्म’ या उदारपंथ इस शक्ति का मुकाबला नहीं कर सकता है। साथ ही, माकपा-भाकपा जैसी संशोधनवादी पार्टियों के प्रतीकवादी शोर-शराबे से भी फासीवाद की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। फासीवाद की कब्र खोदने का काम मज़दूर वर्ग की क्रान्तिकारी पार्टी और उसके क्रान्तिकारी आन्दोलन के ज़रिये ही हो सकता है और हम यह बात महज़ किसी उद्वेलनात्मक जुमले के रूप में नहीं कह रहे हैं बल्कि इसके निश्चित ऐतिहासिक राजनीतिक कारण हैं।
दूसरी बात जो ग़ौर करने लायक है वह यह कि आज के अभूतपूर्व रूप से मानवद्रोही, पतनशील और परजीवी पूँजीवाद के दौर में फासीवाद के सत्ता में रहने या न रहने से उसके अस्तित्व पर परिमाणात्मक रूप में ही असर पड़ता है। हालाँकि यह बात पहले भी एक हद तक लागू होती थी मगर आज के दौर में यह बात पहले हमेशा से ज़्यादा लागू होती है, जबकि फासीवाद वैश्विक संकट के ज़्यादा संरचनागत बनने के साथ पतनशील बुर्जुआ समाज की एक स्थायी और ढाँचागत परिघटना बन चुका है। फासीवादी शक्तियों का जीवित रहना या उनकी सतत् मौजूदगी आज पूँजीवादी व्यवस्था की एक अपरिहार्यता है। वैश्विक संकट के दौर में मज़दूर आन्दोलनों के सरकारी दमन के अलावा ग़ैर-सरकारी दमन और आतंक की रणनीति का शासक वर्गों के लिए एक भारी महत्व है। ऐसे में, शासक वर्ग विशेष तौर पर फासीवाद को ‘ज़ंजीर से बँधे कुत्ते’ के समान इस्तेमाल करता है और पहले से भिन्न उसे इस कुत्ते की ज़रूरत अब लगभग हर वक़्त है। यह अकारण नहीं है कि कांग्रेस के शासन-काल के दौरान भी हिन्दुत्ववादी आतंकवाद पर कोई सख़्त कार्रवाई नहीं की गयी; भोंसले सैन्य विद्यालय से लेकर संघ परिवार की तमाम संस्थाओं को खुलेआम चलते रहने की इजाज़त दी गयी; संक्षेप में कहें तो कांग्रेस या संयुक्त मोर्चे जैसे चुनावी गठबन्धनों की सरकार ने भी संघ परिवार के घृणित षड्यन्त्रों, दंगे फैलाने, हिन्दुत्ववादी आतंकवाद को शह देने आदि जैसी हरक़तों पर कभी भी प्रभावी ढंग से लगाम नहीं कसी। इसका कारण कोई अज्ञान या उपेक्षा के कारण हुई ग़लती नहीं थी। बल्कि यह भारतीय शासक वर्गों की एक सुचिन्तित नीति रही है। मुम्बई में शिवसेना के उभार की कहानी एक मिसाल है। जब शिवसेना सत्ता में नहीं भी थी तो उसे मुम्बई के मज़दूर आन्दोलन को कुचलने के लिए एक गुण्डा शक्ति के रूप में इस्तेमाल किया गया जो कि आतंक की रणनीति अपना कर मज़दूर आन्दोलन पर प्राणान्तक चोट करती रही। यह एक दीगर बात है कि इसका वामपंथी शक्तियों ने संशोधनवाद और सुधारवाद का शिकार होने के कारण कभी कोई अर्थपूर्ण प्रतिरोध ही नहीं किया। बहरहाल, अगर भारतीय इतिहास पर एक सरसरी निगाह भी डाली जाये तो साफ़ हो जाता है कि फासीवादी ताक़तें सत्ता में रहें या न रहें, शासक वर्गों ने हमेशा उनका मज़दूर वर्ग के आन्दोलन पर चोट के लिए इस्तेमाल किया है। फासीवाद मज़दूर वर्ग का सबसे बड़ा शत्रु है और वह सत्ता के अन्दर और बाहर से मज़दूर आन्दोलन पर हमेशा हमले करता रहा है और करता रहेगा। यह बात भी उतनी ही सच है कि किसी भी किस्म का नेहरू-ब्राण्ड मानवतावाद, सर्वधर्म सम्भाव, ‘सेक्युलरिज़्म’ या उदारपंथ इस शक्ति का मुकाबला नहीं कर सकता है। साथ ही, माकपा-भाकपा जैसी संशोधनवादी पार्टियों के प्रतीकवादी शोर-शराबे से भी फासीवाद की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। फासीवाद की कब्र खोदने का काम मज़दूर वर्ग की क्रान्तिकारी पार्टी और उसके क्रान्तिकारी आन्दोलन के ज़रिये ही हो सकता है और हम यह बात महज़ किसी उद्वेलनात्मक जुमले के रूप में नहीं कह रहे हैं बल्कि इसके निश्चित ऐतिहासिक राजनीतिक कारण हैं।
आज नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार (कहने के लिए ‘राष्ट्रीय जनतान्त्रिक गठबन्धन’ की सरकार) सत्ता में है। इसने सत्ता में आने के एक वर्ष के भीतर ही अपने इरादे और मंसूबे साफ़ कर दिये हैं। मोदी सरकार ने जो सबसे पहले कदम उठाये हैं उन पर एक निगाह डाली जाये तो स्पष्ट हो जाता है कि मज़दूर वर्ग के बचे-खुचे श्रम अधिकार, उसका ट्रेड यूनियन आन्दोलन और उसका क्रान्तिकारी आन्दोलन इस सरकार के एजेण्डे पर पहला निशाना हैं। यही कारण है कि मोदी सरकार ने आते ही कारखाना अधिनियम, औद्योगिक विवाद अधिनियम, ट्रेड यूनियन अधिनियम, अप्रेण्टिस कानून आदि में बदलाव करने का एलान कर दिया। यह प्रक्रिया गुजरात और राजस्थान की भाजपा सरकार ने तो पहले ही शुरू कर दी थी और अब मोदी सरकार इसे राष्ट्रीय पैमाने पर अंजाम दे रही है। इन कानूनों में बदलाव का अर्थ होगा मज़दूर वर्ग के बचे-खुचे श्रम अधिकारों का ख़ात्मा और संकट से बिलबिलाये देशी-विदेशी पूँजीपतियों को देश की श्रमशक्ति का बेरोक-टोक दोहन करने की आज़ादी। हर जगह मज़दूर आन्दोलन का पुरज़ोर दमन करने के लिए राज्यसत्ता की दमनकारी मशीनरी को खुली छूट दी जा रही है और उसे पहले से अधिक चाक-चौबन्द और प्रभावी बनाया जा रहा है। इसके अलावा, मज़दूर वर्ग के आन्दोलन को भीतर से कमज़ोर बनाने के लिए एक मिथ्या शत्रु का निर्माण किया जा रहा है। विशेष तौर पर हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान व दिल्ली के क्षेत्रों में (जो कि संघ परिवार के कमज़ोरी के क्षेत्र रहे हैं) में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे पैमाने के दंगे फैलाने के प्रयास किये जा रहे हैं।
इसके अलावा, टटपुँजिया वर्गों के बीच हिन्दुत्ववादी फासीवाद का आधार तैयार करने के लिए शिक्षा व संस्कृति के तमाम संस्थानों और क्षेत्रों का भगवाकरण करने की मुहिम को फासीवादी पुरज़ोर तरीके से चला रहे हैं। स्कूली पाठ्यक्रमों को बदलने से लेकर सामाजिक विज्ञान के अनुसंधान संस्थानों और कला, नाटक व फिल्म आदि के संस्थानों में भगवा ब्रिगेड के बर्बरों को मुखिया बनाने तक, मोदी सरकार वाकई 24 घण्टे काम कर रही है! इसके अलावा, मीडिया में अभूतपूर्व पैमाने पर इज़ारेदारीकरण के साथ तमाम समाचार चैनलों व अन्य मनोरंजन चैनलों को, पहले हमेशा से ज़्यादा, फासीवादी भोंपुओं के समान इस्तेमाल किया जा रहा है। विदेश नीति में भी मोदी सरकार ने ज़्यादा स्पष्टता के साथ साम्राज्यवादी ताक़तों के साथ अपनी पक्षधरता को ज़ाहिर किया है और साथ ही अपने मोलभाव की क्षमता को भी उसने पुरज़ोर तरीके से रेखांकित किया है। हाल ही में गाज़ा में इज़रायल द्वारा एक वर्ष पहले किये गये बर्बर नरसंहार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र में पारित होने वाले प्रस्ताव में भारत ने वोट नहीं डाला। इज़रायल के पक्ष में इतने खुले तौर पर झुकने की घटना विशेष तौर पर ध्यान देने योग्य है। संक्षेप में, मोदी सरकार ने एक वर्ष के भीतर ही अपना मज़दूर-विरोधी फासीवादी रवैया स्पष्ट कर दिया है।
जो एक चीज़ मोदी सरकार के लिए सिरदर्द का सबब है वह यह है कि काफ़ी लम्बे इन्तज़ार के बाद जब भाजपाइयों को सरकार बनाने का अवसर मिला है तो भ्रष्टाचार, घूसखोरी, काली कमाई करने के मामले में वे नियन्त्रण खो बैठे हैं। वसुन्धरा राजे, सुषमा स्वराज, पंकजा मुण्डे, शिवराज सिंह चौहान, तावड़े, रमन सिंह आदि जैसे बड़े भाजपा नेता नग्न तौर पर भ्रष्टाचार और कारपोरेट घरानों की ग़ैर-कानूनी तरीके से सेवा करने में नंगे तौर पर लिप्त पाये गये हैं। यहाँ तक कि नरेन्द्र मोदी तक का नाम ललित मोदी काण्ड में सामने आया है! मोदी ने फासीवादी सौन्दर्यीकरण के ज़रिये अपनी जो एक लोकरंजक शैली विकसित की थी, इन खुलासों के कारण वह भी लोगों में मज़ाक का विषय बन गयी है! फासीवादी अतिमानव को जिस प्रकार का आभा-मण्डल कायम रखना पड़ता है, उसमें मोदी को काफ़ी दिक़्कतों का सामना करना पड़ रहा है! मगर फिर भी महज़ इस पहलू के कारण अगर कोई मौजूदा सरकार के फासीवादी ‘क्रेडेंशियल’ पर शक़ करे तो उसे राजनीतिक नौसिखुआ ही कहा जायेगा! संक्षेप में, इस बात में कोई शक़ नहीं है कि मोदी सरकार स्पष्टतः एक फासीवादी सरकार है और अगर उसके नेतृत्व, नीतियों, विचारधारा और कार्यपद्धति को देखा जाय तो यह बात साफ़ हो जाती है।
लेकिन सिर्फ़ इतना कहने से बात ख़त्म नहीं हो जाती। हमने 2009 में लिखित इस पुस्तिका में फासीवादी उभार के आम कारणों और उसकी चारित्रिक आभिलाक्षणिकताओं के बारे में लिखा था; हमने फासीवादी उभार के सामाजिक आधार का वर्ग विश्लेषण किया था; साथ ही, हमने फासीवादी उभार से लड़ने की सम्भावित मज़दूर वर्गीय रणनीति पर भी संक्षेप में चर्चा की थी। इसके अलावा हमने जर्मनी और इटली में फासीवादी उभार और साथ ही भारत में फासीवादी आन्दोलन के इतिहास का संक्षिप्त विवरण भी पेश किया था। मगर इतना ही काफ़ी नहीं है। इसके साथ ही यह भी ज़रूरी है कि हम कुछ अन्य सवालों पर भी सोचें, मसलन, बीसवीं सदी में जर्मनी, इटली व कुछ अन्य देशों जैसे कि पुर्तगाल और हंगरी में फासीवादी व अर्द्धफासीवादी सत्ताओं और साथ ही अन्य कई देशों में फासीवादी पार्टियों व राजनीति के चरित्र और आज के दौर में फासीवादी सत्ताओं और राजनीति के चरित्र में क्या हम कोई फर्क कर सकते हैं? क्या पूँजीवादी संकट के बदलते चरित्र के साथ फासीवाद की परिघटना के स्वरूप में भी बदलाव आया है? क्या इन बदलावों के मद्देनज़र सर्वहारा वर्ग को अपनी रणनीति में भी कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता है? लेकिन शुरुआत हम इस सवाल से करेंगे कि मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद भारत में भगवा गिरोह की कार्यशैली में क्या बदलाव आये हैं और इस पर हमारा रुख़ क्या होना चाहिए।
फासीवादी मोदी सरकार की मज़दूर-विरोधी रणनीति क्या है?
16 मई 2014 को सत्ता में आने के बाद नरेन्द्र मोदी की सरकार की रणनीति को समझना न सिर्फ दूरगामी तौर पर बल्कि तात्कालिक तौर पर भी मज़दूर वर्ग के लिए अहम है। मोदी सरकार एक ऐसे समय में सत्ता में आयी जबकि पूँजीपति वर्ग दुनिया भर में और हमारे देश में भी आर्थिक संकट से बेहाल है। इस अभूतपूर्व वैश्विक संकट के केन्द्र अभी भारत और चीन जैसे देश नहीं बने हैं, बल्कि अमेरिका और यूरोप हैं। लेकिन इस संकट का गुरुत्व केन्द्र तेज़ी से पूर्व की ओर स्थानान्तरित हो रहा है और कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी अगर यह दशक ख़त्म होते-होते भारत व चीन जैसी “उभरती अर्थव्यवस्थाएँ” इस संकट का केन्द्र बन जायें। लेकिन अभी भी ये अर्थव्यवस्थाएँ संकट से अछूती नहीं हैं और उसका असर यहाँ भी महसूस किया जा रहा है। और चिन्ता की बात यह है कि यह संकट निरन्तर बढ़ रहा है। यह अति-उत्पादन और अति-संचय का संकट है जो कि पूँजीवादी व्यवस्था में नियमित अन्तरालों पर आता रहता है। अब तो वास्तव में आर्थिक मन्दी व्यवस्था की एक स्थायी परिघटना बन गयी है जो कि बीच-बीच में भयंकर संकटों में तब्दील होती रहती है। इस पूरी प्रक्रिया की एक चर्चा हमने इस पुस्तिका में 2009 में ही की थी, जबकि अभी नयी वैश्विक महामन्दी विश्व के विभिन्न हिस्सों को अपनी गिरफ्त में लेने की प्रक्रिया में थी। लेकिन विश्व पूँजीवाद वित्तीय सट्टेबाज़ पूँजी के ज़रिये आवास उद्योग में पैदा किये गये बुलबुले के कारण ‘तेज़ी’ का जो दौर देख रहा था, वह निर्णायक रूप से खत्म हो चुका था। 2007 में अमेरिका में सबप्राइम ऋण संकट की शुरुआत के साथ एक महामन्दी की शुरुआत हुई, जो कि अब 1930 के दशक की महामन्दी से भी ज़्यादा ढाँचागत, गहरी और गम्भीर साबित हो रही है।
अपने इस असमाधेय संकट से निपटने के लिए दुनिया के तमाम देशों में पूँजीपति वर्ग सबसे प्रतिक्रियावादी, दक्षिणपंथी, मज़दूर-विरोधी और फासीवादी सरकारों को चुन रहे हैं। चाहें वह ब्रिटेन में डेविड कैमरून हों, ऑस्ट्रेलिया में टोनी एबट या फिर थाईलैण्ड में सैनिक तानाशाही की स्थापना हो, हम देख सकते हैं कि आर्थिक संकट के भँवर में फँसा पूँजीपति वर्ग अधिकतर देशों में किसी धुर दक्षिणपंथी या फासीवादी विकल्प को चुन रहा है। भारत में नरेन्द्र मोदी के सत्ता में आने को भी इस पूरी वैश्विक परिघटना के एक अंग के तौर पर देखा जाना चाहिए, हालाँकि हर देश में इस आम रुझान की अपनी विशिष्टताएँ हैं। लेकिन सत्ता में आने के पहले और सत्ता में आने के बाद फासीवाद की ठोस रणनीति में कुछ परिवर्तन आते हैं, हालाँकि उसकी राजनीति और विचारधारा वही होती है। साथ ही आज के दौर में फासीवाद की रणनीति में परिवर्तन आने के कुछ ऐतिहासिक कारण भी हैं, जिनकी हम आगे चर्चा करेंगे।
सरकार में आने से पहले हिन्दुत्ववादी फासीवादी ताक़तें देश में ‘लव जिहाद’, ‘घर वापसी’ जैसी जनविरोधी मुहिमें और साथ ही साम्प्रदायिक दंगे आयोजित करवाने का काम खुले तौर पर कर रही थीं और भाजपा का मुख्य नेतृत्व भी इस पर या तो चुप्पी साधे रहता था या फिर उसके समर्थन में बोलता था। सरकार बनाने के बाद इस रणनीति में थोड़ा परिवर्तन हुआ है। अब नरेन्द्र मोदी सामान्य तौर पर साम्प्रदायिकता पर या तो चुप रहते हैं या फिर उसकी निन्दा करते नज़र आते हैं। मोदी द्वारा अब इस तरह की बातें की जाती हैं कि ‘किसी को भारत के सेक्युलर और सहिष्णु ताने-बाने को नष्ट नहीं करने दिया जायेगा’, ‘भारत में सभी नागरिकों को अपने धर्म के पालन की आज़ादी मिलेगी’, वगैरह। लेकिन इस तरह की बयानबाज़ी के साथ मोदी सरकार ने बजरंग दल, विहिप, हिन्दु युवा वाहिनी जैसे हिन्दुत्ववादी फासीवादी गुण्डा गिरोहों को खुला हाथ दे दिया है। ज़मीनी धरातल पर ये हिन्दुत्ववादी फासीवादी गिरोह महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान से लेकर हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल तक में अपनी फासीवादी हरक़तों को अंजाम दे रहे हैं। चाहे वह बहादुगढ़ से पलवल तक दंगे करवाने की हरक़तें हों या फिर देश के तमाम हिस्सों में गाय हत्या की अफ़वाहें उड़ाकर या फिर पाकिस्तान का झण्डा फहरा कर मुसलमानों के ख़िलाफ़ दंगे भड़काने के कुकृत्य हों, ये गुण्डा वाहिनियाँ ‘ओवरटाइम’ काम कर रही हैं। इसका कारण यही है कि मोदी सरकार ऊपरी तौर पर तमाम बयान दे रही है लेकिन ज़मीनी तौर पर उसने भगवा गिरोहों को खुला हाथ दे दिया है।
इन भगवा गिरोहों को खुला हाथ देने के अलावा, तमाम भगवा फासीवादी सांस्कृतिक, बौद्धिक और शैक्षणिक संस्थाओं (जो सुनने में अजीब लगता है क्योंकि इन साम्प्रदायिक फासीवादियों के पास संस्कृति, बुद्धि और शिक्षा के नाम पर जो कुछ है वह हास्यास्पद है!) को देश में अपनी जड़ें फैलाने, सरकारी संस्थाओं का भगवाकरण करने, स्कूली से लेकर उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम का फासीवादीकरण करने की छूट दे दी गयी है। भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद् से लेकर एन.सी.ई.आर.टी. तक और पुणे के भारतीय फिल्म व टेलीविजन संस्थान के भगवाकरण और चेन्नई आई.आई.टी. के प्रगतिशील स्वरों पर पाबन्दी लगाने तक की घटनाएँ संघी फासीवाद के मंसूबों को साफ़ कर रही हैं। इन ख़तरनाक कदमों को मज़दूर वर्ग को कम करके नहीं आँकना चाहिए। ये कदम एक पूरी पीढ़ी के दिमाग़ों में ज़हर घोलने, उनका फासीवादीकरण करने, उन्हें दिमाग़ी तौर पर गुलाम बनाने और साथ ही मज़दूर वर्ग को वैज्ञानिक और तार्किक चिन्तन की क्षमता से वंचित करने का काम करते हैं। जिस देश के मज़दूर और छात्र-युवा वैज्ञानिक और तार्किक चिन्तन की काबिलियत खो बैठते हैं वे अपनी मुक्ति के मार्ग को भी नहीं पहचान पाते हैं और न ही वे मज़दूर आन्दोलन के मित्र बन पाते हैं। उल्टे वे मज़दूर आन्दोलन के शत्रु के तौर पर तैयार किये जाते हैं और शैक्षणिक, बौद्धिक व सांस्कृतिक संस्थाओं का फासीवादीकरण इसमें एक अहम भूमिका निभाता है। ऐसे में इन संस्थानों में पढ़ने वाले छात्र-युवा न तो अपने शत्रुओं की सही पहचान कर पाते हैं और न ही अपने मित्रों की; नतीजतन, अक्सर वे प्रतिक्रियावादी शक्तियों के दुष्प्रचार का शिकार बनकर पूँजीपतियों की कठपुतली बन बैठते हैं। यही कारण है कि जब भी फासीवादी ताक़तें सत्ता में आती हैं तो वे शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र को ख़ास तौर पर निशाना बनाती हैं। मोदी सरकार भी यही कर रही है। लेकिन साथ ही नरेन्द्र मोदी साम्प्रदायिक सद्भाव और सभी को साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं!
मोदी की यह रणनीति-कि सारे फासीवादी कृकृत्यों को अंजाम देने के काम को सतत् चलाया जाय मगर औपचारिक बयानों के स्तर पर सेक्युलरिज़्म, सहिष्णुता और ‘साथ चलने’ की बातें की जाय-फासीवादी राजनीति के अतीत के उदाहरणों से भिन्न है। जर्मनी या इटली में फासीवादियों ने सत्ता में आने पर इन सारे कामों को बिना किसी पर्देदारी के अंजाम दिया। कम्युनिस्टों और यहूदियों व प्रवासियों के ख़िलाफ़ उनका फासीवादी नस्लवाद बेलौस, नंगा और बेशर्म था। शिक्षा व्यवस्था और संस्कृति के क्षेत्र में की गयी साज़िशें और विकृतिकरण भी बिना किसी मुखौटे के किये गये थे। लेकिन अतीत में फासीवादी सत्ताओं और पार्टियों का जो हश्र हुआ, उसके मद्देनज़र फासीवादियों ने भी इतिहास से सबक लिया है। अब वे अपने सारे कुकृत्यों को ज़्यादा शातिर तरीके से अंजाम देते हैं। दूसरे शब्दों में, फासीवाद अब पहले से ज़्यादा विचारधारात्मक हो गया है हालाँकि ऐसी पतनशील बुर्जुआ विचारधारा के लिए ज़्यादा विचारधारात्मक होना मुश्किल ही होता है, जैसा कि थियोडोर अडोर्नो ने एक बार कहा था। बहरहाल, मोदी सरकार इसी रणनीति पर काम कर रही हैः यानी सारे व्यावहारिक कामों में फासीवादी मंसूबों पर बेशर्मी के साथ अमल मगर बयानबाज़ी में सेक्युलर, सहिष्णु, बहुलतावादी आदि होने का दावा!
कुछ कार्य मोदी सरकार वही कर रही है जिसके लिए हमेशा पूँजीपति वर्ग फासीवादी बर्बरों को चुनता है। इसीलिए मोदी सरकार की रणनीति का सबसे अहम हिस्सा वह है जिसके लिए कि मोदी को देश के आर्थिक संकट से कराह रहे पूँजीपति वर्ग ने सत्ता में पहुँचाया है। यह काम है मज़दूर वर्ग के अधिकारों और आन्दोलन पर चोट करना, राज्यसत्ता की दमनकारी मशीनरी को चाक-चौबन्द करना और जनता के हको-हुकूक को एक-एक करके छीनना। इसी के लिए मोदी सरकार और तमाम राज्यों में भाजपा की सरकारों ने सबसे पहले श्रम कानूनों को निशाना बनाना शुरू किया है। वैसे तो पहले भी मौजूदा श्रम कानून असंगठित क्षेत्र के मज़दूरों यानी कि ठेका, दिहाड़ी व कैजुअल मज़दूरों के लिए बिरले ही लागू होते थे, लेकिन श्रम कानूनों में इन सुधारों के साथ अब असंगठित क्षेत्र के मज़दूरों का बुनियादी श्रम अधिकारों पर कानूनी दावा भी नहीं रह जायेगा। यानी कि पूँजीपति वर्ग मज़दूरों को बिना किसी कानूनी रुकावट लूटने की पूरी आज़ादी और दूसरी ओर मज़दूरों से संगठित होकर प्रतिरोध करने का हक़ तक छीन लेना! इसके अलावा मोदी सरकार पूँजीपति वर्ग को अन्य प्रकार भी तमाम छूटें भी दे रही है। उसने कम से कम दरों पर ऋण, ज़मीन, पानी और करों से छूट इन पूँजीपतियों को मुहैया करायी है। यानी कि जिन कारणों से पूँजीपति वर्ग ने नरेन्द्र मोदी पर दस हज़ार करोड़ रुपये का निवेश किया था, अब नरेन्द्र मोदी उस काम को मुस्तैदी से कर रहे हैं।
बहरहाल, मौजूदा फासीवादी सरकार की कार्यपद्धति में जो परिवर्तन नज़र आ रहे हैं, वह फासीवादी राजनीति में इक्कीसवीं सदी में आये कुछ परिवर्तनों का ही एक अंग है। इन परिवर्तनों को समझना मज़दूर वर्ग के क्रान्तिकारी आन्दोलन की फासीवाद के प्रतिरोध की रणनीति को निर्धारित करने के लिए ज़रूरी है।
इक्कीसवीं सदी में पूँजीवादी व्यवस्था का संकट और फासीवाद
इतिहास बताता है कि फासीवादी उभार हर-हमेशा इज़ारेदार पूँजीवाद के आर्थिक संकट के दौर में प्रकट होता है। इसका यह अर्थ नहीं है कि आर्थिक कारक यान्त्रिक तरीके से फासीवादी उभार को सुनिश्चित या निर्धारित करते हैं। जैसा कि हमने मौजूदा पुस्तिका में स्पष्ट किया है, हर आर्थिक संकट हमेशा दोहरी सम्भावनाओं को जन्म देता हैः क्रान्तिकारी सम्भावना और प्रतिक्रियावादी सम्भावना। यह किसी भी समाज में प्रतिक्रियावादी शक्तियों और क्रान्तिकारी शक्तियों के सापेक्षिक शक्ति सन्तुलन पर निर्भर करता है कि कौन-सी सम्भावना वास्तविकता में तब्दील होगी या फिर उनके बीच का अन्तरविरोध तात्कालिक तौर पर अनिर्धारित रह जायेगा। इसके अतिरिक्त, जिन समाजों में क्रान्तिकारी शक्तियाँ कमज़ोर होंगी, वहाँ भी फासीवादी विकल्प बुर्जुआ वर्ग के पास मौजूद एकमात्र विकल्प नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो फिर संकट के शिकार ऐसे सभी देशों में फासीवादी शक्तियों को सत्ता में आना चाहिए था जहाँ क्रान्तिकारी शक्तियाँ कमज़ोर थीं। मगर इतिहास में ऐसा नहीं हुआ और वर्तमान दुनिया में भी ऐसा नहीं हो रहा है। इसलिए आर्थिक अन्तरविरोध इस रूप में किसी भी परिघटना के उदय को यान्त्रिक रूप से निर्धारित नहीं करते हैं। जर्मनी और इटली, दोनों ही देशों में फासीवादी विकल्प का चुनाव वहाँ के बुर्जुआ वर्ग का एक राजनीतिक निर्णय था जो कि आर्थिक संकट से प्रेरित था। लेकिन वहाँ के पूँजीपति वर्ग के पास पूँजीवादी दायरे के भीतर ही अन्य विकल्प भी मौजूद थे। यही बात उस दौर में अन्य कई देशों के बारे में कही जा सकती थी। कुछ देशों में बुर्जुआ वर्ग ने फासीवादी विकल्प का चुनाव किया तो कुछ देशों में बुर्जुआ वर्ग ने दूसरे विकल्पों का चुनाव किया। किन देशों में बुर्जुआ वर्ग ने किन विकल्पों का चुनाव किया इसके अलग-अलग विशिष्ट राजनीतिक और ऐतिहासिक कारण थे। अन्तरविरोधों की विशिष्टता को समझे बग़ैर हम अलग-अलग देशों में संकट की अलग-अलग बुर्जुआ प्रतिक्रियाओं को नहीं समझ सकते।
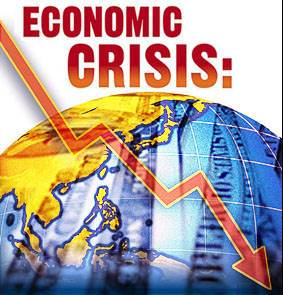 आर्थिक संकट निश्चित तौर पर बुनियादी अन्तरविरोध है, जोकि फासीवादी उभार में हमेशा अपनी भूमिका निभाता है; लेकिन आर्थिक संकट हर-हमेशा फासीवादी उभार में ही परिणत होगा, यह कहना बुनियादी अन्तरविरोध को प्रधान अन्तरविरोध के साथ गड्ड-मड्ड कर देने के समान होगा। बुनियादी अन्तरविरोध का पहलू सामान्य तौर पर अपनी भूमिका निभाता है और किसी भी चरण में सतत् उपस्थित रहता है, लेकिन इतिहास में निश्चित और विशिष्ट सन्धि-बिन्दुओं (conjunctures) को समझने के लिए प्रधान अन्तरविरोध और उसके प्रधान पहलू को समझना आवश्यक होता है। यही कारण है कि कई देशों में (मसलन, इटली, जर्मनी, पुर्तगाल, हंगरी आदि) बुर्जुआ वर्ग ने ऐतिहासिक और राजनीतिक तौर पर निर्धारित प्रधान अन्तरविरोधों के कारण फासीवादी या अर्द्धफासीवादी विकल्प का चुनाव किया, जबकि आर्थिक संकट से उतनी ही बुरी तरह जूझ रहे कई देशों में बुर्जुआ वर्ग ने फासीवादी विकल्प का चुनाव नहीं किया, हालाँकि इन देशों की तथाकथित उदार पूँजीवादी सत्ताओं ने भी मज़दूर वर्ग के हक़ों पर हमलों को संकट के दौर में तीव्र कर दिया था। मगर फिर भी इन पूँजीवादी सत्ताओं और फासीवादी सत्ताओं में फर्क था। इसलिए यह समझना अहम है कि आर्थिक अन्तरविरोध यान्त्रिक तौर पर राजनीतिक घटनाक्रम का निर्धारण नहीं करते हैं।
आर्थिक संकट निश्चित तौर पर बुनियादी अन्तरविरोध है, जोकि फासीवादी उभार में हमेशा अपनी भूमिका निभाता है; लेकिन आर्थिक संकट हर-हमेशा फासीवादी उभार में ही परिणत होगा, यह कहना बुनियादी अन्तरविरोध को प्रधान अन्तरविरोध के साथ गड्ड-मड्ड कर देने के समान होगा। बुनियादी अन्तरविरोध का पहलू सामान्य तौर पर अपनी भूमिका निभाता है और किसी भी चरण में सतत् उपस्थित रहता है, लेकिन इतिहास में निश्चित और विशिष्ट सन्धि-बिन्दुओं (conjunctures) को समझने के लिए प्रधान अन्तरविरोध और उसके प्रधान पहलू को समझना आवश्यक होता है। यही कारण है कि कई देशों में (मसलन, इटली, जर्मनी, पुर्तगाल, हंगरी आदि) बुर्जुआ वर्ग ने ऐतिहासिक और राजनीतिक तौर पर निर्धारित प्रधान अन्तरविरोधों के कारण फासीवादी या अर्द्धफासीवादी विकल्प का चुनाव किया, जबकि आर्थिक संकट से उतनी ही बुरी तरह जूझ रहे कई देशों में बुर्जुआ वर्ग ने फासीवादी विकल्प का चुनाव नहीं किया, हालाँकि इन देशों की तथाकथित उदार पूँजीवादी सत्ताओं ने भी मज़दूर वर्ग के हक़ों पर हमलों को संकट के दौर में तीव्र कर दिया था। मगर फिर भी इन पूँजीवादी सत्ताओं और फासीवादी सत्ताओं में फर्क था। इसलिए यह समझना अहम है कि आर्थिक अन्तरविरोध यान्त्रिक तौर पर राजनीतिक घटनाक्रम का निर्धारण नहीं करते हैं।
मगर फिर भी इतना तो तय है कि फासीवादी सम्भावना के पैदा होने की ज़मीन तैयार करने वाला बुनियादी अन्तरविरोध, विशेष तौर पर इज़ारेदारी के दौर में, पूँजीवादी व्यवस्था का असाध्य आर्थिक संकट ही है। इस सम्भावना का वास्तविकता में तब्दील होना कई अन्य राजनीतिक व ऐतिहासिक कारकों पर निर्भर करता है। लेकिन फासीवादी उभार का आर्थिक संकट से अकाट्य सम्बन्ध है।
बीसवीं सदी में पूँजीवादी व्यवस्था के संकट और इक्कीसवीं सदी में पूँजीवादी व्यवस्था के संकट की तुलना करें तो हम पाते हैं कि उनमें कुछ निश्चित परिवर्तन आये हैं। निश्चित तौर पर, हम आज भी साम्राज्यवाद के युग में जी रहे हैं। लेकिन साम्राज्यवाद का चरण कोई ठहरावग्रस्त या स्थैतिक चरण नहीं हैं। विशेष तौर पर पिछले 70 वर्षों, यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के दौर में विश्व पूँजीवाद की कार्यप्रणाली में कुछ अहम बदलाव आये हैं। इन परिवर्तनों के साथ संकटों के चरित्र और प्रकृति में भी कुछ बदलाव आये हैं। और इन बदलावों के साथ ही विश्व भर में फासीवादी आन्दोलनों के चरित्र और संरचना में भी कुछ बुनियादी परिवर्तन हुए हैं। इन परिवर्तनों को समझना मज़दूर आन्दोलन के लिए कोई अकादमिक या बौद्धिक कसरत नहीं है, बल्कि एक ज़रूरी फौरी सवाल है। इन्हें समझे बिना हम आज के फासीवादी उभार का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। यह समझना नितान्त आवश्यक है कि 1920 या 1930 के दशक के कम्युनिस्ट इण्टरनेशनल में पारित फासीवाद-सम्बन्धी प्रस्तावों को पढ़कर या महान सर्वहारा नेताओं के उस दौर के फासीवाद-विरोधी लेखन को पढ़ कर ही आज के फासीवादी उभार का सर्वहारा प्रतिरोध सम्भव नहीं होगा, हालाँकि उन्हें पढ़े बग़ैर भी यह कार्यभार पूरा नहीं किया जा सकता है।
भूमण्डलीकरण के दौर का यह संकट किन अर्थों में बीसवीं सदी की और विशेष तौर पर 1970 के पहले की आर्थिक मन्दियों से भिन्न है, यह समझने के लिए हमें संक्षेप में 1929 की महामन्दी के बाद विश्व पूँजीवाद की कार्यप्रणाली में हुए परिवर्तनों पर चर्चा करनी होगी।
हम जानते हैं कि द्वितीय विश्वयुद्ध का बुनियादी कारण 1929 में अमेरिका से शुरू हुई वैश्विक महामन्दी और साम्राज्यवाद का संकट था। यह महामन्दी तब तक के इतिहास की सबसे बड़ी पूँजीवादी महामन्दी थी। इसके पहले भी लगभग हर दस-बीस वर्षों के अन्तराल पर पूँजीवादी विश्व गम्भीर आर्थिक संकट का शिकार होता रहा था। लेकिन 1930 के दशक की महामन्दी इस रूप में अलग थी कि यह वित्तीय इज़ारेदार पूँजीवाद के वर्चस्व के मज़बूती के साथ स्थापित होने के बाद की पहली बड़ी मन्दी थी, पूँजीवाद का आम संकट था जो कि किसी एक सेक्टर या क्षेत्र में सीमित नहीं था और इन अर्थों में इसका रूप भी पहले की मन्दी से ज़्यादा विकराल और व्यापक था। कारण यह था कि अति-उत्पादन के संकट से जूझ रहे पूँजीवाद की वित्तीय पूँजी की सट्टेबाज़ी पर निर्भरता विशेष तौर से 1880 के दशक से बुरी तरह से बढ़ गयी थी। इसके कारण पूँजीवादी आर्थिक व्यवस्था पहले से कहीं ज़्यादा खोखली, जर्जर और परजीवी हो चुकी थी और इसका सन्तुलन पहले से कहीं ज़्यादा क्षणभंगुर था। वित्तीय अनुत्पादक पूँजी अब विश्व पूँजीवाद के वाहन की चालक की गद्दी पर काबिज़ हो चुकी थी, जबकि औद्योगिक उत्पादक पूँजी की भूमिका गौण हो चुकी थी। वित्तीय पूँजी बैंक पूँजी और औद्योगिक पूँजी के संलयन से अस्तित्व में आयी थी। उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध से पूँजीवादी व्यवस्था जिस आर्थिक संकट से जूझ रही थी उसका समाधान अब केवल राष्ट्रीय सीमाओं के पार पूँजी के निर्यात से हो सकता था। इसके लिए वित्तीय पूँजी का अस्तित्व में आना अनिवार्य था। लेकिन वित्तीय पूँजी के अस्तित्व में आने के साथ कुछ नयी पूँजीवादी ताक़तों का उदय हुआ जिनके पास आर्थिक शक्तिमत्ता तो थी लेकिन पूँजी के अतिसंचय की समस्या को फौरी तौर पर निपटाने के लिए उनके पास उपनिवेश नहीं थे। इन ताक़तों ने ही दुनिया के पूँजीवादी पुनर्विभाजन के लिए पुरानी साम्राज्यवादी ताक़तों से प्रतिस्पर्द्धा शुरू की जिसकी परिणति दो विश्वयुद्धों में हुई। अति-उत्पादन और अति-संचय के संकट से िनपटने के लिए उत्पादक शक्तियों का बड़े पैमाने पर विनाश ज़रूरी था और इस रूप में इन दो विश्वयुद्धों ने मंदी के संकट से पूँजीवादी विश्व को तात्कालिक तौर पर कुछ राहत दी थी। 1945 में सोवियत संघ के द्वारा नात्सी जर्मनी की पराजय के साथ द्वितीय विश्वयुद्ध का निर्णायक अन्त हो गया था। अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम केवल सोवियत संघ के समक्ष अपने नये हथियार की नुमाइश के लिए गिराया था। युद्ध के अन्त तक यूरोप और जापान खण्डहर में तब्दील हो चुके थे और विश्व पूँजीवाद के नये चौधरी अमेरिका को युद्ध में सबसे कम नुकसान झेलना पड़ा था। अमेरिकी पूँजीपति वर्ग ने इन देशों में पुनर्निर्माण की परियोजनाओं के आधार पर ज़बर्दस्त मुनाफ़ा कमाया।
युद्धोत्तर पुनर्निर्माण परियोजनाओं से पैदा हुई अमेरिकी पूँजीवाद की समृद्धि ने तीन दशकों तक विश्व पूँजीवाद को किसी गम्भीर संकट से बचाये रखा। यह दौर कल्याणकारी पूँजीवादी राज्य, फोर्डवाद, श्रम व पूँजी के बीच समझौते, अर्थव्यवस्था के राजकीय विनियमन, संरक्षणवाद, मौद्रिक अनमनीयता और श्रम बाज़ारों की अनमनीयता का दौर था। लेकिन 1970 के दशक की शुरुआत आते-आते विश्व पूँजीवाद एक बार फिर से अति-उत्पादन और पूँजी के अति-संचय के संकट से ग्रस्त हो चुका था। 1973 में डॉलर-स्वर्ण मानक का टूटने और ओपेक संकट के साथ नयी वैश्विक मन्दी की घण्टी बज गयी। इस मन्दी से निपटने के लिए सभी पूँजीवादी देशों ने मौद्रिक लचीलेपन का रास्ता अपनाया और डॉलर-स्वर्ण मानक का परित्याग कर दिया। डॉलर-स्वर्ण मानक कल्याणकारी राज्य और फोर्डवादी उत्पादन शैली के दौर में पूँजीवाद को एक प्रकार की मौद्रिक स्थिरता देता था। लेकिन पूँजी के अति-संचय के संकट के पैदा होने के साथ यही डॉलर-स्वर्ण मानक पूँजी के लिए एक दमघोंटू पिंजड़ा बन गया था। इसीलिए संकट से निपटने के लिए सबसे पहले अमेरिका ने इस मानक का परित्याग कर दिया ताकि वह मौद्रिक लचीलेपन को अपना कर अपने संकट से तात्कालिक तौर पर निजात पा सके। बाद में अन्य देशों ने भी इस मानक का परित्याग कर दिया। इसके साथ ही विश्व पूँजीवाद की अभूतपूर्व समृद्धि का वह दौर समाप्त हो गया जिसकी पहचान बुर्जुआ कल्याणकारी राज्य, फोर्डवादी उत्पादन शैली, संरक्षणवाद, उन्नत देशों में श्रम और पूँजी के बीच एक समझौते और अनमनीय श्रम बाज़ार व वित्तीय विनियमन के द्वारा की जाती थी। इसके बाद ही नवउदारवादी भूमण्डलीकरण के दौर की शुरुआत होती है। डॉलर-स्वर्ण मानक का टूटना और मौद्रिक लचीलेपन को विभिन्न राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं द्वारा अपनाया जाना महज़ इसकी शुरुआत था।
ज़ाहिर है, नोट छापकर या मुद्रा के मूल्य को ऊपर-नीचे करके अर्थव्यवस्था को बहुत लम्बे समय तक संकट के भँवर से नहीं बचाया जा सकता था। पूरी विश्व पूँजीवादी व्यवस्था में संकट को तात्कालिक तौर पर टालने के लिए भी और ज़्यादा मूलभूत परिवर्तनों की आवश्यकता थी। श्रम बाज़ारों को लचीला बनाने के नाम पर मज़दूर वर्ग द्वारा जीते गये तमाम हक़ों को एक-एक करके वापस लेने की शुरुआत हुई, हालाँकि यह शुरुआत अभी ‘तीसरी दुनिया’ के देशों और विशेष तौर पर लातिन अमेरिकी देशों में की गयी थी। हर प्रकार के राजकीय विनियमन को अब पूँजीवादी संचय में बाधा के तौर पर देखा गया और उसे तिलांजलि देने की शुरुआत कर दी गयी। उत्पादन व पूँजी की प्रचुरता को खपाने के लिए वित्तीय पूँजी का और बड़े पैमाने पर भूमण्डलीकरण हुआ; मन्दी से निपटने के लिए ऋण बाज़ार का विस्तार किया गया और उपभोक्ता वर्ग को निम्न ब्याज़ दरों पर आवास ऋण, कार ऋण आदि देने की पहले से कहीं बड़े पैमाने पर शुरुआत की गयी, ताकि उत्पादन के आधिक्य और पूँजी की प्रचुरता दोनों को खपाया जा सके। नतीजतन, एक ऋण बाज़ार भी अस्तित्व में आया। ऋण स्वयं एक माल में तब्दील हो चुका था और इस माल के विपणन के लिए भी बैंकों व वित्तीय संस्थानों में प्रतिस्पर्द्धा थी। लिहाज़ा, ऋण बाज़ार में भी सन्तृप्ति का एक बिन्दु आना ही था, जिसके बाद इसे और ज़्यादा विस्तारित करने के अलावा पूँजीवाद के पास और कोई रास्ता नहीं था। 2006 के बाद अमेरिका में सबप्राइम ऋण संकट वास्तव में इस ऋण बाज़ार के विस्तारित होने की अन्तिम सीमा तक पहुँचने की निशानी थी। अब ऋण केवल मालदार मध्यवर्ग को नहीं बल्कि ऐसे लोगों को भी दिया जाने लगा जिनके पास ऋण की दो-चार किश्तें चुका सकने योग्य क्षमता भी नहीं थी क्योंकि मालदार मध्यवर्ग का ऋण बाज़ार अब सन्तृप्त हो चुका था। ऐसे ऋणों की ब्याज़ दर को काफ़ी ज़्यादा रखा गया ताकि पहली-दूसरी किश्त तक ही मूलधन से कुछ अधिक की कमाई हो जाये। लेकिन जब व्यापक आबादी में ये सबप्राइम ऋण बाँटे गये, तो बहुत बड़े पैमाने पर आम ग़रीब और निम्न मध्यवर्गीय आबादी पहली और दूसरी किश्त भरने में भी असफल रही और उसने अपने आपको दीवालिया घोषित कर दिया। इसी के साथ अमेरिकी अर्थव्यवस्था में पैदा किया गया आवास बाज़ार का बुलबुला फूट गया और 2007 में शुरू हुए सबप्राइम संकट के साथ 1930 के दशक के बाद की सबसे भयंकर महामन्दी ने पूँजीवादी विश्व को जकड़ लिया और अभी तक यह मन्दी बरक़रार है। यूनान के सम्प्रभु ऋण संकट के रूप में इस समय यह महामन्दी पूरे यूरोपीय संघ और यूरोज़ोन में एक अभूतपूर्व आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक संकट पैदा कर रही है।
लेकिन 2006-07 में शुरू हुई यह महामन्दी कई मायनों में पूँजीवाद के अब तक के इतिहास की सबसे भयंकर मन्दी है। यह न सिर्फ़ अब तक का भयंकरतम आर्थिक संकट है, बल्कि यह पहले के आर्थिक संकटों से गुणात्मक रूप से भिन्न है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि आज की मन्दी किस रूप में पहले के पूँजीवादी संकटों से भिन्न है। सबसे अहम बात यह है कि आज का संकट पहले के सभी संकटों से कहीं ज़्यादा ढाँचागत और गहरा संकट है। भूमण्डलीकरण के दौर में पूँजी दुनिया के उन कोनों तक में व्याप्त हो चुकी है, जो पहले उसकी पहुँच से एक हद तक बाहर थे। लेनिन ने कहा था कि साम्राज्यवाद पूँजीवाद का अन्तिम चरण है। आज कहा जा सकता है कि भूमण्डलीकरण साम्राज्यवाद का अन्तिम चरण है। यह भूमण्डलीकरण के दौर का संकट है और इस रूप में यह पूँजीवाद का अन्तकारी संकट है और पूँजीवाद के ख़त्म होने के साथ ख़त्म होगा।
इसी से जुड़ी हुई दूसरी बात भी है जो कि इस मौजूदा संकट को अतीत में आये अन्य संकटों से अलग करती है। 1870 की दशक में आयी मन्दी हो या फिर 1930 के दशक की महामन्दी, पहले के सभी आर्थिक संकटों के बाद आर्थिक तेज़ी का एक दौर हुआ करता था। लेकिन 1970 की दशक में जो आर्थिक संकट आया उसके बाद विश्व पूँजीवाद ने एक भी तेज़ी का दौर नहीं देखा है। उस दौर से लेकर आज तक दुनिया के सकल घरेलू उत्पाद की दर तीन प्रतिशत के आस-पास या उससे कम रही है, जो कि एक सतत् मन्दी को दिखलाती है। 1970 के दशक से ही विश्व पूँजीवाद एक सतत् मन्द मन्दी का शिकार रहा है। इस मन्दी से उबरने के लिए इसने बीच-बीच में वित्तीय पूँजी की सट्टेबाज़ी के कई बुलबुले पैदा किये। लेकिन सट्टेबाज़ी के हर बुलबुले के फूटने के साथ मन्दी और भी ज़्यादा व्यापक और गम्भीर रूप में फिर से प्रकट हुई। 2006-07 में सबप्राइम ऋण संकट के साथ आवास बाज़ार का बुलबुला फूटा और नतीजे के तौर पर जो आर्थिक संकट पैदा हुआ वह पूँजीवाद के इतिहास का सबसे गम्भीर संकट साबित हो रहा है। यह पहले के सभी संकटों से ज़्यादा ढाँचागत संकट है और इसके बाद किसी वास्तविक तेज़ी की उम्मीद करना पूँजीवादी अर्थशास्त्री भी छोड़ चुके हैं। सट्टेबाज़ी के बुलबुलों और युद्धों के ज़रिये साम्राज्यवाद अपने लिए साँसें उधार ले रहा है। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है साम्राज्यवादी-पूँजीवादी व्यवस्था खुद-ब-खुद ख़त्म हो जाएगी। जब तक सर्वहारा वर्ग अपने हिरावल के नेतृत्व में इसके ख़िलाफ़ इंक़लाबों को अंजाम नहीं देगा, तब तक ये आदमखोर और परजीवी व्यवस्था दुनिया पर बेरोज़गारी, ग़रीबी, युद्ध और पर्यावरणीय विनाश थोप-थोपकर ज़िन्दा रहेगी।
मौजूदा संकट उपरोक्त अर्थों में एक अभूतपूर्व और अद्वितीय संकट है और इसे पूँजीवाद के इतिहास का सबसे गम्भीर और सबसे ढाँचागत संकट कहा जाय तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। मन्दी में अब आकस्मिकता (contingency) या अचानक घटित होने (suddenness) का तत्व नहीं रह गया है या कम-से-कम वह प्रमुख तत्व नहीं रह गया है। यह मौजूदा विश्व पूँजीवाद की स्थायी और संरचनागत परिघटना बन चुकी है। 1930 के दशक की या उससे पहले 1870 के दशक की मन्दी में अचानक घटित होने का एक तत्व था; मानो कोई रास्ते से जा रहा हो और अचानक कोई पेड़ उसके ऊपर गिर पड़े! कहने की आवश्यकता नहीं कि वास्तव में मन्दी कोई आकस्मिक चीज नहीं है, लेकिन कम-से-कम परिघटनात्मक स्तर (phenomenal level) पर इसमें आकस्मिकता का तत्व प्रधान था। यही कारण है कि पहले के गम्भीर आर्थिक संकटों से ठीक पहले जो तेजी के दौर चल रहे थे, उसमें बुर्जुआ अर्थशास्त्री किसी आसन्न मन्दी की सम्भावना को नहीं देख पा रहे थे। ये संकट जब फूटे तो उनके लिए एक अचरज का विषय थे क्योंकि इसका कोई पूर्वानुमान नहीं था। मगर आज ऐसा नहीं है। आज विश्व पूँजीवादी व्यवस्था सतत् मन्दी की शिकार अपनी मृत्युशय्या पर लेटी है और बीच-बीच में वित्तीय सट्टेबाज़ी के स्टेरॉयड के इंजेक्शनों से उसमें कुछ जान आती है। मन्दी के चरित्र में आये इस ऐतिहासिक परिवर्तन के साथ मन्दी के प्रतिक्रियावादी परिणाम के रूप में पैदा होने वाले फासीवादी उभार के चरित्र में भी पहले के मुकाबले कुछ अहम परिवर्तन आये हैं।
1910 के दशक के उत्तरार्द्ध में जब फासीवादी राजनीति का अंकुरण मुख्य रूप से इटली और यूरोप के कई देशों में हो रहा था, तो उसमें भी एक आकस्मिकता का तत्व मौजूद था। इटली में एक मज़बूत सुधारवादी मज़दूर आन्दोलन, 1918-19 के दौरान इटली में मज़दूर परिषदों और सर्वहारा क्रान्ति के प्रयोग के असफल होने और सोवियत संघ में सर्वहारा सत्ता की स्थापना से पूँजीपति वर्ग में पैदा हुए भय और प्रतिक्रिया के कारण फासीवादी राजनीति फल-फूल रही थी। जर्मनी में भी 1920 के दशक के मध्य से यह प्रक्रिया ज़ोर पकड़ चुकी थी और 1919-20 में असफल जर्मन समाजवादी क्रान्ति और रूस में बोल्शेविकों के सत्ता में आने से जर्मन पूँजीपति वर्ग के बदन में पैदा हुई सिहरन भी अभी पूरी तरह से गयी नहीं थी। लेकिन जब 1929 में आर्थिक संकट ने पूँजीपति वर्ग के साँस लेने की जगह को और संकुचित कर दिया, तो फासीवादी और नात्सी राजनीति को पूँजीपति वर्ग का और ज़बर्दस्त समर्थन प्राप्त हुआ और पूँजीपति वर्ग, विशेष तौर पर बड़े पूँजीपति वर्ग ने लगभग एकजुट होकर फासीवादी राजनीतिक विकल्प का चुनाव किया, ताकि संगठित सुधारवादी मज़दूर आन्दोलन का ध्वंस किया जा सके, मुनाफ़े के संकुचन को ख़त्म किया जा सके और हर प्रकार के राजनीतिक विरोध का ख़ात्मा कर संकट के दौर में पूँजीवादी संचय की उत्तरजीविता-योग्य दर को सुनिश्चित किया जा सके।
उस समय यूरोप के कई अन्य देशों में भी फासीवादी आन्दोलनों ने ज़ोर पकड़ा हालाँकि सत्ता हासिल करने में वे सफल नहीं हो पाये, जिसके कि उस देश के इतिहास और राजनीति में निश्चित कारण थे। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि फासीवादी राजनीति का उभार उस दौर में सिर्फ़ जर्मनी या इटली तक ही सीमित नहीं था, बल्कि कुछ देशों को छोड़कर लगभग सभी देशों में फासीवादी राजनीति विविध रूपों में अस्तित्व में आयी थी। लेकिन इन सभी देशों में द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद फासीवादी राजनीति की पकड़ तात्कालिक तौर पर या तो ख़त्म हो गयी थी या फिर इतनी कमज़ोर हो गयी थी कि उन्हें फासीवादी आन्दोलन नहीं कहा जा सकता था, बल्कि बस कुछ फासीवादी गिरोहों की मौजूदगी ही कहा जा सकता था। इसके बाद फासीवादी राजनीति और आन्दोलन के ज़ोर पकड़ने की प्रक्रिया तथाकथित ‘तीसरी दुनिया’ के कई देशों में आर्थिक और राजनीतिक संकट के दौरान घटित होती है। लेकिन आम तौर पर यह कहा जा सकता है कि जहाँ फासीवादी ग्रुप और पार्टियाँ तमाम देशों में आम तौर पर लगभग लगातार मौजूद रहे हैं (चाहें बेहद कमज़ोर रूप में ही क्यों न हों), वहीं दूसरी ओर यह भी सच है कि फासीवाद ने टटपुँजिया वर्गों के बीच एक प्रतिक्रियावादी आन्दोलन का रूप आर्थिक संकट और उसके नतीजे के तौर पर पैदा होने वाले राजनीतिक संकट के दौर में ही लिया है।
एशिया के कई देशों में भी, जिसमें कि भारत भी शामिल है, फासीवादी समूहों या संगठनों की मौजूदगी उनके जन्म के बाद से लगातार बनी रही है। भारत में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इसका क्लासिक उदाहरण है। यह समझना अनिवार्य है कि चूँकि 1940 से 1970 के दशक में आज़ाद हुए तमाम ‘तीसरी दुनिया’ के देशों में जिस किस्म का बौना, विकलांग, रुग्ण और बीमार पूँजीवाद अस्तित्व में आया, जिस किस्म का कमज़ोर पूँजीवादी जनवाद अस्तित्व में आया, जिस किस्म का सतत् रूप से संकटग्रस्त सामाजिक-राजनीतिक ताना-बाना अस्तित्व में आया उसके मद्देनजर वहाँ फासीवादी आन्दोलन और समूहों की निरन्तर सशक्त मौजूदगी की ज़रूरत पूँजीपति वर्ग को कहीं ज़्यादा थी। यही कारण है कि जहाँ हम 1950 के बाद के एक पूरे दौर में यूरोपीय देशों में फासीवादी आन्दोलन की मौजूदगी को किसी महत्वपूर्ण रूप में नहीं देखते हैं, तो वहीं भारत और कुछ ‘तीसरी दुनिया’ के देशों में फासीवादी आन्दोलन अपेक्षाकृत ज़्यादा शक्तिशाली स्थिति में मौजूद था। विश्व अर्थव्यवस्था के साथ ‘तीसरी दुनिया’ के देशों का समेकन 1970 के दशक के बाद विशेष तौर पर बेहद तेज़ी से बढ़ा। नतीजतन, वैश्विक संकट के विश्वव्यापी प्रभाव एक हद तक समतलीकरण हुआ। यही कारण है कि अब फासीवादी संगठन और आन्दोलन की मौजूदगी और उनके उभार की परिघटना का स्वरूप ज़्यादा वैश्विक और समान हो गया है। भारत में 1980 के दशक के अन्त में भूमण्डलीकरण और नवउदारवादी नीतियों की शुरुआत के साथ छोटे उत्पादकों, किसानों और टटपुँजिया वर्गों का उजड़ना और उनके आर्थिक व सामाजिक असुरक्षा में बढ़ोत्तरी के साथ फासीवादी उभार ज़बरदस्त तेज़ी के साथ बढ़ा। जैसा कि हम पहले लिख चुके हैं द्रुत पूँजीवादी विकास से मध्यवर्ती वर्गों के उजड़ने और उनकी आर्थिक-सामाजिक असुरक्षा में बढ़ोत्तरी फासीवादी सामाजिक आन्दोलन के पैदा होने में हमेशा ही एक अहम कारक रहा है। भारत में इस प्रक्रिया को हम 1980 के दशक के अन्त और 1990 के दशक की शुरुआत में शुरू होते हुए देख सकते हैं। यह प्रक्रिया एक नये चरण में आज भी जारी है।
 1980 के दशक के बाद से ही दुनिया भर के देशों में फासीवादी संगठनों और आन्दोलनों की उपस्थिति कहीं तेज़ तो कहीं धीमी रफ़्तार से बढ़ी है। कहीं पर इन आन्दोलनों ने नस्लवादी स्वरूप लिया है, कहीं साम्प्रदायिक तो कहीं प्रवासी-विरोधी। लेकिन अलग-अलग रूपों में इनकी मौजूदगी 1980 के दशक के बाद से ही बढ़ती रही है और नयी सहस्राब्दी की शुरुआत होने के साथ तो इनकी बढ़ोत्तरी और अधिक तेज़ हुई है।
1980 के दशक के बाद से ही दुनिया भर के देशों में फासीवादी संगठनों और आन्दोलनों की उपस्थिति कहीं तेज़ तो कहीं धीमी रफ़्तार से बढ़ी है। कहीं पर इन आन्दोलनों ने नस्लवादी स्वरूप लिया है, कहीं साम्प्रदायिक तो कहीं प्रवासी-विरोधी। लेकिन अलग-अलग रूपों में इनकी मौजूदगी 1980 के दशक के बाद से ही बढ़ती रही है और नयी सहस्राब्दी की शुरुआत होने के साथ तो इनकी बढ़ोत्तरी और अधिक तेज़ हुई है।
1950 के दशक के बाद भी अमेरिका और यूरोप के विभिन्न देशों में खुले और प्रच्छन्न फासीवादी समूह मौजूद थे। मगर उनकी सामाजिक अपील बेहद सीमित थी। वे अक्सर ‘सीक्रेट सोसायटी’ जैसे प्रतिक्रियावादी संगठन हुआ करते थे जो कि प्रवासियों पर, अश्वेतों पर और अन्य अल्पसंख्यकों पर हमले किया करते थे। उनका चरित्र रोगात्मक (pathological), प्रतिक्रियात्मक (reactive), तात्कालिक और मुद्दा-आधारित प्रतिक्रिया का ज़्यादा था न कि एक सुचिन्तित, सुसंगठित विचारधारात्मक और राजनीतिक प्रतिक्रिया का, जो कि योजनाबद्ध रूप से और सचेतन तरीके से मज़दूर-आन्दोलन, कम्युनिस्टों और अल्पसंख्यकों को निशाना बनाते हैं।
वैसे अल्पसंख्यकों को निशाना बनाना वास्तव में फासीवादी राजनीति का सबसे सतही मगर फिर भी ज़रूरी पहलू होता है। मज़दूर आन्दोलन के ध्वंस के लिए और पूँजीवाद द्वारा पैदा की गयी आपदाओं के लिए ज़िम्मेदार ठहराने के लिए फासीवाद को हमेशा ही एक मिथकीय या काल्पनिक शत्रु की, एक ‘फेटिश’ की आवश्यकता होती है। अलग-अलग किस्म के अल्पसंख्यक और अरक्षित समुदाय फासीवादी राजनीति की इस ज़रूरत को अलग-अलग देशों में अलग-अलग तरह से पूरा करते हैं। लेकिन प्रमुख बात यह नहीं है। प्रमुख बात यह है कि फासीवादी विचारधारा, राजनीति और संगठन का असल निशाना कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी और मज़दूर आन्दोलन होता है क्योंकि संकटग्रस्त पूँजीवाद के बचाव और उसकी सेवा के लिए इन दोनों का ख़ात्मा ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है।
ज़ाहिर है, फासीवादी राजनीति की पूँजीपति वर्ग से सापेक्षिक तौर पर ज़्यादा स्वायत्तता होती है और यह पूँजी की प्रतिक्रिया का अतिरेकपूर्ण रूप होने के साथ-साथ टटपुँजिया वर्गों की प्रतिक्रिया का रूमानी उभार भी होता है। इसीलिए फासीवादी राजनीति हमेशा अतिरेकपूर्ण छोरों तक जाती है। दूसरे शब्दों में कहें तो यही कारण है कि फासीवादी राजनीति ऐसे हत्याकाण्डों, जनसंहारों और बर्बरता को अंजाम देती है जिसकी तार्किक या वैज्ञानिक व्याख्या असम्भव प्रतीत होती है। ठीक उसी प्रकार जैसे कि नात्सियों द्वारा यहूदियों, कम्युनिस्टों व अन्य विरोधियों के नरसंहार की व्याख्या में प्रत्यक्षवाद के शिकार समाज-विज्ञानी अपने आपको अक्षम पाते हैं। इसकी व्याख्या करने के लिए ही उनमें एक पूरा अलग स्कूल है जिसे ‘होलोकॉस्ट स्टडीज़’ कहा जाता है। ये उस नरसंहार के मनोवैज्ञानिक पहलुओं आदि पर काफ़ी ज़ोर देते हैं, लेकिन उसकी कोई तार्किक व्याख्या पेश नहीं कर पाते हैं। क्योंकि इस गाँठ को वह जिस छोर को पकड़कर खोलने की कोशिश कर रहे हैं, उसे खींचने से गाँठ और ज़्यादा उलझती है। नात्सियों द्वारा यहूदियों के बर्बर नरसंहार और उसी प्रकार गुजरात में 2002 में हुए बर्बर नरसंहार की व्याख्या एक ऐतिहासिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से की जा सकती है; निश्चित तौर पर, मनोवैज्ञानिक पहलुओं का मूल्यांकन उसमें एक सहायक भूमिका निभा सकता है। मगर अपने आपमें मनोवैज्ञानिक नज़रिये से फासीवादियों के बर्बर और तार्किक व्याख्या से परे लगने वाले कृत्यों का विश्लेषण नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर फासीवादी राजनीति के पूरे चरित्र को समझा जाय तो अतिरेकपूर्ण बर्बरता की ऐतिहासिकता (historicity) और कारणों को समझा जा सकता है। जैसा कि बेर्टोल्ट ब्रेष्ट ने कहा था, “बर्बरता से बर्बरता नहीं पैदा होती; बर्बरता उन व्यावसायिक सौदों से पैदा होती है जिनके लिए बर्बरता की आवश्यकता होती है।”
बहरहाल, हम अभी जिस मूल बात पर ध्यानाकर्षित करना चाहते हैं, वह यह है कि संकट के ज़्यादा ढाँचागत और स्थायी परिघटना में तब्दील होने के साथ, उसकी आकस्मिकता या अचानकपन के पहलू के कम होने के साथ फासीवादी उभार के चरित्र में भी यह परिवर्तन हुआ है कि वह पूँजीवादी व्यवस्था की ‘ऐज़ एण्ड व्हेन नीडेड’ दवाई के समान नहीं रह गया है; वह भी मौजूदा सतत् रूप से संकटग्रस्त पूँजीवादी समाज की एक सतत्, स्थायी और ज़्यादा ढाँचागत परिघटना में तब्दील हो गया है। माइकल कालेकी की वह बात आज पहले हमेशा से ज़्यादा लागू होती है कि फासीवाद जब सत्ता में नहीं भी होता है तो यह पूँजीपति वर्ग का ज़ंजीर से बँधा हुआ कुत्ता होता है।
यही कारण है कि आज फासीवाद के प्रतिरोध की रणनीति भी ज़्यादा स्थायी, सतत्, निरन्तरतापूर्ण और व्यापक होनी चाहिए। फासीवादियों का मुकाबला आज ‘फ़ायर-ब्रिगेड’ शैली में नहीं किया जा सकता है। यानी कि किसी जगह फासीवादियों के किसी कृत्य की सूचना मिली तो फिर क्रान्तिकारी ताक़तें संयुक्त मोर्चा बनाकर उसकी मुख़ालफ़त करने पहुँच गयीं, या फिर किसी जन्तर-मन्तर या आजाद मैदान जैसी जगह पर कोई प्रतीकात्मक प्रदर्शन कर दिया। यह फायर-ब्रिगेड शैली का प्रतिरोध ही आज फासीवादी ताक़तों के विरुद्ध हमें हरा रहा है और हमें कमज़ोर कर रहा है। इसे हमें समझना ही होगा। फासीवाद के प्रतिरोध की हमारी कोई भी प्रभावी रणनीति आज पहले हमेशा से ज़्यादा इस बात की माँग करती है कि हम समाज के विभिन्न मेहनतकश वर्गों और निम्न मध्यवर्गों के बीच, विशेष तौर पर, उनकी बस्तियों में और साथ ही काम करने की जगहों पर भी अपने मज़बूत आधार तैयार करें। यह काम इन इलाकों के दौरे करके नहीं हो सकता। यह काम केवल और केवल सतत् मौजूदगी से और संस्थाबद्ध हस्तक्षेप करके ही हो सकता है। हमें पहले से ही समाज में संघी फासीवादियों द्वारा अपनी तमाम संस्थाओं द्वारा बनायी गयी खन्दकों या अवस्थितियों के समक्ष अपने संस्थागत राजनीतिक व सुधार कार्यों के ज़रिये अपनी खन्दकें या अवस्थितियों का निर्माण करना होगा। केवल इसी रास्ते आज फासीवाद-विरोधी मज़दूर वर्गीय रणनीति सफल हो सकती है।
इसी से जुड़ी हुई बात यह भी है कि आज पहले के मुकाबले कहीं ज़्यादा हद तक फासीवादी ताक़तें और आन्दोलन मज़दूर वर्ग के लिए बुर्जुआ वर्ग की अनौपचारिक राज्यसत्ता (informal state power) का काम करते हैं। फासीवादी ताक़तें सत्ता में रहने पर भी आज के दौर में बहुत से काम उतने खुले और बेशर्म तरीके से नहीं कर पाती हैं, जितने खुले और बेशर्म तरीके से बीसवीं सदी की फासीवादी और नात्सी सत्ताओं ने किया था, जिसके ऐतिहासिक कारणों पर हम ऊपर चर्चा कर चुके हैं। इसलिए समाज में मौजूद फासीवादी गिरोहों के ज़रिये फासीवाद इस कमी को अपने आतंक के अनौपचारिक राज्य को स्थापित करके पूरा करने का प्रयास करता है। मिसाल के तौर पर, मोदी सरकार जो कई सारे काम आधिकारिक तौर पर नहीं कर सकती है, उन्हें समाज में मौजूद फासीवादी ताक़तों द्वारा, जैसे कि बजरंग दल, दुर्गा वाहिनी, विश्व हिन्दू परिषद्, या यहाँ तक कि भाजपा के ही कुछ साधु-सन्त सांसदों और विधायकों द्वारा करवाया जाता है। और जब फासीवादी पार्टी सत्ता में नहीं भी रहती हैं तो समाज में मौजूद फासीवादी गिरोह मज़दूर-आन्दोलन को तोड़ने वाली ताक़तों और पूँजीपति वर्ग के भाड़े के गुण्डा-गिरोहों की भूमिका को निभाते हैं। जो भी लोग देश में क्रान्तिकारी मज़दूर आन्दोलन में सक्रिय हैं वे जानते हैं कि किसी प्रकार हर हड़ताल या मज़दूर संघर्ष के दौरान स्थानीय फासीवादी गुण्डा-गिरोह उनके ख़िलाफ़ काम करते हैं।
एक अन्तिम नुक़्ते पर चर्चा करके हम अगले उपशीर्षक की ओर आगे बढ़ेंगे। भारत और साथ ही दुनिया में कुछ वामपंथी विश्लेषक और संगठन हैं जिनका मानना है कि भारत में मोदी सरकार का आना और तमाम किस्म की भगवा मुहिमों का देश में हावी होना किसी फासीवादी उभार का परिचायक नहीं है। उनमें से कुछ का मानना है कि मौजूदा सरकार एक धुर दक्षिणपंथी प्रतिक्रियावादी सरकार है जिसमें फासीवाद के तत्व हैं। कुछ अन्य का मानना है कि यह ‘नवउदारवादी पूँजी की प्रतिक्रियावादी तानाशाही’ है। संघ परिवार और मोदी सरकार को सीधे फासीवादी न मानने या अर्द्ध-फासीवादी मानने के पीछे एक अनैतिहासिक नज़रिया काम करता है। यह नज़रिया बीसवीं सदी के फासीवादी और नात्सी आन्दोलनों और सत्ताओं से आज के फासीवादी उभार का सादृश्य निरूपण करता है और जब उसे उस सादृश्य निरूपण के आधार पर तमाम असमानताएँ मिलती हैं या कुछ अधूरी तुलनाएँ मिलती हैं, तो वह इस नतीजे पर पहुँचता है कि मौजूदा फासीवादी उभार वास्तव में फासीवादी उभार नहीं है या पर्याप्त रूप से फासीवादी उभार नहीं है। या फिर अतीत के उदाहरणों के आधार पर फासीवाद की एक बेहद संकीर्ण परिभाषा तैयार की जाती है और जो फासीवादी उभार उस परिभाषा की सभी शर्तों को पूरा नहीं करता, उसे फासीवादी उभार नहीं माना जाता। हमारे दृष्टिकोण से यह पूरा नज़रिया इस बात को नहीं समझता कि सर्वहारा वर्ग की राजनीति के साथ-साथ पूँजीपति वर्ग की प्रतिक्रियावादी राजनीति भी ऐतिहासिक परिवर्तनों से होकर गुज़रती है; वह भी अपने अतीत से सबक लेती है और नये ऐतिहासिक सन्दर्भ में नये रूपों राजनीतिक, विचारधारात्मक और सांगठनिक रूपों को जन्म देती है। वाल्टर बेंजामिन के शब्दों का इस्तेमाल करें तो फासीवादी राजनीति भी ‘रिडेम्प्टिव एक्टिविटी’ (redemptive activity) करती है। अगर इस ऐतिहासिक नज़रिये से फासीवादी राजनीति और संगठन में आये बदलावों की समीक्षा न करें और अपने विश्लेषण को सादृश्य निरूपणों पर आधारित कर दें तो न तो फासीवादी राजनीति के इतिहास में निरन्तरता के पहलुओं की पहचान की जा सकती है और न ही विच्छेद के पहलुओं की। इसलिए सर्वहारा वर्ग के दृष्टिकोण से किये जाने वाले विश्लेषण को जहाँ फासीवादी राजनीति में आये तमाम परिवर्तनों को सही ऐतिहासिक सन्दर्भ में रखकर उनकी व्याख्या करनी चाहिए, वहीं उसे इन परिवर्तनों से विस्मित होकर फासीवादी राजनीति को पहचानने से इंकार नहीं करना चाहिए।
पूँजीवादी आर्थिक संकट और फासीवादी उभार के आर्थिक नियतत्ववादी विश्लेषण की सीमाएँ
कई यान्त्रिक और आर्थिक नियतत्ववादी विश्लेषक पूँजीवादी आर्थिक संकट और फासीवादी उभार के बीच एक ‘दो दूनी चार’ का या समानुपातिकता का सम्बन्ध देखते हैं। ऐसे विश्लेषण आपको असमाधेय अन्तरविरोधों के ढेर में ले जाकर गिरा देते हैं। इस प्रकार के विश्लेषण ऐसे नतीजों पर पहुँचाते हैं कि आर्थिक संकट लगभग अनिवार्य रूप में फासीवादी राजनीति के उदय में परिणत होते हैं। लेकिन ऐसा कोई भी दृष्टिकोण इस बात की व्याख्या नहीं कर पाता है कि आख़िर आर्थिक संकट ने अतीत में और वर्तमान में वैश्विक चरित्र होने के बावजूद सभी देशों में सशक्त फासीवादी आन्दोलनों और सत्ताओं को जन्म क्यों नहीं दिया? यह सच है कि आर्थिक संकटों ने लगभग हर देश में किसी न किसी प्रकार की पूँजीवादी प्रतिक्रिया को पालने-पोसने का काम किया। लेकिन हर पूँजीवादी प्रतिक्रिया को फासीवाद का नाम नहीं दिया जा सकता है। मिसाल के तौर पर, सैनिक हुण्टाएँ और अन्य प्रकार तानाशाह सत्ताएँ भी कई देशों में संकट के दौर में अस्तित्व में आयीं। कइयों को बिखरे हुए फासीवादी समूहों का समर्थन भी प्राप्त था। लेकिन वे सत्ताएँ अपने आप में फासीवादी सत्ताएँ नहीं थीं। अपने विश्लेषण की तमाम गम्भीर सीमाओं के बावजूद इतालवी कम्युनिस्ट और बाद में संशोधनवादी पामीरो तोग्लियाती की यह चेतावनी बिल्कुल सही है कि कम्युनिस्टों में हर प्रकार की प्रतिक्रियावादी पूँजीवादी सत्ताओं को फासीवादी क़रार दे देने की प्रवृत्ति होती है जो बेहद घातक होती है क्योंकि यह सर्वहारा वर्ग को एक कारगार फासीवाद-विरोधी रणनीति बनाने की आज्ञा नहीं देती है। फासीवादी प्रतिक्रिया अन्य प्रकार की पूँजीवादी प्रतिक्रियाओं जैसे कि सैन्य तानाशाही या अन्य प्रकार की संसदीय तानाशाहियों से इस मायने में भिन्न होती है है कि यह टटपुँजिया वर्गों के एक प्रतिक्रियावादी, कट्टरतावादी सामाजिक आन्दोलन के रूप में अस्तित्व में आती है। यह बड़ी पूँजी की नग्न तानाशाही को स्थापित करती है हालाँकि इसका सामाजिक आधार टटपुँजिया वर्गों, सफेद कॉलर के मज़दूरों, लम्पट टटपुँजिया और लम्पट मज़दूर वर्ग के बीच होता है। इसलिए आर्थिक संकट आम तौर पर पूँजीवादी प्रतिक्रिया को जन्म देता है और यह पूँजीवादी प्रतिक्रिया कई किस्म के रूप में सामने आ सकती है, जिसमें से फासीवाद केवल एक रूप है। निकोस पुलान्तज़ास ने इसी बात को इस रूप में कहा है कि उदार पूँजीवादी जनवाद के अलावा तीन प्रकार की अपवादस्वरूप पैदा होने वाली पूँजीवादी राज्यसत्ताएँ या पूँजीपति वर्ग के अधिनायकत्व के तीन अपवादस्वरूप रूप होते हैं: फासीवादी राज्यसत्ता, सैन्य तानाशाही और बोनापार्तवादी सत्ता।
बहरहाल, आर्थिक संकट और फासीवादी उभार के बीच समानुपातिक आर्थिक रिश्ता कायम करने वाले विश्लेषण की सीमाओं को समझने के लिए यह समझना ज़रूरी है कि आर्थिक संकट किस प्रकार प्रतिक्रियावादी सम्भावना को जन्म देता है; किस प्रकार प्रतिक्रियावादी सम्भावना के साथ ही एक ऐतिहासिक रूप से प्रगतिशील सम्भावना भी आर्थिक संकट के एक परिणाम के तौर पर सामने आती है; किस प्रकार प्रतिक्रियावादी सम्भावना हर-हमेशा फासीवादी प्रतिक्रिया में परिणत नहीं होती है; और किसी प्रकार क्रान्तिकारी सम्भावना के वास्तविकता में तब्दील न होने पर अलग-अलग प्रकार की विशिष्ट राजनीतिक-ऐतिहासिक स्थितियों की मौजूदगी के कारण अलग-अलग किस्म की पूँजीवादी प्रतिक्रियाओं की सम्भावनाएँ वास्तविकता में तब्दील हो सकती हैं। इसके लिए पूँजीवादी राज्य के प्रकार्यों और उनकी पूर्ति की शर्तों को समझना ज़रूरी है।
पूँजीवादी राज्यसत्ता का सबसे अहम कार्य होता है पूँजीवादी समाज के उत्पादन सम्बन्धों के राजनीतिक व वैधिक रूपों को रेखांकित करना, उनकी हिफ़ाज़त करना और पूँजीपति वर्ग के सामूहिक वर्ग हितों को संगठित करना और उन्हें “राष्ट्रीय हितों” के रूप में पेश करना। जब पूँजीवादी राज्यसत्ता यह कार्य करने में अक्षम होती है तब पूँजीवादी राज्य का संकट पैदा होता है। आर्थिक संकट के दौर में मुनाफ़े की ख़तरनाक हदों तक गिरती दरों और आपसी गलाकाटू प्रतिस्पर्द्धा के कारण पूँजीपति वर्ग अपनी राज्यसत्ता के ज़रिये राजनीतिक तौर पर संगठित हो पाने में कई बार असफल हो जाता है। इसके कारण वह अपने वर्ग हितों को “राष्ट्र” के हितों के तौर पर जनता के सामने पेश करने में भी असफल हो जाता है। परिणामतः पूँजीवादी राज्यसत्ता और पूँजीवादी शासक वर्ग अपना सामाजिक आधार खोने लगते हैं। पूरी पूँजीवादी व्यवस्था का वर्चस्व खण्डित होने लगता है; दूसरे शब्दों में पूँजीपति वर्ग के शासन की वैधता संकट में पड़ जाती है। उदार पूँजीवादी राज्यसत्ता को जिस प्रकार का और जिन कारणों से एक सामाजिक आधार प्राप्त होता है वह संकट के दौर में पूँजीवादी संचय के लिए एक बाधा बन जाता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार संयुक्त प्रगतिशील गठबन्धन सरकार के, विशेष तौर पर, पहले कार्यकाल के कल्याणकारी लोकरंजकतावाद के दौरान जो झुनझुने जनता को थमाये गये थे (मसलन, ग्रामीण रोज़गार गारण्टी अधिनियम, सूचना अधिकार कानून, शिक्षा का अधिकार इत्यादि) उन दिखावटी झुनझुनों का ख़र्च उठाने में भी संकट के दौर में भारतीय पूँजीवादी राज्य अक्षम था; इन ख़र्चीले झुनझुनों की मौजूदगी के कारण भारतीय पूँजीपति वर्ग और उसकी राज्यसत्ता के सामने कई प्रकार के संकट उत्पन्न हो रहे थे। ऐसे में, पूँजीपति वर्ग की आपसी प्रतिस्पर्द्धा भी एक ऐसी दिशा में विकसित हो रही थी, जिसके कारण उसके राजनीतिक तौर पर संगठित होने और अपने वर्ग हितों को “राष्ट्र” के हितों के तौर पर पैकेज करने के कार्यभार का निपटारा होना मुश्किल होता जा रहा था। विशालकाय घोटालों का घटित होना केवल इस संकट की एक अभिव्यक्ति मात्र था। ऐसे में, पूँजीपति वर्ग के सामूहिक वर्ग हितों को कोई ऐसी राज्यसत्ता ही संगठित कर सकती है, जिसकी पूँजीपति वर्ग से सापेक्षिक स्वायत्तता अपेक्षाकृत ज़्यादा हो; जो पूँजीपति वर्ग को वह सामाजिक आधार मुहैया करा सके, जिसे पूँजीपति वर्ग संकट के दौर में आपसी अन्तरविरोधों के कारण खोने लगता है। दक्षिणपंथी लोकरंजकता के विभिन्न संस्करणों की ज़मीन एक ऐसे दौर में ही पैदा होती है।
एक ऐसी स्थिति में ही हमारे देश में दक्षिणपंथी लोकरंजकता के विभिन्न संस्करण तैयार हुए हैं या मज़बूत हुए हैं, जिनमें से एक था ‘आम आदमी पार्टी’ का धुर दक्षिणपंथी लोकरंजकतावाद, जिसे सीधे तौर पर फासीवादी तो नहीं क़रार दिया जा सकता, लेकिन निश्चित तौर पर इसमें फासीवादी तत्वों की मौजूदगी से इंकार भी नहीं किया जा सकता है। दूसरा था भारत के क्लासिकीय फासीवादी संघ परिवार और भाजपा की राजनीति और प्रतिक्रियावादी आन्दोलन का उभार। हमने पहले भी किसी और जगह इंगित किया है कि इसमें से पहले वाली राजनीतिक धारा यानी ‘आम आदमी पार्टी’ की राजनीति कम-से-कम इसी रूप में मौजूद नहीं रह सकती है, जिस रूप में वह आज मौजूद है। या तो ‘आम आदमी पार्टी’ अपने ‘विशिष्ट बिक्री गुण’ को खोकर किसी भी आम पूँजीवादी पार्टी में तब्दील हो जायेगी (जिस सूरत में वह अन्ततः विसर्जित ही होगी) या फिर वह विसर्जित होकर भाजपा और संघ परिवार के फासीवादी उभार में ही इज़ाफ़ा करने का काम करेगी। जो भी हो यह आराम से कहा जा सकता है कि इन दोनों धुर-दक्षिणपंथी उभारों में ज़्यादा स्थायी और टिकाऊ उभार संघ परिवार की फासीवादी राजनीति और आन्दोलन का उभार ही है।
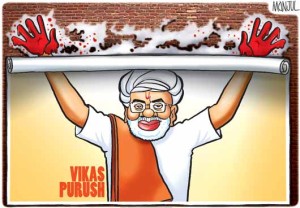 बहरहाल, भारतीय पूँजीपति वर्ग द्वारा मोदी के विकल्प का चुनाव एक राजनीतिक फैसला था न कि शुद्धतः आर्थिक फैसला। हालाँकि राजनीति और आर्थिक पहलुओं के बीच कोई चीन की दीवार नहीं होती है। जैसा कि लेनिन ने कहा था, ‘राजनीति अर्थशास्त्र की सर्वाधिक सान्द्र अभिव्यक्ति होती है।’ निश्चित तौर पर, यह राजनीतिक फैसला आर्थिक संकट से प्रेरित था। लेकिन यह कहना अतिशयोक्ति होगा कि पूँजीपति वर्ग केवल यही फैसला ले सकता था। अभी पूँजीवादी दायरे के भीतर भी अन्य प्रतिक्रियावादी विकल्प मौजूद थे जिनका भारतीय पूँजीपति वर्ग चुनाव कर सकता था। वास्तव में, अगर हम आर्थिक नीतियों की बात करें तो संयुक्त प्रगतिशील गठबन्धन सरकार के दूसरे कार्यकाल की नीतियों और मौजूदा मोदी सरकार की नीतियों में परिमाणात्मक अन्तर ही मौजूद है, हालाँकि मोदी सरकार अपने श्रम-विरोधी एजेण्डे को ज़्यादा आक्रामक और खुले तरीके से लागू कर रही है और किसी भी प्रकार के प्रतिरोध के भीषण दमन के लिए ज़्यादा प्रतिबद्ध है। मगर आतंकवाद-रोधी कानून, ऑपरेशन ग्रीन हण्ट, श्रम कानूनों में सुधार से लेकर नर्म केसरिया लाइन, साम्राज्यवाद के साथ समझौते कर देश के संसाधनों की खुली लूट की छूट देने तक के मामले में कांग्रेस-नीत संप्रग गठबन्धन किसी भी रूप में भाजपा सरकार से ज़्यादा पीछे नहीं था। लेकिन आर्थिक संकट का असर उन पूँजीपति वर्गों में ज़्यादा तेज़ी से भयाक्रान्तता का माहौल तैयार करता है जिनका आर्थिक सन्तुलन ज़्यादा नाजुक हो और जिनका जनवादी चरित्र या तो अनुपस्थित हो या फिर न होने की हद तक कमज़ोर और क्षणभंगुर हो। भारत के पूँजीपति वर्ग के बारे में ये दोनों ही बातें लागू होती हैं। इसलिए यह संकट के दबाव में जल्दी भयाक्रान्त होता है, इसमें जल्दी भगदड़ मचती है, यह जल्दी अपने राजनीतिक संगठन व एका को खो बैठता है और इसीलिए यह कहीं जल्दी फासीवादी विकल्प को चुनने की ओर अग्रसर होता है। साथ ही, भारतीय समाज के टटपुँजिया वर्गों के फासीवादी रूपान्तरण की सम्भावना-सम्पन्नता भी आज के यूरोपीय देशों के टटपुँजिया वर्ग की अपेक्षा कहीं ज़्यादा है। इसलिए फासीवाद भारत के पूँजीपति वर्ग को ज़्यादा तेज़ी के साथ अपने टटपुँजिया उभार के ज़रिये तात्कालिक तौर पर एक सामाजिक आधार मुहैया करा सकता है। इस रूप में भारत में फासीवादी उभार के कुछ विशिष्ट राजनीतिक और ऐतिहासिक कारण हैं जिन्हें समझना बेहद ज़रूरी है और केवल आर्थिक संकट के उपोत्पाद के रूप में उसका चित्रण हर-हमेशा बेहद सीमित होगा और आज के दौर में जो राजनीतिक सन्धि-बिन्दु उपस्थित है, उसकी कारणात्मक व्याख्या नहीं कर पायेगा।
बहरहाल, भारतीय पूँजीपति वर्ग द्वारा मोदी के विकल्प का चुनाव एक राजनीतिक फैसला था न कि शुद्धतः आर्थिक फैसला। हालाँकि राजनीति और आर्थिक पहलुओं के बीच कोई चीन की दीवार नहीं होती है। जैसा कि लेनिन ने कहा था, ‘राजनीति अर्थशास्त्र की सर्वाधिक सान्द्र अभिव्यक्ति होती है।’ निश्चित तौर पर, यह राजनीतिक फैसला आर्थिक संकट से प्रेरित था। लेकिन यह कहना अतिशयोक्ति होगा कि पूँजीपति वर्ग केवल यही फैसला ले सकता था। अभी पूँजीवादी दायरे के भीतर भी अन्य प्रतिक्रियावादी विकल्प मौजूद थे जिनका भारतीय पूँजीपति वर्ग चुनाव कर सकता था। वास्तव में, अगर हम आर्थिक नीतियों की बात करें तो संयुक्त प्रगतिशील गठबन्धन सरकार के दूसरे कार्यकाल की नीतियों और मौजूदा मोदी सरकार की नीतियों में परिमाणात्मक अन्तर ही मौजूद है, हालाँकि मोदी सरकार अपने श्रम-विरोधी एजेण्डे को ज़्यादा आक्रामक और खुले तरीके से लागू कर रही है और किसी भी प्रकार के प्रतिरोध के भीषण दमन के लिए ज़्यादा प्रतिबद्ध है। मगर आतंकवाद-रोधी कानून, ऑपरेशन ग्रीन हण्ट, श्रम कानूनों में सुधार से लेकर नर्म केसरिया लाइन, साम्राज्यवाद के साथ समझौते कर देश के संसाधनों की खुली लूट की छूट देने तक के मामले में कांग्रेस-नीत संप्रग गठबन्धन किसी भी रूप में भाजपा सरकार से ज़्यादा पीछे नहीं था। लेकिन आर्थिक संकट का असर उन पूँजीपति वर्गों में ज़्यादा तेज़ी से भयाक्रान्तता का माहौल तैयार करता है जिनका आर्थिक सन्तुलन ज़्यादा नाजुक हो और जिनका जनवादी चरित्र या तो अनुपस्थित हो या फिर न होने की हद तक कमज़ोर और क्षणभंगुर हो। भारत के पूँजीपति वर्ग के बारे में ये दोनों ही बातें लागू होती हैं। इसलिए यह संकट के दबाव में जल्दी भयाक्रान्त होता है, इसमें जल्दी भगदड़ मचती है, यह जल्दी अपने राजनीतिक संगठन व एका को खो बैठता है और इसीलिए यह कहीं जल्दी फासीवादी विकल्प को चुनने की ओर अग्रसर होता है। साथ ही, भारतीय समाज के टटपुँजिया वर्गों के फासीवादी रूपान्तरण की सम्भावना-सम्पन्नता भी आज के यूरोपीय देशों के टटपुँजिया वर्ग की अपेक्षा कहीं ज़्यादा है। इसलिए फासीवाद भारत के पूँजीपति वर्ग को ज़्यादा तेज़ी के साथ अपने टटपुँजिया उभार के ज़रिये तात्कालिक तौर पर एक सामाजिक आधार मुहैया करा सकता है। इस रूप में भारत में फासीवादी उभार के कुछ विशिष्ट राजनीतिक और ऐतिहासिक कारण हैं जिन्हें समझना बेहद ज़रूरी है और केवल आर्थिक संकट के उपोत्पाद के रूप में उसका चित्रण हर-हमेशा बेहद सीमित होगा और आज के दौर में जो राजनीतिक सन्धि-बिन्दु उपस्थित है, उसकी कारणात्मक व्याख्या नहीं कर पायेगा।
इस सन्दर्भ में पूँजीवादी व्यवस्था के तहत राज्यसत्ता और राजनीति की इस सापेक्षिक स्वायत्तता को समझना बेहद ज़रूरी है। हर वर्ग समाज में राज्यसत्ता का कार्य होता है उस समाज के उत्पादन सम्बन्धों को कानूनी जामा पहनाना और उसकी हिफ़ाज़त करना या उसे कायम रखना। लेकिन पूँजीवादी समाज अपने से पहले के समाजों से इस मायने में भिन्न होता है कि यह आर्थिक शोषण पर आधारित होता है, आर्थिकेतर उत्पीड़न पर नहीं। यहाँ आर्थिक प्रक्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए किसी प्रत्यक्ष राजनीतिक हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती है, जैसा कि सामन्तवाद में होता है। इसलिए पूँजीवादी राज्यसत्ता और पूँजीवादी राजनीति पूँजीवादी समाज में जारी उत्पादन व आर्थिक गतिविधियों से सापेक्षिक रूप से स्वायत्त होते हैं, हालाँकि अन्तिम विश्लेषण में किसी भी पूँजीवादी समाज में पूँजीवादी राज्यसत्ता को पूँजीवादी उत्पादन सम्बन्धों, मुनाफ़े और पूँजी संचय के जारी रहने को सुनिश्चित करना होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो अन्तिम विश्लेषण में पूँजीवादी राज्यसत्ता को पूँजीवादी उत्पादन सम्बन्धों के पुनरुत्पादन को सुनिश्चित करना होता है। लेकिन पूँजीवादी राज्यसत्ता यह कार्य वर्चस्व की अपनी प्रणाली के द्वारा करती है। पूँजीपति वर्ग केवल अपनी राज्यसत्ता के द्वारा ही एक वर्ग के तौर पर राजनीतिक रूप से संगठित होता है, या कहें कि अपने वैयक्तिक पूँजीवादी हितों से ऊपर उठकर अपने सामूहिक पूँजीवादी वर्ग हितों की मंज़िल तक पहुँचता है। राज्यसत्ता जब भी पूँजीपति वर्ग के वैयक्तिक सदस्यों के साथ अपनी निकटता को छिपा नहीं पाती तो यह उसकी भारी असफलता होती है और उसकी वैधता को कमज़ोर करती है। दूसरे शब्दों में, पूँजीवादी राज्यसत्ता अगर पूँजीपति वर्ग के वैयक्तिक सदस्यों से दूरी को प्रदर्शित करने में असफल होगा तो वह पूँजीपति वर्ग के हितों को राजनीतिक तौर पर संगठित कर पाने और उनकी नुमाइन्दगी कर पाने की क्षमता खोता जायेगा। वैयक्तिक पूँजीपतियों से दूरी को प्रदर्शित करके ही पूँजीवादी राज्यसत्ता पूँजीपति वर्ग के सामूहिक वर्ग हितों को संगठित कर सकती है और उसे “राष्ट्रीय हित” के तौर पर जनता के बीच पेश कर वैधता अर्जित कर सकती है, और इसके लिए पूँजीवादी राज्यसत्ता को कई बार पूँजीपति वर्ग के वैयक्तिक सदस्यों की इच्छा के विपरीत कार्य भी करना होता है। यह पूँजीवादी राज्यसत्ता का सबसे अहम कार्य होता है।
इसी के साथ पूँजीवादी राज्यसत्ता का दूसरा सबसे अहम कार्य जुड़ा हुआ है। यह दूसरा कार्यभार है मज़दूर वर्ग व अन्य शासित मेहनतकश वर्गों को विसंगठित रखना, उन्हें लगातार वैयक्तिक या आणविकीकृत (atomized) व्यक्तियों के रूप में बनाये रखना। दूसरे शब्दों में कहें तो उन्हें ‘नागरिक’ के रूप में, बुर्जुआ “राष्ट्र” के एक अंग या सदस्य के रूप में उत्पादित व पुनरुत्पादित करना (बड़े विस्मय की बात है कि सर्वहारा राजनीति का अगुवा होने का दावा करने वाला एक अर्थवादी और अराजकतावादी-संघाधिपत्यवादी संगठन ‘नागरिक’ नाम से अपना मुखपत्र निकालता है, जो कि उसकी अधकचरी और दरिद्र ऐतिहासिक समझदारी को दिखलाता है; नागरिकता का पूरा विमर्श ही वास्तव में बुर्जुआ जनवादी क्रान्तियों के दौर में पैदा हुआ था और आज इस विमर्श की कोई विशिष्ट प्रगतिशील सम्भावना शेष नहीं रह गयी है)।
पूँजीवादी राज्य को पूँजीवादी आर्थिक सम्बन्धों के कानूनी औपचारिकीकरण और उनके सांगठनिक ढाँचे को तैयार करने और पूँजीवादी उत्पादन को सम्भव बनाने के लिए अवसरंचनात्मक ढाँचा तैयार करने के अलावा संकटों को टालने के लिए आर्थिक विनियमन करने, श्रम और पूँजी के बीच के अन्तरविरोधों को ख़तरनाक हदों तक विकसित होने से रोकने के लिए राजकीय हस्तक्षेप द्वारा उन्हें विनियमित करने और साथ ही कल्याणकारी नीतियों और जुमलों के ज़रिये और साथ ही राष्ट्रीय कट्टरवाद के ज़रिये अपने शासन की ख़ातिर जनता की सहमति का निर्माण भी करना होता है। इनमें से विशेष तौर पर बाद के तीन कार्यों को पूरा करने के लिए उसे कभी-कभी पूँजीपति वर्ग के बहुलांश की इच्छाओं की अवहेलना भी करनी पड़ती है। लेकिन पहले दो कार्यों के लिए उसे पूँजीपति वर्ग के प्रत्यक्ष सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। इन सारे प्रकार्यों के निष्पादन के लिए पूँजीवादी राज्यसत्ता को आर्थिक संसाधनों के साथ ही साथ न सिर्फ़ जनता की सहमति की आवश्यकता पड़ती है, बल्कि पूँजीपति वर्ग के भी प्रत्यक्ष सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। ज़ाहिर है, इसके लिए अर्थव्यवस्था में लगातार वृद्धि, यानी कि स्वस्थ व सतत् पूँजीवादी मुनाफ़े की, और साथ ही सामाजिक जीवन स्तर में बेहतरी की आवश्यकता होती है जो कि जनता के बीच सहमति का निर्माण कर सके और पूँजीपति वर्ग के सहयोग को सुनिश्चित कर सके। लेकिन आर्थिक संकट के दौर में राज्यसत्ता के पास ये सारी सहूलियतें नहीं रह जाती हैं। आर्थिक संकट के दौरों में जनता के व्यापक जनसमुदायों के बीच सहमति के निर्माण की प्रक्रिया को पूँजी संचय को जारी रखते हुए चलाना बेहद मुश्किल होता जाता है। दूसरे शब्दों में, पूँजीपति वर्ग के पूँजी संचय को सुनिश्चित करना और जनता के बीच पूँजीवादी शासन की वैधता को बरक़रार रखना एक साथ असम्भव हो जाता है। विशेष तौर पर, अगर किसी मज़बूत सुधारवादी मज़दूर आन्दोलन का दबाव हो तो आर्थिक संकट का असर पूँजीपति वर्ग पर और भी ज़्यादा ज़बर्दस्त होता है, जैसा कि इटली और जर्मनी में हुआ। ऐसे में, पूँजीपति वर्ग की प्रतिक्रिया का फासीवादी रूप लेने की सम्भावना ज़्यादा प्रबल होती है। अगर मज़दूर वर्ग की राजनीति क्रान्तिकारी विकल्प को न अपनाकर सुधारवादी, अर्थवादी, संशोधनवादी और ट्रेड यूनियनवादी विकल्प को अपनाती है, तो वास्तव में वह फासीवादी उभार और प्रतिक्रिया को बढ़ावा देने का ही काम करती है। ऐसी सुधारवादी मज़दूर राजनीति न तो पूँजीवादी व्यवस्था के आगे जाने की बात करती है और न ही पूँजीवादी व्यवस्था के लिए साँस लेने की जगह छोड़ती है, जिसका नतीजा होता है पूँजीवादी प्रतिक्रिया जो कि फासीवादी रूप भी ले सकती है।
फासीवादी उभार और टटपुँजिया वर्गों की भूमिका का प्रश्न
हमने प्रस्तुत पुस्तिका में लिखा है कि फासीवादी उभार का प्रमुख सामाजिक आधार तमाम टटपुँजिया वर्ग होते हैं। हमने यह भी स्पष्ट किया है कि पूँजीवादी लूट और मुनाफ़े के कारण उजड़ते हुए टटपुँजिया वर्ग में फासीवादी प्रचार का शिकार होने की सम्भावना होती है; बर्बाद होता हुआ टटपुँजिया वर्ग यदि अपनी बर्बादी के कारणों को नहीं समझता तो फिर फासीवाद उसके सामने एक मिथ्या शत्रु खड़ा करने में सफल होता है और यह मिथ्या शत्रु होता है मज़दूर वर्ग और उसका आन्दोलन और साथ ही धार्मिक, नस्लीय, जातीय या किसी भी किस्म की अल्पसंख्यक आबादी, जिसे ‘बाहरी’, ‘अन्य’, ‘भिन्न’ आदि के रूप में चित्रित करके एक ख़तरे के तौर पेश किया जा सके। इस वर्ग के भीतर एक किस्म के अन्धराष्ट्रवाद को भड़काना, तानाशाही के लिए समर्थन पैदा करना और वास्तव में अपने ही आर्थिक और राजनीतिक हितों के ख़िलाफ़ जाते हुए फासीवादी बर्बरता की हिमायत करने और उसका उपकरण बनने की सम्भावनासम्पन्नता मौजूद होती है। साथ ही, हमने यह भी स्पष्ट किया था कि सामाजिक-जनवादियों यानी संसदीय वामपंथियों के अर्थवाद और सुधारवाद के कारण भी मज़दूर आन्दोलन एक राजनीतिक रवैया नहीं अपना पाता। इसके कारण वह निम्न मध्यवर्ग के विभिन्न संस्तरों को अपने साथ लाने का प्रयास नहीं करता, जिसके कारण ये वर्ग फासीवादी प्रचार के समक्ष अरक्षित होते हैं। एक प्रकार से चाहे क्रान्तिकारी कम्युनिस्टों के नेतृत्व में हो या फिर ग़द्दार संशोधनवादियों के नेतृत्व में, अर्थवादी व ट्रेडयूनियनवादी मज़दूर आन्दोलन फासीवाद को इस बात की इजाज़त दे देता है कि वह टटपुँजिया वर्गों की फासीवादी गोलबन्दी कर उसे मज़दूर आन्दोलन के विरुद्ध एक प्रति-सन्तुलनकारी शक्ति या प्रतिभार (बटखरे) के रूप में इस्तेमाल करे। यह स्पष्ट करना ज़रूरी है कि अर्थवाद और ट्रेडयूनियनवाद की यह ग़लती केवल संसदीय वामपंथियों तक नहीं सीमित है बल्कि क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट आन्दोलन में भी इस प्रकार के अर्थवाद का असर है। जैसा कि लेनिन ने लिखा था, ‘अर्थवाद राजनीतिक प्रश्न उठा पाने में अक्षमता की प्रवृत्ति का नाम होता है।’ आज देश में क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट आन्दोलन यदि मध्यवर्ग व निम्न मध्यवर्ग के विभिन्न स्तरों तक कोई पहुँच रखता है तो वह मुख्य रूप से कुछ विश्वविद्यालय परिसरों और विशेष तौर पर कुछ कुलीन विश्वविद्यालय परिसरों तक सीमित है। एक व्यापक निम्न मध्यवर्गीय और अर्द्धमज़दूर बनने की सीमा पर खड़ी आम ग़रीब आबादी है जिसमें क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट आन्दोलन की कोई विशेष पकड़ नहीं है। इस आबादी के बीच या तो संघ परिवार के विभिन्न फासीवादी संगठन काम कर रहे हैं और उन्हें ‘हिन्दू राष्ट्र’ के मिथ्या समाधान के लिए सहमत करने का प्रयास कर रहे हैं या फिर इन वर्गों में साम्राज्यवादियों के टुकड़ों पर पलने वाले तमाम एन.जी.ओ. संगठन काम कर रहे हैं और इन वर्गों में सुधारवाद के ज़रिये भिक्षावृत्ति पैदाकर उनकी क्रान्तिकारी सम्भावनाओं पर चोट पहुँचा रहे हैं। साम्राज्यवाद-पोषित एन.जी.ओ. राजनीति और पतित समाजवादी राजनीति के अवैध सम्बन्धों से पैदा होने वाली ‘आम आदमी पार्टी’ की राजनीति भी इन्हीं वर्गों को निशाना बना रही है।
मगर क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट आन्दोलन इन वर्गों में अपने क्रान्तिकारी संगठनों को खड़ा करने के काम में अभी काफ़ी पीछे है और इसे कदम-कदम पर इसकी कीमत भी चुकानी पड़ती है। मुम्बई के मज़दूर आन्दोलन के ध्वंस में शिवसेना एक अहम भूमिका निभाने में कामयाब रही तो इसके दो प्रमुख कारण थेः पहला, शिवसेना ने तमाम आम मेहनतकश आबादी के रिहायशी इलाकों में ‘लॉयल्टी नेटवर्क’, मित्र मण्डल, युवा मण्डल, जिम आदि बनाने के ज़रिये अपना सामाजिक आधार तैयार किया जबकि मज़दूर वर्ग का आन्दोलन ट्रेडयूनियनवादी फ्रेमवर्क से बाहर नहीं निकल सका और वहाँ तक अपनी पहुँच नहीं बना सका; दूसरा, शिवसेना ने निम्न मध्य वर्ग के एक अच्छे-ख़ासे हिस्से की मराठी कट्टरवाद के जुमले के ज़रिये फासीवादी प्रतिक्रियावादी गोलबन्दी करने में सफलता पायी क्योंकि कम्युनिस्ट आन्दोलन ने इन वर्गों में क्रान्तिकारी प्रचार और उद्वेलन को पर्याप्त महत्व नहीं दिया। इसलिए क्रान्तिकारी मज़दूर आन्दोलन के लिए एक अहम सबक यह है कि उसे टटपुँजिया वर्गों के विशेष तौर पर निम्नतर संस्तरों के बीच सतत् राजनीतिक प्रचार करना होगा और संस्थाबद्ध हस्तक्षेप करते हुए उन्हें संगठित करना होगा; उनके सामने यह स्पष्ट करना होगा कि उनके जीवन की अनिश्चितता और असुरक्षा के लिए वास्तव में पूँजीवादी व्यवस्था ज़िम्मेदार है; उनके बीच सुधार कार्यों व सांस्कृतिक कार्यों की निरन्तरता बनानी होगी। यह समझना बेहद अहम है कि उनके बीच इस प्रकार के कार्यों को संस्थाबद्ध रूप (institutional form) देना होगा। मिसाल के तौर पर, नौजवानों व बच्चों के पुस्तकालय, जिम, खेल क्लब आदि बनाने होंगे, मेडिकल कैम्प, सफाई अभियान जैसे कार्यक्रम आयोजित करने होंगे, अपनी जनता डिस्पेंसरी व जनता क्लिनिक खोलने होंगे, मृतक वाहन सेवा आदि शुरू करनी होगी और इसी प्रकार के अगणित कार्य करने होंगे। और सबसे अहम बात यह कि इन वर्गों के विभिन्न हिस्सों, जैसे कि युवाओं, स्त्रियों, छात्रों व नागरिकों के जनसंगठन बनाने होंगे और उन्हें उनकी आर्थिक व सामाजिक माँगों के लिए संघर्ष करने के लिए शिक्षित-प्रशिक्षित करना होगा। लेकिन केवल आर्थिक मुद्दों तक हमें अपने प्रचार को सीमित नहीं रखना होगा, बल्कि जनसमुदायों के भीतर मौजूद उन प्रवृत्तियों और मूल्यों-मान्यताओं के विरुद्ध मित्रतापूर्ण संघर्ष चलाना होगा, जोकि उन्हें फासीवादी राजनीति के समक्ष अरक्षित बनाती हैं, विशेष तौर पर पितृसत्ता-विरोधी व स्त्री मुक्ति का संघर्ष और जाति उन्मूलन के लिए सर्वहारा वर्गीय कार्यदिशा के साथ जुझारू संघर्ष। केवल इसी रास्ते से हम फासीवादियों के विरुद्ध समाज में अपनी अवस्थितियाँ बाँध सकते हैं और उनसे लड़ सकते हैं।
लेकिन इतना ही समझना काफ़ी नहीं है। टटपुँजिया वर्गों के हरेक हिस्से को इन सारे प्रयासों के ज़रिये भी मज़दूर वर्ग के पक्ष में नहीं जीता जा सकता है। और इसमें चिन्तित होने वाली भी कोई बात नहीं है! टटपुँजिया वर्ग कोई एकाश्मी निकाय नहीं है और इसके तमाम संस्तर होते हैं। मज़दूर वर्ग और पूँजीपति वर्ग से सापेक्षिक दूरी के अनुसार इनके राजनीतिक वर्ग चरित्र में परिवर्तन होता है। पूँजीवादी लूट से इसके कुछ संस्तर उजड़ते हैं तो एक छोटा-सा हिस्सा सामाजिक पदानुक्रम में सीढ़ियाँ चढ़ता भी जाता है। फासीवाद जिस हद तक उजड़ते हुए टटपुँजिया वर्ग का मिथकीय या रूमानी उभार है वह उसी हद तक सामाजिक रूप से ऊपर की ओर गतिमान टटपुँजिया वर्ग का आन्दोलन भी है। और उजड़ता हुआ टटपुँजिया वर्ग अगर फासीवादी उभार का आधार बनता है तो इसका एक अहम कारण तो क्रान्तिकारी कम्युनिस्टों और मज़दूर आन्दोलन की विफलता भी है, जैसा कि हमने ऊपर प्रदर्शित किया। मगर सामाजिक पदानुक्रम में ऊपर की ओर चढ़ते टटपुँजिया वर्ग का फासीवाद का सामाजिक अवलम्ब बनना ज़्यादा स्वाभाविक है और क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट प्रचार को चाहे जितनी भी सटीकता और कुशलता के साथ अंजाम दिया जाय, इस वर्ग के एक हिस्से को ही जीता जा सकता है और उस हिस्से के छोटा होने की सम्भावना ही ज़्यादा होगी। हमने अपनी पुस्तिका में इस पहलू को सन्तोषजनक रूप से स्पष्ट नहीं किया था, क्योंकि यह यथार्थ का प्रमुख पहलू नहीं है। लेकिन आज के परिदृश्य में फासीवादी उभार के तमाम पहलुओं को समझने के लिए हमें इस नुक्ते को स्पष्ट करने की आवश्यकता महसूस हो रही है। प्रमुख पहलू यही है कि उजड़ते हुए टटपुँजिया वर्ग फासीवादी प्रतिक्रिया का सामाजिक आधार बनते हैं क्योंकि समूचे टटपुँजिया वर्गों में ये उजड़ते हुए वर्ग बहुसंख्या होते हैं। लेकिन फिर भी इस प्रमुख पहलू पर सारी सच्चाई को अपचयित करने देने के अपने नुकसान भी हैं। अगर दूसरे गौण पहलू को नहीं समझा जाता है तो टटपुँजिया वर्गों में क्रान्तिकारी प्रचार और उद्वेलन की उपयुक्त रणनीति नहीं तैयार की जा सकती है।
यह सच है कि टटपुँजिया वर्गों का एक अच्छा-ख़ासा हिस्सा पूँजीवादी संचय की प्रक्रिया में अनिश्चितता और सामाजिक-आर्थिक असुरक्षा के गड्ढे में धकेल दिया जाता है। यदि उनके बीच व्यापक और सघन पूँजीवाद-विरोधी क्रान्तिकारी प्रचार न हो तो उसका एक बड़ा हिस्सा इस फासीवादी प्रचार को मानने को तैयार होता है कि उसके जीवन की अनिश्चितता के लिए मज़दूर वर्ग को मिले हुए “विशेषाधिकार” (सुरक्षात्मक श्रम कानून, न्यूनतम मज़दूरी, अन्य कल्याणकारी नीतियाँ आदि) ज़िम्मेदार हैं क्योंकि इनके कारण “राष्ट्र” का विकास नहीं हो पा रहा है, देश पूरी दुनिया में प्रतिस्पर्द्धात्मक नहीं हो पाता है, आर्थिक वृद्धि की दर कम हो जाती है, वगैरह। मोदी सरकार आजकल इस प्रकार का प्रचार ज़ोर-शोर से कर रही है। यह बात टटपुँजिया वर्ग के विशेष तौर पर ऊपरी हिस्सों और उद्यमी तबके पर लागू होती हैं। हालाँकि यह टटपुँजिया वर्ग किसी भी रूप में तकनोलॉजी, आधुनिकीकरण और उद्योगों का विरोधी नहीं होता है, मगर फिर भी यह संघ परिवार के काल्पनिक आधुनिकता-विरोध की ओर काफ़ी आकर्षित होता है। चूँकि इस वर्ग के पास देखने के लिए कोई भविष्य नहीं होता है या चूँकि इसे भविष्य का सपना दिखाने वाली ताक़तें मौजूद नहीं होतीं इसलिए इसे किसी कल्पित मिथकीय अतीत के चित्र बहुत रमणीय लगते हैं, जैसे कि किसी “रामराज्य” या किसी भी किस्म के प्राचीन हिन्दू राज्य की तस्वीर। इन वर्गों में पूँजीवादी प्रचार के प्रभाविता का एक और कारण भी होता है। इनमें से कई पूँजीपति या उद्यमी बनने के सपने भी पालते रहते हैं। निम्न मध्यवर्ग का वह हिस्सा विशेष तौर पर उद्यमी बन जाने के इस सपने या कहें भ्रम का शिकार होता है जो कि पेशेवर के तौर पर काम नहीं करता, यानी कि जो किसी और नियोक्ता के पास नौकरी नहीं करता और अपना छोटा-मोटा कोई काम करता है, जैसे कि कोई वर्कशॉप या दुकान आदि चलाना। इस हिस्से को हमेशा यह लगता है कि वह भी एक दिन समृद्ध पूँजीपति बन जायेगा! इन लोगों को धीरूभाई अम्बानी जैसों के ‘नीचे से ऊपर उठने’ की कहानी बहुत अपील करती है! यह बात दीगर है कि इस वर्ग का बिरला ही कोई ऊपर चढ़कर पूँजीपति बन पाता है! इनमें से अधिकांश कभी इस स्थिति में ही नहीं आ पाते हैं। मगर फिर भी अपने छोटे-मोटे धंधे का मालिक होने के कारण इनके भीतर मालिक बनने का भ्रम, सपना और मानसिकता मौजूद होती है। इस सपने के सच न हो पाने के कारण के तौर पर वे हमेशा मज़दूरों को देखते हैं, जो कि “आलसी और कामचोर” होते हैं; ऐसा सोचने का कारण यह होता है कि ऐसे बेहद छोटे उद्यमी भी कई बार एक-दो मज़दूर काम पर रखते हैं। इस वर्ग को उदार पूँजीवादी संसदीय जनवाद के विरुद्ध भड़का कर “राष्ट्र-विकास” हेतु, “रामराज्य-पुनर्स्थापना” हेतु फासीवादी तानाशाही और एक “मज़बूत नेता”, “छप्पन इंच छाती वाले प्रधानमन्त्री” के लिए तैयार करना अपेक्षाकृत आसान होता है! अपनी सामाजिक अवस्थिति से ही यह किसी भी प्रकार के प्रतिक्रियावादी प्रचार के सामने कहीं ज़्यादा निहत्था होता है। भारत में ऐसा टटपुँजिया उद्यमी वर्ग कोई छोटा नहीं है और इसको क्रान्तिकारी अवस्थिति पर जीतना सबसे मुश्किल होता है और इसका एक अच्छा-ख़ासा हिस्सा अक्सर फासीवादी उभार का एक सामाजिक आधार बनता है। इस ‘पूँजीपति बनने के आकांक्षी उद्यमी टटपुँजिया वर्ग’ के मुकाबले किसी अन्य मालिक को अपना श्रम बेचने वाले टटपुँजिया वर्ग के क्रान्तिकारी अवस्थिति पर आने की सम्भावनासम्पन्नता कहीं ज़्यादा होती है और क्रान्तिकारी शक्तियों को उन्हीं पर अपने प्रयासों को केन्द्रित करना चाहिए।
टटपुँजिया वर्ग का एक दूसरा छोटा-सा हिस्सा ऐसा भी होता है जो कि सामाजिक पदानुक्रम में ऊपर की सीढ़ियाँ चढ़ रहा होता है, जो कि पूँजीवादी लूट का एक छोटा लाभ प्राप्तकर्ता होता है। छोटे ठेकेदारों, जॉबरों, दलालों, मोटी तनख़्वाहें पाने वाले पढ़े-लिखे शिक्षित मध्यवर्गीय युवाओं (जैसे कि आई.टी., बी.पी.ओ. सेक्टर आदि में काम करने वाली आबादी), अच्छी तनख़्वाहों वाली सरकारी नौकरी करने वाले मध्यवर्ग को पूँजीवादी संचय और विकास का लाभ भी प्राप्त होता है। उसे आधुनिकीकरण व उद्योगीकरण से भी फायदा मिलता है। इन वर्गों की राजनीतिक चेतना, या कहें भावनाएँ, पूँजीवादी व्यवस्था की अस्थिरता से काफ़ी डावाँडोल होती है। उसे हर ऐसी चीज़ से नफ़रत होती है जो कि उसके जीवन की प्रीतिकर स्थिरता या कहें ठहराव को अस्थिर करती हुई नज़र आती है। मिसाल के तौर पर, अगर वह अपनी बालकनी से मज़दूरों के किसी जुलूस को भी देखता है तो घबरा जाता है; उसे एकदम असम्बद्ध तरीके से तत्काल अपनी समृद्धि और सम्पत्ति पर ख़तरा महसूस होता है और साथ ही उसे अपने परिवार और “उसकी स्त्रियों” पर भी ख़तरा महसूस होता है। । यहीं से उसकी प्रतिक्रिया पैदा होती है। उसे लगता है कि मज़दूरों पर मज़बूती से लगाम कसने के लिए उदार पूँजीवादी जनवाद नाक़ाफ़ी है और एक तानाशाह होना चाहिए जो इन सबके पेंच टाइट करके रखे! विशेष तौर पर आर्थिक संकट के दौर में इस खाती-पीती टटपुँजिया आबादी के बीच इस प्रकार के विचारों की ज़बर्दस्त अपील होती है। अगर आप तमाम सामाजिक मीडिया की वेबसाइटों पर मोदी-समर्थकों की एक पूरी प्रोफाइल तैयार करें, तो आप पायेंगे कि उनमें से करीब 90 प्रतिशत लोग इसी वर्ग और इन्हीं पेशों से आते हैं। अपनी प्रतिक्रिया में यह वर्ग जल्द ही सामान्यीकरण कर लेता है और इसकी प्रतिक्रिया जल्द ही पूरी तरह से अन्धी और निरंकुश हो जाती है। मिसाल के तौर पर, यह वर्ग जल्द ही मुखर तौर पर स्त्री-विरोधी, दलित-विरोधी, दमित राष्ट्रीयता-विरोधी, आदि भी हो जाता है, हालाँकि ऐसा बन जाने की सुषुप्त सम्भावना उसमें हमेशा से ही मौजूद रहती है। ये ही लोग हैं जो कविता कृष्णन, अभिनेत्री खुशबू और श्रुति सेठ के विरुद्ध ट्विटर व फेसबुक जैसी वेबसाइटों पर भयंकर अश्लील और गन्दी टिप्पणियाँ करते हुए नरेन्द्र मोदी का गुणगान करते हैं। इस वर्ग का कोई व्यक्ति पूँजीवाद-विरोधी क्रान्तिकारी पक्ष के साथ आ सकता है मगर एक वर्ग के तौर पर यह किसी सूरत में क्रान्तिकारी पक्ष के साथ नहीं आ सकता है।
टटपुँजिया वर्ग के ये दो हिस्से ऐसे हैं जो कि क्रान्तिकारी मज़दूर आन्दोलन के मित्र बनने की क्षमता नहीं रखते हैं और नैसर्गिक तौर पर इनमें प्रतिक्रिया का आधार बनने की सम्भावना ज़्यादा होती है, यानी कि टटपुँजिया वर्ग का ऊपरी हिस्सा और निम्न पूँजीवादी उद्यमी आबादी, यानी ‘पूँजीपति बनने की आकांक्षी’ टटपुँजिया आबादी। इसलिए यह भी समझने की आवश्यकता है कि केवल एक मिथ्या चेतना का शिकार उजड़ता हुआ टटपुँजिया वर्ग ही फासीवादी उभार का सामाजिक आधार नहीं बनता, बल्कि सामाजिक रूप से ऊपर की ओर गतिमान और पूँजीवादी लूट का लाभ प्राप्तकर्ता बनने वाला टटपुँजिया वर्ग भी फासीवादी उभार का ज़बर्दस्त सामाजिक आधार बनता है। फासीवाद केवल उजड़ते टटपुँजिया वर्ग का प्रतिक्रियावादी सामाजिक आन्दोलन नहीं है, बल्कि इस आर्थिक तौर पर उभरते टटपुँजिया वर्ग का भी प्रतिक्रियावादी सामाजिक आन्दोलन है। सच कहें तो यह उभरता हुआ टटपुँजिया वर्ग सचेतन तौर पर इस फासीवादी प्रतिक्रिया का सामाजिक आधार बनता है और टटपुँजिया वर्गों के रूमानी उभार का नेतृत्व भी इसी के पास होता है। यह खाता-पीता टटपुँजिया वर्ग मिथ्या वर्ग भावना से कम अपने नैसर्गिक वर्ग हितों से ज़्यादा प्रेरित होता है, जबकि उजड़ता हुआ टटपुँजिया वर्ग वास्तव में अपने असली वर्ग हितों के प्रति अनभिज्ञ होता है और इस अज्ञान के कारण ही वह फासीवादी उभार के साथ खड़ा होता है। इसीलिए उजड़ता हुआ टटपुँजिया वर्ग या दूसरे शब्दों में कहें तो निम्न मध्यवर्गीय आबादी और विशेषकर आम मेहनतकश निम्न मध्यवर्गीय आबादी के भीतर क्रान्तिकारी पक्ष के साथ आने की सम्भावना ज़्यादा होती है बशर्ते कि क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट आन्दोलन अपने सतत् प्रचार और उद्वेलन के ज़रिये इस वर्ग को अपने पक्ष में लेने के लिए रचनात्मक, नये और व्यावहारिक तरीकों और रूपों का इस्तेमाल करे और अर्थवादी रवैये को छोड़ कर एक क्रान्तिकारी राजनीतिक रवैया अख्तियार करे।
मज़दूर वर्ग के कौन-से हिस्से फासीवाद का आधार बन सकते हैं
कई मार्क्सवादी विश्लेषणों में यह प्रवृत्ति पायी गयी है कि वे फासीवादी आन्दोलनों की मज़दूर वर्ग के भीतर पकड़ को कम करके दिखलाते हैं। हमने मौजूदा पुस्तिका में संक्षेप में इस बात पर चर्चा की थी कि मज़दूर वर्ग के भी कुछ हिस्सों में फासीवादी राजनीति का असर होता है और वे किस प्रकार फासीवादी उभार का एक उपकरण बन बैठते हैं। फिर भी हमें लगता है कि इस पर थोड़ा और विस्तार में जाने की आवश्यकता है क्योंकि यह मज़दूर वर्ग के क्रान्तिकारी आन्दोलन के लिए एक तात्कालिक महत्व रखता है और चुनौती पेश करता है। इसे न समझने के कारण पहले ही काफ़ी नुकसान हो चुका है और आगे चलकर और भी ज़्यादा नुकसान होगा।
हमने पुस्तिका में दिखलाया था कि किस प्रकार संघ परिवार से जुड़े हुए ‘भारतीय मज़दूर संघ’ द्वारा मज़दूरों के बीच पूँजीवादी राष्ट्रवाद का प्रचार किया जाता है और किस तरह से विशेष तौर पर सफेद कॉलर वाले मज़दूरों (जो कि अपने आपको ‘कर्मचारी’ कहलवाना पसन्द करते हैं!) के बीच फासीवादी का आधार तैयार होता है। कुछ वर्षों पहले भारतीय मज़दूर संघ का माकपा से सम्बद्ध ट्रेड यूनियन संघ ‘सीटू’ को पीछे छोड़ते हुए सबसे बड़ी यूनियन बन जाना सफेद कॉलर के मज़दूरों के बीच फासीवादी राजनीति की बढ़ती दख़ल को ही प्रदर्शित करता है। और यह कोई चौंकाने वाली बात भी नहीं है। अतीत में भी मज़दूर वर्ग के इस हिस्से का एक अंग फासीवादी उभार का आधार बन चुका है। आइये कुछ ठोस आँकड़ों पर निगाह डालें और फिर फासीवाद का आधार बनने वाले मज़दूर तबके का करीबी से विश्लेषण करें।
1930 में नात्सी पार्टी की सदस्यों में से 26.3 प्रतिशत मज़दूर थे। यह आँकड़ा 1932 में बढ़कर 32.5 प्रतिशत हो गया। इटली में तो फासीवादी आन्दोलन ने मज़दूर आन्दोलन के भीतर जड़ जमाने से ही शुरुआत की थी। हंगरी के ‘एरो क्रॉस’ नामक फासीवादी संगठन की भी मज़दूर आबादी के एक हिस्से में अच्छी पकड़ थी। बताने की ज़रूरत नहीं है कि इसके लिए फासीवादी राजनीति ने इटली और जर्मनी दोनों ही देशों में मज़दूरों के इलाकों में कुछ कारपोरेटवादी उपक्रम भी चलाये थे, जैसे कि मज़दूरों के लिए सुरक्षा फण्ड पूल का निर्माण करना; ज़रूरत पड़ने पर कुछेक मज़दूरों को ऋण देना, फासीवादी संगठन के चहेते मज़दूरों के समुदाय (जाति, क्षेत्र, भाषा, आदि) के कुछेक लोगों को नौकरियाँ दिलवा देना आदि। शिवसेना ने भी महाराष्ट्र में कुछ इलाकों में पकड़ बनाने के लिए उन इलाके के कुछ विशिष्ट समुदायों के कुछेक लोगों को किन्हीं कम्पनियों या उपक्रमों में बन्दूक की नोक पर नौकरी दिलवाने का काम किया था, जिससे कि उस पूरे समुदाय में ही उसका आधार तैयार होता था। ज़ाहिर है, ऐसे तरीकों से मज़दूर आबादी को बेरोज़गारी या ग़रीबी से निजात नहीं मिल जाती है। बस एक भ्रम तैयार होता है और समुदायगत चेतना में बँधे मज़दूर, दूसरे शब्दों में कहें तो राजनीतिक चेतना की कमी के शिकार मज़दूर ऐसे फासीवादी संगठनों का समर्थन करते हैं और उनमें से कुछ उनके पैदल सैनिक बनने को भी तैयार हो जाते हैं। भारत में भी भाजपा और संघ परिवार के अन्य अनुषंगी संगठन इन कारपोरेटवादी तरीकों को अपनाते हैं। कारपोरेटवाद की सोच मुसोलिनी ने इटली में लागू की थी जिसका मकसद था मज़दूर वर्ग और पूँजीपति वर्ग के बीच सहकार की बात करना और उनके अन्तरविरोधों को विभिन्न तरीकों से कुन्द करना। इसके लिए मज़दूरों के प्रतिनिधियों और पूँजीपतियों के प्रतिनिधियों को फासीवादी पार्टी की मध्यस्थता में साथ बिठाया जाता था। हालाँकि इस प्रकार के सहकार का अन्त हमेशा ऐसे समझौतों या सौदों में होता था जिसमें मज़दूर वर्ग को पूँजीपति वर्ग की शर्तों को स्वीकार करना पड़ता था। कहने की आवश्यकता नहीं है कि फासीवादी ताक़तें मज़दूरों के बीच अपने आधार को तैयार करने के लिए मज़दूरों के बीच मौजूद कूपमण्डूकतापूर्ण विचारों, धार्मिक ढोंग, ढकोसले और पाखण्ड और हर प्रकार की पिछड़ी हुई धार्मिक व जातिगत चेतना का भी इस्तेमाल करती हैं। इसलिए विशेष तौर पर सफेद कॉलर वाले मज़दूरों का एक हिस्सा फासीवादी उभार का सामाजिक आधार बनता है। लेकिन साथ ही मज़दूर आबादी के कुछ अन्य हिस्से भी होते हैं जिनमें फासीवादी उभार का आधार बन बैठने की सम्भावना होती है।
टिम मेसन नामक एक मार्क्सवादी अध्येता ने नात्सी जर्मनी का अध्ययन करते हुए दिखलाया था कि मज़दूर वर्ग के कौन-से हिस्सों में फासीवादी प्रचार के समक्ष कमज़ोर पड़ने की प्रवृत्ति और फासीवाद का आधार बनने की सम्भावना सबसे ज़्यादा होती है। मेसन ने दिखलाया है कि ठेका, दिहाड़ी या अस्थायी प्रकृति के रोज़गार में काम करने वाले नये युवा और सतत् गतिमान या अस्थिर मज़दूर आबादी में, जिन्हें किसी भी किस्म के मज़दूर संगठन या ट्रेड यूनियन संघर्ष का कोई अनुभव नहीं होता, फासीवादी राजनीति के पकड़ बनाने की पर्याप्त सम्भावना होती है। मेसन के अनुसार इसका कारण यह है कि यह आबादी राजनीतिक चेतना से सबसे ज़्यादा वंचित होती है। लेकिन आज के दौर में इसमें थोड़ा बदलाव आया है। हमारा मानना है कि आज के दौर में इस वर्ग में राजनीतिक बनने और ज़्यादा तेज़ी से व्यवस्था-विरोधी राजनीतिक वर्ग चेतना हासिल करने की क्षमता (सम्भावना-सम्पन्नता) सबसे ज़्यादा होती है। वास्तव में, विशेष तौर पर 1970 के दशक के बाद के दौर में समूचे अनौपचारिक/असंगठित मज़दूर वर्ग के राजनीतिक चरित्र में कुछ अहम बदलाव आये हैं और इसे पहले की तरह वर्ग चेतना के अभाव, राजनीतिक चेतना की कमी, आदिम चेतना या पिछड़ेपन से नहीं पहचाना जा सकता है। लेकिन यह बात आज भी सच है कि उनमें किसी भी किस्म के क्रान्तिकारी प्रचार व संगठन के अभाव में उनमें आज भी यह सम्भावना-सम्पन्नता मौजूद है कि वे समुदाय, जाति, धर्म आदि के आधार पर किसी फासीवादी गोलबन्दी का हिस्सा बन जायें। मगर निश्चित तौर पर पहले के दौर के मुकाबले इस सम्भावना में कमी आयी है।
टिम मेसन के अनुसार मज़दूर वर्ग का वह दूसरा हिस्सा जिसमें फासीवादी राजनीति का आधार बनने की सम्भावना होती है, वह है ‘वर्दी वाले मज़दूर’ जो कि रेलवे, पोस्ट व टेलीग्राफ़, आदि में काम करते हैं। इनमें बैंक व बीमा सेक्टर में काम करने वाली, बड़े सरकारी दफ्तरों में अच्छे वेतन के साथ काम करने वाली एक मज़दूर आबादी भी शामिल है। तीसरा हिस्सा उन मज़दूरों का है जो कि छोटे व्यावसायिक सेक्टर में काम करते हैं। ऐसे मज़दूर अक्सर अकेले काम करते हैं या बेहद छोटे समूहों में काम करते हैं और इस वजह से इनमें वर्ग चेतना के विकसित होने की गति बेहद धीमी होती है और अवरुद्ध होती रहती है। टिम मेसन के अनुसार चौथा और आखि़री हिस्सा है लम्पट सर्वहारा का जिसमें वर्ग चेतना की नितान्त अभाव होता है, कई बार ग़रीबी और अमानवीकरण के कारण आपराधिक और बर्बरता की प्रवृत्तियाँ होती हैं। इन्हीं गुणों के कारण फासीवादी ताक़तें मज़दूर आबादी के इस हिस्से का इस्तेमाल का विनियोजन कर पाती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस आबादी को संगठित करने के प्रयास नहीं किये जा सकते हैं। वास्तव में, मज़दूर वर्ग के एक अच्छे-ख़ासे हिस्से में फासीवादी राजनीति कम्युनिस्टों की असफलता और ग़लत कार्यपद्धति के कारण ही जगह बना पाती है। जैसा कि टिम मेसन ने दिखलाया है कि अनौपचारिक/असंगठित मज़दूर वर्ग के एक हिस्से में नात्सी पार्टी ने जर्मनी में अपना आधार बनाया था और इसका बहुत बड़ा कारण था जर्मन सामाजिक जनवादी आन्दोलन और ट्रेड यूनियन आन्दोलन का संगठित/औपचारिक मज़दूर वर्ग तक सीमित रह जाना।
आज यह अनौपचारिक/असंगठित मज़दूर वर्ग कुल मज़दूर वर्ग का 93 प्रतिशत है और यह मज़दूर वर्ग 1930 के दशक के असंगठित मज़दूर वर्ग के समान पिछड़ा नहीं है। इस पूरे वर्ग में आज भारत के फासीवादियों ने आधार बनाने के नये तरीके निकाले हैं। जागरण, चौकी आदि जैसे धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन कराकर धर्म और पुरानी धार्मिक परम्पराओं के आधार पर एक समुदाय की रचना करना; इसके अलावा, दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा आदि के आयोजन के लिए मित्र मण्डलों का निर्माण करना, आदि। इसके साथ ही संघ परिवार पुराने कारपोरेटवादी तरीकों का इस्तेमाल भी कर रहा है और उन्हें उन्नत भी कर रहा है। मिसाल के तौर पर, तमाम मज़दूर इलाकों में ‘सेवा भारती’ के नाम से तमाम सुधारवादी और एन.जी.ओ.-मार्का उपक्रम चलाये जा रहे हैं। इनमें महिलाओं को सिलाई-कढ़ाई सिखाने आदि से लेकर बच्चों को पढ़ाने तक के कार्य किये जा रहे हैं। इसके अलावा एक अन्य उदाहरण है जिसे मज़दूर इलाकों में कई ‘कमेटी डालने’ के नाम से जाना जाता है। ये वास्तव में एक ‘फण्ड पूल’ होता है जिसका प्रयोग मज़दूर आबादी के जीवन की आर्थिक अनिश्चितता में कुछ कमी लाने के लिए किया जाता है, हालाँकि इससे भ्रम ज़्यादा पैदा होता है और वास्तव में मज़दूरों के जीवन में कोई विशेष फर्क नहीं आता। ज़ाहिर है, इन कार्रवाइयों के साथ-साथ लोगों की चेतना का फासीवादीकरण करने का कार्य भी किया जाता है।
लेकिन यहाँ सबसे अहम बात यह है कि मज़दूर वर्ग के इन संस्तरों में फासीवादी ताक़तें आम तौर पर इसी लिए सामाजिक आधार बनाने में सफल होती हैं क्योंकि वहाँ क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट ताक़तें या तो पहुँच ही नहीं पातीं या फिर उनकी उपस्थिति जिस रूप में होनी चाहिए उस रूप में नहीं होती। जर्मनी में सामाजिक जनवादी शक्तियों के साथ-साथ कम्युनिस्टों की भी एक भारी ग़लती यह थी कि संगठित मज़दूर आबादी के बाहर मज़दूर वर्ग को संगठित करने के उनके प्रयास नगण्य थे। अफसोस की बात यह है कि अधिकांश देशों में इतिहास से कम्युनिस्ट ताक़तों ने कोई सबक नहीं लिया है। अभी भी उनकी ताक़तों का बड़ा हिस्सा संगठित मज़दूर आबादी के बीच ही लगा हुआ है, जो कि पूरे मज़दूर वर्ग का अब छोटा सा हिस्सा रह गया है। भारत के भीतर भी क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट संगठनों की बड़ी ताक़त या तो मज़दूर आबादी से ही दूर हैं क्योंकि वे भारत को एक अर्द्धसामन्ती अर्द्धऔपनिवेशिक देश मानते हैं और अपने इस पुराने पड़ चुके कार्यक्रम में बदलाव करने को ही मार्क्सवाद-लेनिनवाद से ग़द्दारी मानते हैं! ऊपर से वे यह भी नहीं समझते कि नवजनवादी क्रान्ति की मंज़िल में भी मज़दूर वर्ग ही नेतृत्वकारी ताक़त होता है; किसान वर्ग केवल मुख्य ताक़त होता है। इसके अलावा, मोदी सरकार द्वारा हाल ही में किये गये जाति सर्वेक्षण के दौरान पता चला है कि गाँव की आबादी का भी आधे से ज़्यादा गैर-कृषि रोज़गार में लगा हुआ है और आबादी का जो हिस्सा कृषि में लगा भी है उसमें से अधिकांश ज़मीन के मालिक नहीं हैं और खेतिहर मज़दूर हैं! ऐसे में, नवजनवादी क्रान्ति का कार्यक्रम किस रूप में प्रासंगिक है? ‘जो ज़मीन को जोते-बोए वह ज़मीन का मालिक होए’ नारा किस रूप में प्रासंगिक है? और तो और ताज्जुब की बात यह है कि नवजनवादी क्रान्ति को मानने वाले तमाम “वामपंथी” दुस्साहसवाद और क्रान्तिकारी आतंकवाद की लाइन के शिकार ये संगठन गाँवों में खेतिहर आबादी में भी अपनी पकड़ अधिकांश प्रदेशों में खो चुके हैं। अब कुल मिलाकर उनका आधार मध्य भारत के कुछ जनजातीय क्षेत्रों में रह गया है, जहाँ ‘आदिम संचय’ की प्रक्रिया के ज़रिये कारपोरेट पूँजीवाद जनजातीय आबादी को उजाड़ रहा है। इनका मानना है कि भारत का पूँजीपति वर्ग एक दलाल पूँजीपति वर्ग है। ऐसे में उन्हें यह नहीं मानना चाहिए कि भारत में फासीवाद का उभार हो रहा है। दलाल पूँजीपति वर्ग प्रतिक्रियावादी होता है और उसका प्रतिक्रियावाद कई रूप ले सकता है। लेकिन दलाल पूँजीपति वर्ग प्रकृति से ही इस बात में अक्षम होता है कि उसका प्रतिक्रियावाद एक फासीवादी सामाजिक आन्दोलन का रूप ले सके। फासीवाद औद्योगिक और वित्तीय बड़े पूँजीपति वर्ग की सेवा करने वाला टटपुँजिया वर्ग का प्रतिक्रियावादी रूमानी उभार होता है। ऐसा प्रतिक्रियावादी रूमानी उभार किसी दलाल या कठपुतली पूँजीपति वर्ग के नेतृत्व में नहीं हो सकता है। नवजनवादी क्रान्ति की लाइन पर अटके हुए इन कम्युनिस्ट क्रान्तिकारियों के लिए फासीवादी उभार की विवेचना करने का अर्थ है असमाधेय और मज़ाकिया अन्तरविरोधों के गड्ढे में जा गिरना। ख़ैर, इन तमाम नवजनवादी क्रान्ति मानने वालों और ‘टाइम कैप्स्यूल’ में कैद रह गये कम्युनिस्ट क्रान्तिकारियों के बारे में जितना कम कहा जाय उतना अच्छा है।
लेकिन इससे भी ज़्यादा आश्चर्य की बात तो यह है कि समाजवादी क्रान्ति मानने वाले तमाम क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट संगठन भी ऐसे हैं जिनका मानना है कि कम्युनिस्टों को उन्नत और बड़े उद्योगों में लगे संगठित मज़दूरों पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए क्योंकि वही मज़दूर आबादी का उन्नत हिस्सा है! यानी कि उनके अनुसार 93 प्रतिशत असंगठित/अनौपचारिक मज़दूर आबादी उन्नत नहीं है, पिछड़ी हुई है, वर्ग चेतना से लैस नहीं है, वगैरह! यह वास्तव में कम्युनिस्ट आन्दोलन का एक पूर्वाग्रह है जो अतीत के एक ख़ास दौर में पैदा हुआ था। वैसे तो यह पूर्वाग्रह उस दौर में भी निहायत ग़लत था मगर आज तो यह भयंकर रूप से नुकसानदेह है। आज की असंगठित/अनौपचारिक मज़दूर आबादी पहले के समान नहीं है। यह वर्ग चेतना से लैस है या उसमें वर्ग चेतना से लैस होने की सम्भावनासम्पन्नता मौजूद है; यह आबादी क्रान्तिकारी राजनीतिक वर्ग चेतना की दिशा में अपेक्षाकृत ज़्यादा सहजता से विकसित हो सकती है क्योंकि यह एक वर्ष में ही कई बार कई मालिकों के मातहत काम करती है और इसलिए किसी एक मालिक को अपने शत्रु के तौर पर नहीं देखती, बल्कि मालिकों के पूरे वर्ग को अपने शत्रु के तौर पर देखती है। यह आबादी रोज़मर्रा की ज़िन्दगी में राज्यसत्ता के दमनकारी निकायों का भी सामना करती है और इसके अन्दर नैसर्गिक तौर पर एक व्यवस्था-विरोधी भावना होती है। यह आबादी उन्नत मशीनों व तकनोलॉजी पर कार्य करने अनुभव रखती है और साथ ही बहुकुशल होती है। इस करोड़ों-करोड़ की और ज़बर्दस्त क्रान्तिकारी सम्भावनाओं से लैस अनौपचारिक/असंगठित मज़दूर आबादी को “पिछड़ा”, “आदिम“ आदि मानना भयंकर भूल है। इसलिए भी यह भयंकर भूल है कि अगर क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट आन्दोलन इस व्यापक मज़दूर आबादी को संगठित नहीं करता तो निश्चित तौर पर इसका एक हिस्सा फासीवाद के पाले में जायेगा और फासीवादी ताक़तों के उपकरण में तब्दील होगा। इसलिए इस मज़दूर आबादी के बीच ट्रेड यूनियन आन्दोलन खड़ा करने के साथ-साथ क्रान्तिकारी सुधार कार्य और क्रान्तिकारी सांस्कृतिक कार्य को संस्थाबद्ध रूप से करना आज क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट आन्दोलन के सामने एक अस्तित्व का प्रश्न बन गया है।
इस अस्तित्व के प्रश्न के समाधान में क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट संगठनों में व्याप्त एक और प्रवृत्ति भी भारी बाधा बनती है। यह प्रवृत्ति है स्वतःस्फूर्ततावाद और अराजकतावादी-संघाधिपत्यवाद की प्रवृत्ति। कई ऐसे संगठनों का तर्क है कि मज़दूर आन्दोलन के प्रतिरोध की नयी रणनीतियों को निकालने का काम मज़दूर वर्ग स्वयं करेगा और क्रान्तिकारी पार्टी का कार्य महज़ उन नयी रणनीतियों को थोड़ा और सुसंगत रूप देना होगा! यह एक पुछल्लावाद (tailism) की प्रवृत्ति है और आज के दौर में जबकि मज़दूर वर्ग के आन्दोलन में मज़दूर वर्ग की क्रान्तिकारी हिरावल पार्टी के संस्थाबद्ध हस्तक्षेप और भी ज़्यादा शिद्दत के साथ ज़रूरत है, उस समय इस प्रकार के विचार ख़ास तौर पर नुकसान पहुँचा रहे हैं। मारुति मज़दूर आन्दोलन में मज़दूरों के बीच ‘सहयोग केन्द्र’ चलाने वाले एक संगठन के ज़रिये ऐसे रुझान का हावी होना इस आन्दोलन की असफलता का सबसे बड़ा कारण बना। बजाय आन्दोलन को सचेतन तौर पर राजनीतिक नेतृत्व देने के यह संगठन उसे कभी खाप पंचायतों तो कभी संशोधनवादियों की ट्रेड यूनियनों के गलियारों में घुमाता रहा और अन्ततः उसे थका कर हरा दिया।
बहरहाल, मज़दूर वर्ग के इन विभिन्न हिस्सों के बीच फासीवादी ताक़तों द्वारा आधार बनाने के प्रयासों को विफल करने और उनके बीच क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट आन्दोलन का आधार तैयार करने के लिए क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट आन्दोलन को अपने पुराने पड़ चुके विश्लेषण को और पूर्वाग्रहों को त्यागना होगा और नये रचनात्मक तरीके से मज़दूर वर्ग के बीच क्रान्तिकारी कार्य को अंजाम देना होगा। और इस पूरे कार्य में अनौपचारिक/असंगठित मज़दूर वर्ग के बीच में विशेष ज़ोर दिये जाने की ख़ास अहमियत है।
फासीवाद और किसान आबादी
भारत के फासीवादी कई मामलों में अपने जर्मन व इतालवी पिताओं से ज़्यादा सयाने साबित हुए हैं। मगर कई मामलों में वे उनसे काफ़ी पीछे भी साबित हुए हैं। उनमें से एक मामला है इस बात की ज़रूरत को समझना कि भारत में फासीवादी उभार को थोड़ा टिकाऊ बनाने के लिए टटपुँजिया ग्रामीण आबादी व किसान आबादी में पकड़ बनाना बेहद ज़रूरी है। बीसवीं सदी में यूरोप में कई देशों में फासीवादी आन्दोलन पैदा हुआ। लेकिन हर जगह वह विजयी नहीं हो सका। आनुभविक तौर पर देखें तो हम पाते हैं कि जिन देशों में भी फासीवादी आन्दोलन टटपुँजिया किसान आबादी और ग्रामीण पूँजीपति वर्ग के ठीक-ठाक हिस्से में पकड़ नहीं बना सका, वहाँ-वहाँ वह एक राष्ट्रीय पैमाने का आन्दोलन बनने में असफल रहा। मिसाल के तौर पर, फिनलैण्ड का लापुआ आन्दोलन (1929-32) और पैट्रियॉटिक नेशनल मूवमेण्ट (1932-44)। यही हाल स्वीडन और नॉर्वे के फासीवादी आन्दोलनों का हुआ। जर्मनी और इटली में फासीवादी आन्दोलन के सफल होने का एक बहुत बड़ा कारण था उसका कुलकों और युंकरों, यानी कि धनी किसानों और पूँजीवादी भूस्वामियों के साथ मज़बूत गठजोड़।
भारत में संघ परिवार की राजनीति की गाँवों में पकड़ ऐतिहासिक तौर पर कुछ अपवादों को छोड़कर अधिकांश क्षेत्रों में बेहद कमज़ोर रही है। इसका एक कारण तो यह है कि भारत में फासीवादी नेतृत्व स्वयं इस बात को समझने में काफी समय तक असफल रहा। तो दूसरी ओर इसका दूसरा कारण यह भी है कि भारत में एक विशिष्ट किस्म की कुलक राजनीति का वर्चस्व भी इसमें आड़े आता रहा, जो कभी कांग्रेस के करीब रही, कभी समाजवादियों के करीब तो कभी इनसे बराबर दूरी बनाकर कुछ समय के लिए अपनी स्वायत्तता बनाये रही। लेकिन चरण सिंह-ब्राण्ड कुलक राजनीति का अब भारतीय राजनीति के परिदृश्य में कोई विशेष स्थान नहीं रह गया है। इसके ऐतिहासिक और राजनीतिक कारण हैं। नवउदारवादी नीतियों के दौर में संरक्षण करने के लिए उसके पास बहुत-सी सहूलियतें रह नहीं गयी हैं! नवउदारवादी भूमण्डलीकरण के दौर में अधिशेष विनियोजन में ग्रामीण पूँजीपति वर्ग के हिस्से में सापेक्ष गिरावट आयी है। भारतीय राजनीति के दृश्यपटल से इस क्लासिकीय कुलक राजनीति के प्रस्थान के साथ एक खाली जगह पैदा हुई है। संघ परिवार के विचारकों ने इस दफ़ा अपनी कमी को पकड़ा है और इस ख़ाली जगह को भरने के योजनाबद्ध षड्यन्त्र को अंजाम देना शुरू किया है।
गत चुनावों में भाजपा-नीत राजग गठबन्धन के विजय का एक बहुत बड़ा कारण उत्तर प्रदेश और बिहार में हुई सीटों की बढ़ोत्तरी था। अगर हम उत्तर प्रदेश और बिहार में हुई बढ़ोत्तरी को हटा दें तो हम पाते हैं कि भाजपा के लिए सामान्य बहुमत तक पहुँचना भी मुश्किल हो जाता। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में साम्प्रदायिक तनाव फैलाकर फासीवादी गोलबन्दी करना और विशेष तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के जाट-बहुल क्षेत्रों के साम्प्रदायिकीकरण के काम को योजनाबद्ध तरीके से अंजाम देना भाजपा के लिए काफ़ी फ़ायदेमन्द रहा। किसान राजनीति करने वाली तमाम ताक़तें आज कुलक वर्ग और धनी किसान वर्ग को अधिशेष में हिस्सा बढ़ाने में कोई विशेष सहायता नहीं कर सकती हैं; साथ ही, तमाम किस्म की राजकीय सहायता जो कुलक व धनी किसान वर्गों को उपलब्ध थीं, उनमें भी लगातार कटौती हुई है। यह सच है कि किसान आबादी को पूँजीवादी राज्य द्वारा आज जो भी थोड़ा-बहुत दिया जा रहा है वह सब कुलकों और धनी किसानों को ही मिलता है। मगर यह भी सच है कि वित्तीय, औद्योगिक और वाणिज्यिक पूँजीपति वर्ग को मिल रहे तोहफ़ों की तुलना में यह कुछ ख़ास नहीं है। निश्चित तौर पर, इसमें हमें ज़्यादा चिन्तित होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यह बड़े और छुटभैये लुटेरों का आपसी झगड़ा है!
कृषि व कृषि-सम्बन्धित क्षेत्रों में कारपोरेट घरानों के प्रवेश के साथ भी पुराने पूँजीवादी भूस्वामियों और साथ ही धनी काश्तकार किसान वर्ग के एक छोटे-से हिस्से का तो कारपोरेट सहयोजन हो गया, मगर दूसरे हिस्से को अपने ग्रामीण वर्चस्व के लिए ख़तरा महसूस हो रहा है। आज भारतीय कृषि जिस पूँजीवादी संकट का शिकार है, वह असुरक्षा और अनिश्चितता के माहौल को और भी बढ़ा रहा है। नतीजतन, एक अलग रूप में उच्च मध्यम और धनी काश्तकार किसानों और साथ ही पूँजीवादी भूस्वामियों के बीच भी फासीवादी प्रतिक्रिया की ओर आकृष्ट होने की ज़मीन पैदा हुई। वैसे भी इस वर्ग में हमेशा से ही एक फासीवादी सम्भावनासम्पन्नता थी, जिसका इस्तेमाल समय-समय पर समाजवादी व अन्य ब्राण्ड की कुलक राजनीति ने किया था। इस सम्भावना को हम गाँवों में मौजूद खाप पंचायतों और अन्य ऐसे निकायों में साफ़ तौर पर देख सकते हैं। अब इसी सम्भावना को वास्तविकता में तब्दील करने का कार्य संघ परिवार और भाजपा की राजनीति कर रही है। ये ग्रामीण पूँजीपति और टटपुँजिया वर्ग अपनी वर्ग प्रवृत्ति से ही जनवाद-विरोधी, आधुनिकता-विरोधी (मगर आधुनिक!), ग़रीब-विरोधी, जातिवादी, पितृसत्तावादी और निरंकुश हैं। इन सारी प्रवृत्तियों के फासीवादी विनियोजन में संघ परिवार और भाजपा को बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। एक तरह से कह सकते हैं कि इन प्रतिक्रियावादी वर्गों की यह सम्भावना-सम्पन्नता वस्तुतः कई दशकों से फासीवादी विनियोजन की ही प्रतीक्षा कर रही थी! क्लासिकीय कुलक राजनीति के प्रस्थान के साथ यह प्रतीक्षा समाप्त हो गयी!
इसलिए आज यह समझना भी बेहद अहम हो गया है कि अगर गाँवों में हम फासीवादी गोलबन्दी और आन्दोलन के बरक्स ग्रामीण ग़रीबों के क्रान्तिकारी संगठन नहीं खड़े करते, तो आने वाले समय में हम एक भयंकर संकट के सामने खड़े होंगे। बल्कि इस कार्यभार में पहले ही कुछ देर हो चुकी है। अभी से ही गाँवों नौजवानों के क्रान्तिकारी संगठन, जातितोड़क संगठन, ग्रामीण मज़दूरों की यूनियन, खेतिहर मज़दूरों की यूनियन बनाने के साथ-साथ ग़रीब और परिधिगत किसानों के संगठन भी बनाने होंगे। ताज़ा आँकड़े बता रहे हैं कि ये वर्ग आज गाँवों में बहुसंख्यक हैं। मगर वे स्वयं ही क्रान्तिकारी गोलबन्दी नहीं कर सकते हैं। वहाँ क्रान्तिकारी अभिकर्ता की और भी ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसे में, क्रान्तिकारी कम्युनिस्टों को गाँवों भी अपने क्रान्तिकारी जनसंगठनों का नेटवर्क तैयार करने और अपना व्यापक सामाजिक आधार बनाने पर कार्य करना होगा और इसमें ज़रा भी देर नहीं करनी होगी।
फासीवादी प्रचार की विशिष्टता और उसके सटीक जवाब की चुनौती
जैसा कि हमने ऊपर देखा, फासीवादी प्रचार और गोलबन्दी के आम तौर पर और राष्ट्रीय तौर पर सफल होने के पीछे तमाम किस्म के शहरी और ग्रामीण टटपुँजिया वर्गों में इसकी सफलता अनिवार्य रही है और आज भी अनिवार्य है। मगर हम जिन वर्गों की बात कर रहे हैं वे बेहद भिन्न प्रकृति और प्रवृत्तियों के हैं; उनकी आकांक्षाएँ, उनके वर्ग हित, उनकी संस्कृति आपस में एकदम तुलनीय नहीं प्रतीत होती। वर्गों के इस वैविध्यपूर्ण समुच्चय में फासीवादी राजनीति अपना आधार किस प्रकार तैयार करती है? फासीवादी संगठन अपने प्रचार को किस प्रकार इन विभिन्न प्रकार के वर्गों के बीच प्रभावी बनाते हैं? निश्चित तौर पर, इसमें कुछ भूमिका इन वर्गों के वस्तुगत चरित्र और प्रकृति की भी है। मसलन, तमाम टटपुँजिया वर्गों और विशेष तौर पर तमाम किस्म के लम्पटीकृत वर्गों, चाहे वह टटपुँजिया वर्ग हों या फिर मज़दूर वर्ग, में अपने वर्ग हितों को समझ पाने की क्षमता ठीक अपनी सामाजिक-आर्थिक अवस्थिति के कारण बेहद कम होती है, जैसा कि हम ऊपर देख चुके हैं। इन वर्गों के बीच एक मिथ्या शत्रु को तैयार करना, इसकी प्रतिक्रियावादी गोलबन्दी करना और इसे पूँजीपति वर्ग की नग्न और बर्बर तानाशाही का उपकरण बनाना अपेक्षाकृत आसान होता है। मगर सिर्फ इस वस्तुगत प्रकृति को समझना पर्याप्त नहीं है क्योंकि इन्हीं वर्गों के एक अच्छे-ख़ासे हिस्से को क्रान्तिकारी प्रचार से जीता भी जा सकता है। इसलिए फासीवादी प्रचार की विशिष्टता और उसकी कार्यप्रणाली को समझना उसे निष्फल बनाने के लिए बेहद ज़रूरी है।
इस बाबत जो बात सबसे अहम है वह यह है कि हम फासीवादी प्रचार की एक स्वच्छन्द प्रकार की अनुकूलनीयता (adaptability) या लचीलेपन को समझें। क्रान्तिकारी प्रचार कार्य का मकसद होता है आम मेहनतकश जनता के बीच पूँजीवादी व्यवस्था और उनकी ज़िन्दगी की दुर्वस्था के सच को उजागर करना। ऐसा प्रचार तर्क और विज्ञान पर आधारित ही हो सकता है क्योंकि उसे एक वस्तुगत यथार्थ को सामने लाना है। वह सिद्धान्तहीन नहीं हो सकता है। न ही वह विज्ञान और तर्क से रिक्त हो सकता है। वह व्यवहारवादी तरीके से किसी भी चीज़ का और हर चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। लेकिन फासीवादी प्रचार कार्य के सामने ऐसी कोई बाध्यता नहीं होती है। उसे जनता के सामने एक मिथ्या शत्रु पैदा करना होता है; उसे जनता को एक अन्धभक्ति (fetish) की राजनीतिक वस्तु प्रदान करनी होती है जिससे कि जनता अपने जीवन के हालात के सच्चे कारणों और उसके लिए ज़िम्मेदार ताक़तों को न समझ पाये। यह ‘फेटिश’ उसे नात्सी पार्टी ने यहूदी-विरोध व अन्य अल्पसंख्यकों के विरोध के रूप में दी, भाजपा और संघ परिवार की राजनीति यह ‘फेटिश’ उसे मुसलमान व इस्लाम के प्रति नफ़रत के रूप में देते हैं, फ्रांसीसी फासीवादी इस ‘फेटिश’ को प्रवासी-विरोध के रूप में पेश करते हैं। जब पूरी फासीवादी राजनीतिक प्रचार ही मिथकों को सामान्य बोध (Common Sense) के रूप में स्थापित करने और मिथ्या चेतना तैयार करने पर आधारित होता है, तो ज़ाहिर है उसके हाथ दाँव-पेच के लिए ज़्यादा खुले होते हैं। उसे किसी भी किस्म के सिद्धान्त की आवश्यकता नहीं होती। प्रतिक्रियावादी व्यवहारवाद ही उसका सिद्धान्त होता है। वैसे हर प्रकार की व्यवहारवादी राजनीति में, चाहे वह ड्यूईवादी या अम्बेडकरवादी राजनीति का “प्रगतिशील व्यवहारवाद” (?) ही क्यों न हो, दक्षिणपंथी रास्ता पकड़ लेने की सम्भावना हमेशा मौजूद होती है। आज अम्बेडकरवादी राजनीति जिस नंगे तरीके से शासक वर्गों की गोद में बैठी है वह अम्बेडकर की राजनीति से कोई प्रस्थान या विचलन नहीं है, जैसा कि तमाम उदार अम्बेडरकवादी और विशेष तौर पर वामपंथी अम्बेडरकवादी सोचते हैं। यह अम्बेडकर की व्यवहारवादी राजनीति का तार्किक निर्वाण है। ऐसी व्यवहारवादी राजनीति अपने उद्गम से ही इस संयोग (contingency) पर निर्भर थी कि उसके शीर्ष पर कौन है। हो सकता है कि अम्बेडकर जैसे किसी नेता की मौजूदगी में वह दक्षिणपंथी प्रतिक्रियावाद तक नहीं जाये, मगर इस प्रकार की व्यवहारवादी राजनीति में अपने आपमें ऐसा कुछ नहीं है जो उसे धुर दक्षिणपंथ के साथ खड़ा होने से रोक दे।
बहरहाल, फासीवादी राजनीति की सबसे अहम ख़ासियत होती है उसकी स्वच्छन्द, बल्कि मार्क्सवादी विश्लेषक ज्यॉफ एली के शब्दों का प्रयोग करें तो, कामुक किस्म की अनुकूलनीयता (promiscuous adaptability)। यह हर चीज़ को फासीवादी राजनीति के हितों के अनुसार सहयोजित कर सकती है क्योंकि इसे प्रतिक्रियावादी व्यवहारवाद के अलावा किसी सिद्धान्त से बँधे होने की आवश्यकता नहीं होती है। एक ऐसे किस्म का प्रचार अनगिनत किस्म के आकारहीन और दिशाहीन सामाजिक असन्तोषों को अपने में समेट लेने की क्षमता होती है। कारण यह है कि फासीवादी प्रचार वास्तव में एक साथ इन तमाम अस्पष्ट सामाजिक असन्तोष के शिकार वर्गों को हरेक चीज़ देने, मगर वास्तव में, कुछ भी नहीं देने का वायदा करते हैं। फासीवादी विचारधारा और राजनीति अपनी इस प्रचार पद्धति के ज़रिये एकदम असमान प्रकार के, असम्बद्ध प्रकार के और अक्सर आपस में अन्तरविरोधी किस्म के असन्तोषों, आकांक्षाओं और सपनों को एक सर्वसमावेशी या कहें सर्वसत्तावादी किस्म के लोकरंजक राजनीतिक ढाँचे में सम्मिलित कर लेते हैं। यह क्षमता एक हद तक हर दक्षिणपंथी लोकरंजक राजनीति में होती है, जैसे कि ‘आम आदमी पार्टी’ की राजनीति। मिसाल के तौर पर, कुछ समय पहले तक दिल्ली के टटपुँजिया व्यापारियों, धनी व्यापारियों व दुकानदारों, ठेकेदारों, प्रापर्टी डीलरों के साथ-साथ छोटी-मोटी नौकरी करने वाली निम्न मध्यवर्गीय आबादी, झुग्गीवासियों, लम्पट सर्वहारा आबादी और यहाँ तक कि औद्योगिक मज़दूर वर्ग के भी एक हिस्से को यह लग रहा था कि आम आदमी पार्टी का “भ्रष्टाचार-विरोधी धर्मयुद्ध” उन सबकी सभी समस्याओं का समाधान कर देगा! लेकिन इस प्रकार के यूटोपियाई राजनीति के मुकाबले संघ परिवार का प्रतिक्रियावादी यूटोपिया ज़्यादा मज़बूत है क्योंकि वह शुद्ध रूप से फन्तासी है! फासीवादी प्रचार सच्चाई से जितना दूर और जितना रूमानी फन्तासी के करीब होता है, उतना प्रभावी होता है। इसी के ज़रिये वह जनसमुदायों विशेषकर टटपुँजिया जनसमुदायों के भीतर मौजूद प्रतिक्रियावादी सम्भावना को वास्तविकता में तब्दील कर सकता है। यही कारण है कि भाजपा की राजनीति भारतीय पूँजीवादी राजनीति की कहीं ज़्यादा स्थायी परिघटना है, बनिस्बत ‘आम आदमी पार्टी’ की राजनीति के जिसे कालान्तर में या तो विसर्जित हो जाना है या फिर यह छोटी नाली अन्त में संघ परिवार की राजनीति के बड़े गन्दे नाले में आकर मिलने वाली है!
ख़ैर, मूल बात यह है कि फासीवादी राजनीति की प्रचार पद्धति में यह ख़ासियत होती है कि यह एकदम अतुलनीय अस्पष्ट व आकारहीन सामाजिक असन्तोषों, आकांक्षाओं और सपनों को एक सर्वसत्तावादी और सर्वसमावेशी आमूलगामी यूटोपिया में सम्मिलित कर लेती है या सोख लेती है। नात्सी पार्टी का यूटोपिया जर्मन जनता/नस्ल का एक शुद्ध श्रेष्ठ विचारधारात्मक समुदाय था और भाजपा और संघ परिवार के लिए यह हिन्दुत्ववादी शासन या “रामराज्य” है। (‘विचारधारात्मक’ इस रूप में कि वास्तव में ऐसा कोई समुदाय कभी नहीं था और इसे विशेष वर्ग हितों के मद्देनज़र काल्पनिक और मिथकीय तौर पर गढ़ा जाता है) यहाँ अतीत के और परम्परा के आविष्कार और मिथकीकरण को और फिर इन मिथकों को सामान्य बोध के तौर पर अत्यधिक दुहरावपूर्ण प्रचार के द्वारा स्थापित करने की प्रक्रिया को समझना बेहद ज़रूरी है। यह अनायास नहीं है कि भारत की फासीवादी ताक़तें ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों, विज्ञान, कला, साहित्य, सिनेमा आदि में भगवा मिथकीकरण की एक पूरी प्रक्रिया चला रहे हैं। यह प्रक्रिया एक शुद्ध श्रेष्ठ विचारधारात्मक हिन्दू समुदाय के निर्माण के लिए आवश्यक है। यह कोई अलग-थलग घटना नहीं है। न ही यह फासीवादी अपनी अज्ञानता मात्र के कारण कर रहे हैं। फासीवादियों के साथ इतिहास में भी अपने दौर की कुछ श्रेष्ठ मेधाएँ थीं और आज भी हैं। इनमें तमाम वैज्ञानिक भी हैं, कलाकार भी हैं। ऐसे में, हमें कला और विज्ञान के क्षेत्र में किये जा रहे भगवा मिथकीकरण को सम्पूर्ण फासीवादी राजनीतिक एजेण्डे के अंग के तौर पर समझना चाहिए। तभी इन प्रयासों का सफल विरोध किया जा सकता है। आज एन.सी.ई.आर.टी., इतिहास अनुसन्धान परिषद्, भारतीय फिल्म व टेलीविजन संस्थान, आदि के साथ जो दुराचार संघ परिवार कर रहा है, वह भी केवल अज्ञान या पिछड़ेपन के कारण नहीं है। यह समूचे फासीवादी राजनीतिक एजेण्डा का अभिन्न अंग है।
 अब प्रश्न यह उठता है कि कम्युनिस्ट प्रचार फासीवादी प्रचार के इस ख़तरनाक किस्म के लचीलेपन का मुकाबला किस प्रकार करे? ज़ाहिर है, जो बात कोई भी क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट स्वतः ही समझ सकता है वह यह है कि कम्युनिस्टों को हमेशा जनता के जनसमुदायों को उनके जीवन की ठोस भौतिक, सामाजिक और आर्थिक माँगों के लिए लगातार गोलबन्द और संगठित करना चाहिए, उन्हें यह समझाना चाहिए कि उनके जीवन में ये समस्याएँ क्यों हैं और उनके लिए कौन ज़िम्मेदार है। लेकिन क्या इतना ही काफ़ी है? नहीं! हमारे विचार में इस सन्दर्भ में सर्वहारा पुनर्जागरण और प्रबोधन की पूरी अवधारणा को समझना बेहद ज़रूरी है।
अब प्रश्न यह उठता है कि कम्युनिस्ट प्रचार फासीवादी प्रचार के इस ख़तरनाक किस्म के लचीलेपन का मुकाबला किस प्रकार करे? ज़ाहिर है, जो बात कोई भी क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट स्वतः ही समझ सकता है वह यह है कि कम्युनिस्टों को हमेशा जनता के जनसमुदायों को उनके जीवन की ठोस भौतिक, सामाजिक और आर्थिक माँगों के लिए लगातार गोलबन्द और संगठित करना चाहिए, उन्हें यह समझाना चाहिए कि उनके जीवन में ये समस्याएँ क्यों हैं और उनके लिए कौन ज़िम्मेदार है। लेकिन क्या इतना ही काफ़ी है? नहीं! हमारे विचार में इस सन्दर्भ में सर्वहारा पुनर्जागरण और प्रबोधन की पूरी अवधारणा को समझना बेहद ज़रूरी है।
क्रान्तिकारी शक्तियों को आज सर्वहारा वर्ग और जनता के संघर्षों के गौरवशाली अतीत से सघनता के साथ और रोचक तरीके से परिचित कराया जाना चाहिए। जनता के विभिन्न हिस्सों में प्राचीन भारत की तमाम प्रगतिशील और भौतिकवादी परम्पराओं का प्रचार करना चाहिए। प्राचीन भारत, यानी कि हमारे देश के सुदूर अतीत पर फासीवादियों को अपना एकाधिकार या दावा स्थापित नहीं करने देना चाहिए। वास्तव में, प्राचीन भारत के सच्चे इतिहास को देखें तो उस पर फासीवादी दावा स्थापित होने योग्य ज़्यादा चीज़ें संघ परिवार को मिलेंगी भी नहीं! यही कारण है कि प्राचीन भारत की तमाम प्रगतिशील और भौतिकवादी परम्पराओं का भी संघ परिवार विकृतिकरण करके उसे अपने एजेण्डा में शामिल करने का प्रयास करता रहता है। मिसाल के तौर पर, योग की परम्परा। जब योग दिवस मनाने की नौटंकी चल रही थी तो बहुत से मार्क्सवादियों ने योग की पूरी परम्परा और आनुभविक विज्ञान के भगवा विनियोजन पर प्रश्न खड़ा करने और उसे बेनक़ाब करने की बजाय योग पर ही प्रश्न करना या उसका मखौल बनाना शुरू कर दिया। यह तरीका वास्तव में भगवा ताक़तों को ही फायदा पहुँचा रहा था। साथ ही, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत की ऐसी कई जनपक्षधर परम्पराएँ, बुद्धिजीवी, लेखक, वैज्ञानिक हैं जिनकी प्रगतिशील विरासत से भारत का आम जनमानस अपरिचित है। हम अगर उन्हें अपने सर्वहारा पुनर्जागरण का अंग नहीं बनाते, उन्हें अपने क्रान्तिकारी सांस्कृतिक प्रचार और कार्य का अंग नहीं बनाते तो वास्तव में फासीवादी ताक़तों को समूचे भारतीय अतीत के ही भगवा विनियोजन का अवसर देते हैं। साथ ही, हमें इस सर्वहारा पुनर्जागरण का अंग महज़ भारत की अतीत की प्रगतिशील और जनपक्षधर परम्पराओं को नहीं बनाना चाहिए, बल्कि पूरी दुनिया की भौतिकवादी, प्रगतिशील और जनपक्षधर परम्पराओं, कला, साहित्य और विज्ञान को भी इसका एक हिस्सा बनाना चाहिए। सर्वहारा पुनर्जागरण का यही अर्थ है-दुनिया भर में जनता की प्रगतिशील और भौतिकवादी परम्पराओं और व्यक्तित्वों से और इन परम्पराओं और व्यक्तित्वों के पश्चगामी और प्रतिक्रियावादी ताक़तों के विरुद्ध संघर्ष से जनता के जनसमुदायों का परिचय कराना। यह हमारे अतीत के विषय में जनता के बीच एक ऐसी समझदारी विकसित कर सकता है जो कि उन्हें किसी कल्पित गौरवशाली अतीत की ओर देखते रहना या अतीतग्रस्त रहना नहीं बल्कि भविष्य की ओर देखना और एक बेहतर भविष्य का निर्माण करने के बारे में सिखाये। निश्चित तौर पर, इस कार्य में बच्चों के मोर्चे की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, जोकि पीढ़ी निर्माण के कार्य के लिए अनिवार्य है। साथ ही, इस कार्य को अंजाम देने के लिए क्रान्तिकारी साहित्य के प्रकाशन, क्रान्तिकारी नाट्य व संगीत मण्डली, फिल्म प्रोडक्शन हाउस, फिल्म क्लब समेत सामुदायिक रेडियो जैसे माध्यमों तक का इस्तेमाल करना होगा।
ज़ाहिर है कि केवल अतीत की इस तार्किक और वैज्ञानिक पेशगी से ही हमारे कार्यभार पूरे नहीं होते। भविष्य के सारे सवालों का जवाब अतीत की भौतिकवादी और प्रगतिशील परम्पराओं में भी नहीं मिल सकता है। भविष्य और वर्तमान के प्रश्नों के जवाब को तभी पूर्ण किया जा सकता है, जबकि उसमें नये के तत्व की भी पहचान सही तरीके से की जाय। इतिहास अपने आपको हूबहू दुहराता नहीं है, बल्कि हर बार उच्चतर स्तर पर दुहराता है। इसलिए नये के तत्व की पहचान ज़रूरी है। आज पूरी पूँजीवादी व्यवस्था जिस अन्तकारी संकट का शिकार है और इस मरणासन्न हालत में वह जिस प्रकार की सड़ी चीज़ें पैदा कर रही है उसे केवल अतीत के सन्दर्भ से नहीं समझा जा सकता है। इसलिए आज की साम्राज्यवादी-पूँजीवादी दुनिया के एक वैज्ञानिक-तार्किक विश्लेषण की ज़रूरत है जिससे कि इसकी ऐतिहासिकता को भी समझा जा सके, यानी कि निरन्तरता के तत्व को, और इसकी समकालीनता को भी समझा जा सके, दूसरे शब्दों में, परिवर्तन के तत्व को। यह दूसरा कार्यभार सर्वहारा प्रबोधन का कार्यभार है। निश्चित तौर पर, इस कार्यभार के लिए उन सभी माध्यमों के उपयोग की आवश्यकता होगी जिनकी हमने ऊपर चर्चा की है। साथ ही, मज़दूर वर्ग के एक राजनीतिक अख़बार की विशेष तौर पर आवश्यकता होगी। इसके अतिरिक्त, छात्रों-युवाओं के बीच, स्त्रियों के बीच, युवा व ईमानदार बुद्धिजीवियों के बीच प्रचार हेतु भी तमाम मुखपत्रें की आवश्यकता होगी। इन तमाम मुखपत्रें को ज़्यादा से ज़्यादा बारम्बारता के साथ नियमित तौर पर निकालना सर्वहारा पुनर्जागरण और प्रबोधन के कार्यभार को पूरा करने के लिए अनिवार्य है।
लेकिन सिर्फ इस व्यापक कार्यभार को समझ लेना पर्याप्त नहीं है। यह तो सामान्य राजनीतिक कार्यभार या यूँ कहें कि पहुँच (approach) और पद्धतिशास्त्र (methodology) के विषय में कुछ मोटी बातों को समझने के समान है। इसके अतिरिक्त, आज फासीवादी राजनीति की प्रचार पद्धति को निष्फल करने के लिए बहुत से अन्य पहलुओं को समझना अनिवार्य है। लेनिन की राजनीतिक पद्धति पर लिखते हुए एक जगह हंगेरियाई कम्युनिस्ट ग्यॉर्गी लूकाच ने लिखा था कि लेनिन के राजनीतिक व्यवहार से कम्युनिस्टों के सीखने के लिए जो अहम बात निकलती है वह यह है कि सर्वहारा राजनीतिज्ञ को अपने राजनीतिक वर्चस्व को स्थापित करने और फिर उसकी हिफ़ाज़त करने की प्रक्रिया में दाँव-पेच में कभी भी अपने हाथ नहीं बाँधने चाहिए; उसे अपने दोनों हाथ खुले रखने चाहिए! दूसरे शब्दों में, सर्वहारा राजनीति को सिद्धान्त के मसलों को रणनीति के मसलों से और रणनीति के मसलों को रणकौशल के मसलों से गड्ड-मड्ड नहीं करना चाहिए। चाहे वह मज़दूर आन्दोलन का प्रश्न हो, किसी ट्रेड यूनियन संघर्ष का प्रश्न हो, युवा मोर्चे पर किसी अभियान या आन्दोलन का प्रश्न हो या किसी भी अन्य मोर्चे पर ठोस ज़मीनी कार्रवाइयों का मसला हो, यदि कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी नेतृत्व में हैं तो उन्हें ठोस ज़मीनी कार्रवाइयों में फासीवादी और अन्य प्रतिक्रियावादी ताक़तों से निपटने में ठोस व्यावहारिकता का परिचय देना चाहिए। ज़मीनी संघर्ष के दाँव-पेच में अपने हाथ किसी भी रूप में बाँधने नहीं चाहिए। यह एक बुनियादी शिक्षा है जो हमें विशेष तौर पर लेनिन के राजनीतिक व्यवहार से लेनी चाहिए।
तीसरी अहम बात जिसे समझना हमें ज़रूरी लगता है वह यह है कि किसी भी किस्म की राजनीति का प्रचार किस हद तक प्रभावी होगा इसका निर्धारण करने वाला एक बहुत बड़ा कारक सामाजिक आधार होता है। जिस ताक़त का सामाजिक आधार जितना व्यापक और जितना गहरा होता है, उसके प्रचार की प्रभाविता और जनता के बीच उसकी स्वीकार्यता भी उतनी ही ज़्यादा होती है। फासीवादी ताक़तें इस चीज़ पर पर्याप्त ज़ोर देती हैं कि वे तमाम निम्न मध्यवर्गीय और साथ ही मज़दूर इलाकों में अपने सामाजिक आधार को विस्तारित करें। इसके लिए वे तमाम संस्थाओं का निर्माण करते हैं, मसलन, मित्र मण्डल, पूजा समितियाँ, जिम आदि। अगर इतिहास में जायें तो हम पाते हैं कि रिहायशी इलाकों में सामाजिक आधार विकसित करने के लिए सुधार कार्य और सांस्कृतिक कार्य की परम्परा वास्तव में कम्युनिस्टों की थी; फासीवादियों ने यह चीज़ उनसे ही सीखी थी। यह अनायास नहीं है कि इटली में फासीवादी आन्दोलन का संस्थापक बेनितो मुसोलिनी पहले इतालवी समाजवादी पार्टी का सदस्य था। मगर अफ़सोस की बात है कि कम्युनिस्ट अपनी इस शानदार कार्यशैली को भूल गये और फासीवादियों ने लगभग सभी देशों में और विशेष तौर पर हमारे देश में इस कार्यशैली को मज़बूती से अपना लिया। इस सूरत को बदले बग़ैर हम फासीवाद के प्रतिरोध के कार्यभार को शायद ही पूरा कर पायें। कई दृष्टिकोणों और कई ज़रूरतों से हमें मज़दूरों और निम्न मध्यवर्गीय रिहायशी इलाकों में संस्थाबद्ध रूप से सुधार कार्य और सांस्कृतिक कार्य करने होंगे। जब क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी का तमाम मज़दूर बस्तियों और निम्न मध्यवर्गीय इलाकों में मज़बूत सामाजिक आधार होगा, तभी उनके क्रान्तिकारी प्रचार की प्रभाविता भी दूनी-चौगुनी होगी। इसके बिना, सही तर्क और सही विज्ञान के बावजूद उसकी प्रभाविता को अधिकतम बनाना सम्भव नहीं होगा।
इसके अलावा, अन्य कई सहज समझे जाने वाले कारक हैं जिनका हम ज़िक्र नहीं कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर, हरेक फासीवादी प्रचार के विरुद्ध क्रान्तिकारी ताक़तों को प्रचार करना चाहिए और उसकी असत्यता को जनता के बीच उघाड़कर रख देना चाहिए। फासीवादियों के बीच व्याप्त अनैतिकता और भ्रष्टाचार को लगातार बेनक़ाब करना चाहिए क्योंकि फासीवादियों को अपनी राजनीति को सफल बनाने के लिए हमेशा एक आभा-मण्डल (aura) की आवश्यकता होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पूरी की पूरी फासीवादी राजनीति दरअसल राजनीति का सौन्दर्यीकरण करती है। दूसरे शब्दों में फासीवादी राजनीति हमेशा अपने आपको स्वच्छता, नैतिकता, शुद्धि के पर्याय के तौर पर पेश करती है क्योंकि तभी किसी गौरवशाली और शुद्ध-बुद्ध अतीत पर उसका वैध दावा हो सकता है। इसीलिए आज व्यापम, ललित-गेट आदि जैसे खुलासों से फासीवादियों को काफ़ी नुकसान पहुँच रहा है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहीं न कहीं अपने आपको अपने चुनावी फ्रण्ट भाजपा से इन मामलों में अलग दिखलाने का प्रयास कर रहा है। क्योंकि अगर मुख्य सिक्का ही पिट गया तो फासीवादी राजनीति का बड़ा भारी नुकसान हो जायेगा। इसलिए जो भी लानत-मलामत होनी है वह भाजपा और उसके चन्द नेताओं की होनी चाहिए और ऐसा दिखना चाहिए कि संघ स्वयं भी भाजपा के नेतृत्व पर पार्टी को भ्रष्टाचारियों से शुद्ध करने के लिए दबाव डाल रहा है। यह भी फासीवादियों के प्रचार के अद्भुत रूप से लचीले होने की ही निशानी है। हालाँकि, आज यह लचीलापन बहुत प्रभावी सिद्ध नहीं हो पा रहा है। इसलिए सर्वहारा शक्तियों को फासीवादियों की इस कोर ताक़त पर लगातार चोट करनी चाहिए; इसके लिए पर्चे, लेख, नाटक, गीत आदि तैयार किये जाने चाहिए और इन संघियों की नैतिकता, चाल-चेहरा-चरित्र की पोल लगातार खोलते रहना चाहिए। ये चोटें इनके लिए बड़ी दर्दनाक होती हैं! फासीवादी प्रचार की विशिष्टता और उसे निष्प्रभावी बनाने के विषय में इस संक्षिप्त चर्चा के बाद हम कम्युनिस्ट आन्दोलन द्वारा अतीत में फासीवाद के विरुद्ध संघर्ष की रणनीति और रणकौशल के बारे में संक्षेप में चर्चा करेंगे और साथ ही उससे आज की फासीवाद-विरोधी रणनीति और रणकौशल के बारे में कुछ आम नतीजे निकालने का प्रयास करेंगे। हमने मौजूदा पुस्तिका में कुछ ठोस कार्यभारों को पहले ही रेखांकित किया है। उसी आम दिशा में आगे बढ़ते हुए हम फासीवाद-विरोधी वर्ग मोर्चे के विषय में कुछ परिवर्तनों की ओर ध्यानाकर्षित करना चाहेंगे।
फासीवाद-विरोधी संघर्ष की रणनीति व आम रणकौशल तथा वर्ग मोर्चे के विषय में अतीत में कम्युनिस्ट आन्दोलन की समझदारी और मौजूदा हालात में हुए परिवर्तनों का प्रश्न
प्रथम विश्वयुद्ध और बोल्शेविक क्रान्ति के बाद जब इटली और जर्मनी में फासीवादी राजनीति का उभार हुआ तो दुनिया भर में कम्युनिस्ट क्रान्तिकारियों की ओर से इस नयी परिघटना की कई व्याख्याएँ सामने आयीं। उनमें कई भिन्नताएँ थीं मगर वे कुछ बुनियादी बिन्दुओं पर सहमत थी। उनमें से एक महत्वपूर्ण बिन्दु यह था कि फासीवादी राजनीति का जन्म पूँजीवाद के एकाधिकारी चरण या इज़ारेदारी के चरण का नतीजा है। इसका कारण यह है कि इज़ारेदार पूँजीवाद के दौर में, या दूसरे शब्दों में साम्राज्यवाद के दौर में पूँजीपति वर्ग के लिए हर प्रकार के मज़दूर अधिकार, जनवादी अधिकार का दमन एक अनिवार्यता बन जाती है; आर्थिक कट्टरपंथ राजनीतिक कट्टरपंथ को जन्म देता है। लेकिन ज़ाहिर है कि इज़ारेदार पूँजीवाद आम तौर पर पूँजीवादी प्रतिक्रिया को जन्म देता है, जिसमें से फासीवादी प्रतिक्रिया केवल एक रूप है और एक अहम मायने में वह अन्य पूँजीवादी प्रतिक्रियाओं से भिन्न है, यानी कि इस अर्थ में यह एक प्रतिक्रियावादी सामाजिक आन्दोलन होता है जिसका मुख्य तौर पर टटपुँजिया वर्गों में आधार होता है। आरम्भिक कम्युनिस्ट विश्लेषण में इस बात की पहचान की गयी थी कि फासीवाद का सामाजिक आधार मुख्य तौर पर टटपुँजिया वर्गों के भीतर होता है। इन विश्लेषणों में फासीवाद के गुणों तौर पर सैन्यवाद और अन्धराष्ट्रवाद की भी पहचान की गयी थी और साथ ही यह तथ्य भी इंगित किया गया था कि फासीवाद मज़दूर वर्ग के तमाम श्रम अधिकारों को नष्ट करने के अलावा आम तौर पर जनवादी और नागरिक अधिकारों को भी छीनता है। लेकिन यह स्पष्ट तौर पर रेखांकित किया गया था एक धुर दक्षिणपंथी, मानवतावाद-विरोधी पूँजीवादी प्रतिक्रिया के तौर पर इसका प्रमुख निशाना मज़दूर वर्ग और कम्युनिस्ट होते हैं।
1921 से 1928 के बीच कम्युनिस्ट इण्टरनेशनल की नीति इसी समझदारी से तय हो रही थी। उस समय कोमिण्टर्न ने मज़दूर वर्ग के संयुक्त मोर्चे (United Front of the Working Class) की कार्यदिशा का अनुमोदन किया था। इस कार्यदिशा के अनुसार कम्युनिस्ट शक्तियाँ सामाजिक-जनवादियों के साथ फासीवाद-विरोधी संयुक्त मोर्चा तो बना सकती थीं, मगर साथ ही उनका यह कार्यभार भी पूरे ज़ोर के साथ रेखांकित किया गया था कि उन्हें मज़दूर वर्ग के आन्दोलन में सामाजिक-जनवाद की ग़द्दार भूमिका को विशिष्ट रूप से बेनक़ाब करना चाहिए और उनके सुधारवाद पर चोट करनी चाहिए। 1924 में कोमिण्टर्न की पाँचवीं कांग्रेस में कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी पार्टियों ने सामाजिक-जनवाद की फासीवादी उभार में भूमिका को सटीक तौर पर चिन्हित किया था और कहा था कि ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और एक-दूसरे के पूरक हैं। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए 1928 की कोमिण्टर्न कांग्रेस में सामाजिक-जनवादियों को पहली बार सामाजिक फासीवादी कहा गया। इस समय तक फासीवादी उभार में मज़दूर आन्दोलन में सुधारवादी संशोधनवादियों के असर की भूमिका स्पष्ट तौर पर दिखने लगी थी और कोमिण्टर्न में इसकी सही पहचान की जा रही थी। लेकिन 1928 तक आधिकारिक नीति के अन्तर्गत सामाजिक-जनवादियों के साथ फासीवाद-विरोधी मोर्चा बनाने और साथ में मज़दूर आन्दोलन में उसके ख़िलाफ़ संघर्ष करने की नीति, यानी कि मज़दूर वर्ग के संयुक्त मोर्चे की नीति को स्वीकार किया गया था।
1930-34 के दौरान पूरे यूरोप में फासीवादी ताक़तें तेज़ी से मज़बूत हुईं। जर्मनी में नात्सी पार्टी सत्ता में आ चुकी थी। इसी बीच पहली बार ‘पापुलर फ्रण्ट’ की सोच सामने आने लगी थी। कोमिण्टर्न की सातवीं कांग्रेस 1935 में हुई। इस कांग्रेस में उदार पूँजीवादी जनवाद और फासीवादी तानाशाही में अन्तर किया गया और इसे पूँजीवादी अधिनायकत्व के दो रूपों के तौर पर देखा गया। इसमें फासीवादी तानाशाही को धुर दक्षिणपंथी प्रतिक्रियावादी तानाशाही और पूँजीपति वर्ग के सबसे कट्टरवादी, प्रतिगामी हिस्से की आतंकवादी तानाशाही का नाम दिया गया। ग्यॉर्गी दिमित्रेव ने दलील पेश की कि चूँकि फासीवाद कई देशों में सत्ता में आ चुका है, इसलिए इस समय मज़दूर वर्ग के पास तात्कालिक विकल्प समाजवादी जनवाद और पूँजीवादी जनवाद नहीं है, बल्कि उदार पूँजीवादी जनवाद और फासीवादी तानाशाही है। नतीजतन, इस समय कम्युनिस्ट शक्तियों को व्यापक फासीवाद-विरोधी पॉपुलर फ्रण्ट का निर्माण करना चाहिए। उस समय दूसरे इण्टरनेशनल, यानी पीले इण्टरनेशनल की पार्टियों और साथ ही कोमिण्टर्न की पार्टियों के साझा मोर्चे का आह्वान किया गया और साथ ही इस मोर्चे में अन्य सभी फासीवाद-विरोधी ताक़तों को शामिल करने की बात की गयी। इसके अलावा, इस मोर्चे के अन्तरराष्ट्रीय चरित्र पर विशेष तौर पर बल दिया गया। लेकिन साथ ही दिमित्रेव ने यह भी रेखांकित किया कि यह आम नीति है और इसकी कोई भी यान्त्रिक व्याख्या नुकसानदेह हो सकती है। साथ ही, उन्होंने आगाह किया कि फासीवादी उभार के कई विविध रूप अस्तित्व में आये हैं और उनमें से कुछ औपनिवेशिक और अर्द्धऔपनिवेशिक समाजों में भी अस्तित्व में आये हैं। उनके विरुद्ध संघर्ष की रणनीति स्वतन्त्र जाँच-पड़ताल के बाद ही बनायी जा सकती है क्योंकि तभी उनकी विशिष्टता की पहचान हो सकती है। कोमिण्टर्न की इसी कार्यदिशा की रोशनी में आने वाले कई वर्षों तक कम्युनिस्टों ने अपनी फासीवाद-विरोधी रणनीति तैयार की। हंगरी में ग्यॉर्गी लूकाच ने भी फासीवाद-विरोधी जनमोर्चे (Anti-Fascist People’s Front) के निर्माण की बात की जिसका मकसद होगा जनता की जनवादी तानाशाही की स्थापना जो कि साम्राज्यवाद के युग में बुर्जुआ शासन के तहत अस्तित्व में आ ही नहीं सकती है। लेकिन ऐसी व्यवस्था का वर्ग चरित्र बुर्जुआ जनवादी ही होगा क्योंकि लूकाच के अनुसार हंगरी में कृषि क्षेत्र में मुख्य कार्य बुर्जुआ भूमि सुधार का ही था।
द्वितीय विश्वयुद्ध की समाप्ति के बाद भी विश्व के कम्युनिस्ट आन्दोलन में पॉपुलर फ्रण्ट की नीति आम तौर पर स्वीकृत नीति बन गयी। समय बीतने के साथ यह कम्युनिस्टों के बीच एक आकाशवाणी के समान सत्य के तौर पर स्थापित हो गया कि फासीवाद-विरोधी कम्युनिस्ट रणनीति हर-हमेशा पॉपुलर फ्रण्ट की ही होगी! हमारे विचार में यह एक अनैतिहासिक नज़रिये को अपनाने के कारण हुआ है। कम्युनिस्ट आन्दोलन में भी हमेशा से पॉपुलर फ्रण्ट की नीति ही स्वीकार्य नीति नहीं रही है। जैसा कि हमने ऊपर प्रदर्शित किया, विशेष तौर पर 1921 से 1928 के दौर में मज़दूर वर्ग के संयुक्त मोर्चे की रणनीति को अपनाया गया था। पॉपुलर फ्रण्ट की रणनीति केवल तब अपनायी गयी जब यूरोप के तमाम देशों में मज़दूर आन्दोलन निर्णायक तौर पर परास्त हो चुका था और जर्मनी और इटली में फासीवादी सत्ता मज़बूती से स्थापित हो चुकी थी और एक भयंकर नरसंहार और विनाश का ख़तरा पूरी मानवता के सिर पर था। उस दौर में भी वास्तव में किस हद तक बुर्जुआ और सामाजिक-जनवादी ताक़तों ने ऐसे पॉपुलर फ्रण्ट में सक्रिय और प्रभावी भागीदारी की, यह शोध का विषय हो सकता है। सरसरी निगाह से देखा जाय तो फासीवाद का विरोध सबसे बहादुरी और प्रभाविता के साथ करने में कम्युनिस्टों के बाद अगर किसी शक्ति का नाम आता है तो वे अराजकतावादी थे, जिन्होंने सशस्त्र तौर पर कई स्थानों पर फासीवादियों से ज़बर्दस्त टक्कर ली। कई जगहों पर कम्युनिस्ट और अराजकतावादी साथ में फासीवादियों के ख़िलाफ़ लड़े। सामाजिक-जनवादी ताक़तें ज़्यादातर स्थानों पर आत्मसमर्पण की मुद्रा में थीं और कहीं-कहीं ही कुछ सशस्त्र प्रतिरोध कर रही थीं। इसलिए उस दौर में भी पॉपुलर फ्रण्ट में वास्तव में उदार बुर्जुआ या सामाजिक-जनवादी ताक़तों की औपचारिक ही भूमिका थी, न कि वास्तविक। वास्तविक तौर पर अधिकांश जगहों पर क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट और अराजकतावादी ही फासीवादी ताक़तों के विरुद्ध लड़ रहे थे। बहरहाल, फिर भी पॉपुलर फ्रण्ट की नीति अगर अराजकतावादी शक्तियों को भी साथ लेने की निगाह से देखा जाय, तो सही थी। कम-से-कम तात्कालिक तौर पर, यही उस समय की कमोबेश व्यावहारिक नीति प्रतीत होती है।
मगर आज के दौर में क्या पॉपुलर फ्रण्ट की नीति क्या फासीवाद के ख़िलाफ़ संघर्ष की आम रणनीति हो सकती है? हमारे विचार में यह मुश्किल है। इसका कारण यह है कि 1934-35 के दौर से आज पूँजीवाद और पूरी पूँजीवादी दुनिया बहुत आगे निकल आयी है। उस दौर में सामाजिक-जनवादी शक्तियों में जो कुछ प्रगतिशील बचा था, वह भी आज कितना बचा है, यह देखना पड़ेगा। वास्तव में, रूस और चीन में सत्ता में आने और रहने के बाद भी पूरे सामाजिक-जनवाद के चरित्र में और ज़बर्दस्त प्रतिक्रियावादी परिवर्तन हुए हैं। क्या आज चीन की सामाजिक-फासीवादी और धीरे-धीरे विश्व पूँजीवाद में अपनी वर्चस्वकारी स्थिति को स्थापित करने की प्रक्रिया में व्यस्त चीनी बुर्जुआज़ी से यह उम्मीद की जा सकती है कि वह किसी फासीवाद-विरोधी मोर्चे में वास्तविक (औपचारिक नहीं!) और सक्रिय (जुबानी जमाख़र्च नहीं!) वाली भूमिका निभायेगी? क्या आज माकपा और भाकपा जैसी शक्तियों से यह उम्मीद की जा सकती है कि वे भारत में फासीवादी उभार के ख़िलाफ़ नपुंसक किस्म का प्रतीकवाद करने के अलावा कोई जुझारू भूमिका निभायेंगे? अगर ऐसा करना होता तो क्या 2002 के गुजरात नरसंहार के ख़िलाफ़ ही ये सामाजिक-जनवादी पार्टियाँ पूरे देश में आम हड़ताल का आह्वान नहीं कर सकती थीं, क्योंकि सबसे बड़ी ट्रेड यूनियनें इन्हीं के पास हैं? ये ताक़तें आज बुर्जुआ चुनावी खेल में इस कदर डूबी हुई हैं और पूँजीपति वर्ग के साथ इनका समेकन 1930 के दशक की तुलना में इतना बढ़ गया है कि ये फासीवादी उभार के विरुद्ध कोई भी जुझारू कदम उठाने की क्षमता खो बैठी हैं। कुल मिलाकर इन संशोधनवादी पार्टियों से जुड़े या उनके करीब पड़ने वाली कुछ मार्क्सवादी बुद्धिजीवी हैं जो कि फासीवादी उभार के इतिहास और जन्मकुण्डली को खोलने में एक सराहनीय भूमिका निभाते हैं। लेकिन विडम्बना की बात है कि उनकी ये रचनाएँ भी आम तौर पर अंग्रेज़ी में होती हैं और इनको भी जनता के बीच जनता की भाषा में ले जाने का कार्य आम तौर पर स्वतन्त्र मार्क्सवादी या फिर क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टियाँ और समूह ही करते हैं। संक्षेप में, ये तमाम उदार पूँजीवादी और सामाजिक-जनवादी ताक़तें वह थोड़ी-बहुत क्षमता भी खो चुके हैं, जो कि 1930 के दशक में इन्हें ‘पॉपुलर फ्रण्ट’ जैसे किसी फासीवाद-विरोधी मोर्चे में शामिल होने के योग्य बनाती थी। आज के दौर में ये जिन भी फासीवाद-विरोधी मोर्चों में शामिल भी होते हैं, उनमें भी ये उसकी धार को कुन्द करने, कुछ उदारवादी रवैया अपनाने की वकालत करने, कायरता प्रदर्शित करने और हर प्रकार की जुझारू कार्रवाई से बचने के प्रयास में लगे रहते हैं। इस रूप में ये ताक़तें आज ऐसे मोर्चे की शक्ति को कमज़ोर ही करती हैं।
इस परिवर्तन का कारण क्या है? सामाजिक जनवाद वास्तव में एक टटपुँजिया पूँजीवादी विचारधारा ही है। इसका सामाजिक आधार भी वास्तव में टटपुँजिया वर्गों के बीच ही होता है; यह दीगर बात है कि यही टटपुँजिया वर्ग संकट के दौर में फासीवाद का आधार बन जाते हैं। कारण यह है कि सामाजिक जनवादी राजनीति पूँजीवाद की समृृद्धि के दौरों में और सामान्य दौरों में इन्हीं वर्गों को मिली हुई सहूलियतों की हिफ़ाज़त करने का काम करती हैं। लेकिन जब संकट के दौर में व्यवस्था इतना अधिशेष उत्पन्न नहीं करती जिससे कि इन सहूलियतों का ख़र्च उठाया जा सके, तो सामाजिक-जनवाद के समझ नहीं आता है कि वह क्या करे! नग्न रूप से नवउदारवादी होना उसके लिए सम्भव नहीं होता क्योंकि इससे वह अपने बचे-खुचे वोटर भी खो देगा और वैसे भी बुर्जुआ राजनीति के उस खेमे में पहले ही माँग से ज़्यादा आपूर्ति है; न ही वह क्रान्तिकारी रास्ते को अपना सकता है! दूसरे शब्दों में कहें तो सामाजिक-जनवाद मन्दी और राजनीतिक संकट से घिरी पूँजीवादी व्यवस्था से निपटना नहीं जानता क्योंकि क्रान्तिकारी रास्ता उसकी कल्पना के सीमान्त के दूसरी ओर होता है। नतीजतन, वही वर्ग जो सहूलियतें मिलने तक सामाजिक-जनवाद का आधार होता है, इन सहूलियतों के कम होने या ख़त्म होने पर आम तौर पर पूँजीवादी प्रतिक्रिया और विशिष्ट तौर पर फासीवादी प्रतिक्रिया का सामाजिक आधार बनता है।
ख़ैर, हम अभी जिस तथ्य की ओर ध्यानाकर्षित करना चाहते हैं वह यह है कि सामाजिक-जनवाद का सामाजिक आधार हमेशा से ही पूँजीवादीकृत मज़दूर वर्ग (सफेद कॉलर वाले कुलीन मज़दूर), टटपुँजिया वर्ग (मँझोले किसान, छोटे उद्यमी व व्यवसायी आदि) और पेशेवर मध्यवर्ग का एक हिस्सा होता है। 1930 के दशक में इन वर्गों में कुछ प्रगतिशील सम्भावना बची थी। दूसरे शब्दों में मज़दूर वर्ग के आन्दोलन के लिए खाते-पीते मध्यवर्ग की प्रासंगिकता एक हद तक बची हुई थी। लेकिन आज भूमण्डलीकरण और नवउदारवाद के दौर में यह वर्ग मज़दूर वर्ग के साथ अपनी ऐतिहासिक ग़द्दारी को अंजाम दे चुका है। आज इसके कुछ सदस्य मज़दूर आन्दोलन के साथ आ सकते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा इसका एक बेहद छोटा-सा हिस्सा मज़दूर आन्दोलन के साथ आ सकता है। मूलतः और मुख्यतः खाता-पीता मध्यवर्ग मज़दूर वर्ग के साथ अपना विश्वासघात कर चुका है। मध्यवर्ग के चरित्र में आये इस बदलाव के कारण इसकी पूरी ऐतिहासिक भूमिका में भी परिवर्तन आया है। आज के दौर में पूँजीवादी व्यवस्था ने खाते-पीते मध्यवर्ग के एक अच्छे-ख़ासे हिस्से को तमाम किस्म की सुविधाओं और ऋण-वित्तपोषित उपभोग की नीति द्वारा सहयोजित कर लिया है। इसका अधिकांश हिस्सा संकट के दौर में बर्बाद होने पर भी मज़दूर वर्ग के साथ नहीं आता, बल्कि फासीवाद का ही आधार बनता है क्योंकि इसकी आकांक्षाएँ मूलतः पूँजीवादी हो चुकी हैं।
खाते-पीते मध्यवर्ग के चरित्र में आये इन ऐतिहासिक परिवर्तनों के फलस्वरूप और साथ ही रूस और चीन में सामाजिक-जनवादी सत्ताओं के सामाजिक फासीवाद के पूर्ण रूप से अनावृत्त होने के ऐतिहासिक अनुभवों के बाद सामाजिक-जनवाद के चरित्र में भी अहम बदलाव हुए हैं। आज उनमें वह प्रगतिशीलता भी नहीं बची रह गयी है जो कि एक फासीवाद-विरोधी पॉपुलर फ्रण्ट के स्थायी और भरोसेमन्द मित्र बनने के लिए एक अनिवार्य पूर्वशर्त है। आज अन्य उदार पूँजीवादी ताक़तों में भी किसी में यह राजनीतिक पुंसत्व नहीं रह गया है कि वह फासीवादी उभार का सक्रिय और जुझारू तौर पर मुकाबला करने के लिए आगे आये। ऐसे में, कुछ मुद्दों या घटनाओं पर ऐसी ताक़तों के साथ संयुक्त गतिविधि करना एक बात हो सकती है और इसमें कोई गुरेज़ भी नहीं होना चाहिए। मगर सकारात्मक तौर पर ऐसा कोई फासीवाद-विरोधी मोर्चा बनाना हो तो निश्चित तौर पर क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट ताक़तों को स्वयं अपनी ताक़त और प्रयासों पर ज़्यादा भरोसा करना चाहिए; वैसे तो भारत में उस प्रकार ऐसे अराजकतावादी समूह या संगठन पाये नहीं जाते हैं जो कि जुझारू तरीके से फासीवादियों के ख़िलाफ़ संघर्ष करने को तैयार हों (जैसे कि बीसवीं सदी के पूर्वार्द्ध में और आज भी यूरोप के तमाम देशों में पाये जाते हैं) , मगर फिर भी अगर ऐसे अराजकतावादी समूह हों तो उनके साथ फासीवाद-विरोधी मोर्चा बनाया जा सकता है।
 दूसरे शब्दों में कहें तो आज फासीवाद-विरोधी पॉपुलर फ्रण्ट की कार्यदिशा कितनी कारगर होगी इस पर इतिहास ने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न-चिन्ह खड़े कर दिये हैं। पॉपुलर फ्रण्ट की सोच पर आज प्रश्न इसलिए भी खड़े हो गये हैं कि आज उदार पूँजीपति वर्ग के पूरे चरित्र में भी कुछ बुनियादी बदलाव आये हैं। इज़ारेदार पूँजीवाद जिस तेज़ी से लेनिन के समय से कहीं ज़्यादा परजीवी, अनुत्पादक, सट्टेबाज़ और जुआखोर बना है, उसी गति से तथाकथित उदार पूँजीपति वर्ग की सारी उदारता, बची-खुची जनवादी स्पिरिट जाती रही है। हम यह प्रश्न भी पूछ सकते हैं कि आज मज़दूर वर्ग के आन्दोलनों के दमन और उसके अधिकारों को छीने जाने की बात करें तो क्या दुनिया भर के देशों के उदार पूँजीपति वर्ग उन देशों के फासीवादियों से क्या ज़्यादा पीछे ठहरते हैं? यह उदार पूँजीपति वर्ग 1930 के दशक में भी कोई ज़्यादा प्रगतिशील नहीं रह गया था, मगर आज तो इसकी प्रगतिशीलता की बात एक अच्छा राजनीतिक चुटकुला हो सकती है। साथ ही, आज के फासीवादी उभार के जवाब में क्या किसी उदार पूँजीवादी जनवाद के लिए लड़ना सम्भव है? दूसरे शब्दों में, क्या उदार पूँजीवादी जनवाद जैसी कोई चीज़ अब अस्तित्वमान है? उन्नत दुनिया तक में इस उदार पूँजीवादी जनवाद कितना उदार और कितना जनवादी रह गया है, इस पर गहरे सवालिया निशान लग रहे हैं। ऐसे में, फासीवादी उभार के समक्ष आज मज़दूर वर्ग के पास विकल्प उदार पूँजीवादी जनवाद नहीं बल्कि समाजवाद है। इसलिए कोई व्यक्ति किसी भी वर्ग से क्रान्ति का मित्र और फासीवाद का विरोधी हो सकता है मगर “उदार” पूँजीपति वर्ग के किसी भी हिस्से को फासीवाद-विरोधी मोर्चे में शामिल करने की बात करना आज कितना अर्थपूर्ण होगा, इस पर सोचना पड़ेगा।
दूसरे शब्दों में कहें तो आज फासीवाद-विरोधी पॉपुलर फ्रण्ट की कार्यदिशा कितनी कारगर होगी इस पर इतिहास ने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न-चिन्ह खड़े कर दिये हैं। पॉपुलर फ्रण्ट की सोच पर आज प्रश्न इसलिए भी खड़े हो गये हैं कि आज उदार पूँजीपति वर्ग के पूरे चरित्र में भी कुछ बुनियादी बदलाव आये हैं। इज़ारेदार पूँजीवाद जिस तेज़ी से लेनिन के समय से कहीं ज़्यादा परजीवी, अनुत्पादक, सट्टेबाज़ और जुआखोर बना है, उसी गति से तथाकथित उदार पूँजीपति वर्ग की सारी उदारता, बची-खुची जनवादी स्पिरिट जाती रही है। हम यह प्रश्न भी पूछ सकते हैं कि आज मज़दूर वर्ग के आन्दोलनों के दमन और उसके अधिकारों को छीने जाने की बात करें तो क्या दुनिया भर के देशों के उदार पूँजीपति वर्ग उन देशों के फासीवादियों से क्या ज़्यादा पीछे ठहरते हैं? यह उदार पूँजीपति वर्ग 1930 के दशक में भी कोई ज़्यादा प्रगतिशील नहीं रह गया था, मगर आज तो इसकी प्रगतिशीलता की बात एक अच्छा राजनीतिक चुटकुला हो सकती है। साथ ही, आज के फासीवादी उभार के जवाब में क्या किसी उदार पूँजीवादी जनवाद के लिए लड़ना सम्भव है? दूसरे शब्दों में, क्या उदार पूँजीवादी जनवाद जैसी कोई चीज़ अब अस्तित्वमान है? उन्नत दुनिया तक में इस उदार पूँजीवादी जनवाद कितना उदार और कितना जनवादी रह गया है, इस पर गहरे सवालिया निशान लग रहे हैं। ऐसे में, फासीवादी उभार के समक्ष आज मज़दूर वर्ग के पास विकल्प उदार पूँजीवादी जनवाद नहीं बल्कि समाजवाद है। इसलिए कोई व्यक्ति किसी भी वर्ग से क्रान्ति का मित्र और फासीवाद का विरोधी हो सकता है मगर “उदार” पूँजीपति वर्ग के किसी भी हिस्से को फासीवाद-विरोधी मोर्चे में शामिल करने की बात करना आज कितना अर्थपूर्ण होगा, इस पर सोचना पड़ेगा।
यही बात राष्ट्रीय पूँजीपति वर्ग पर भी लागू होती है, जो कि अब इतिहास की संग्रहालय की वस्तु बन चुका है! दुनिया के किसी भी देश में आज बुर्जुआ वर्ग का कौन-सा हिस्सा जनता के साथ है? कोई नहीं! बुर्जुआ वर्ग के हरेक हिस्से को आज सत्ता में कम या ज़्यादा भागीदारी हासिल है। अपनी भागीदारी के हिस्से को बढ़ाने के लिए उनमें परस्पर प्रतिस्पर्द्धा और अन्तरविरोध होना और हमारे द्वारा उन अन्तरविरोधों का लाभ उठाने के दाँव-पेच अलग मसला हैं, मगर अपने इन तमाम अन्तरविरोधों के बावजूद मेहनतकश ग़रीब जनता के विरुद्ध वे एक हैं। एक उदाहरण से हम अपनी बात स्पष्ट करना चाहेंगे। हमने देखा था कि जब दिल्ली में इस सहस्राब्दी की शुरुआत में प्रदूषण के नाम पर छोटे उद्योग-धन्धे आदि दिल्ली से बाहर किये जा रहे थे या बन्द किये जा रहे थे और उसके बाद जब खुदरा व्यापार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की बात हो रही थी तो हमारे देश के नवजनवादी क्रान्ति मानने वालों ने किस प्रकार अपना मखौल बनाया था। मतलब, एक मज़ेदार दृश्य उपस्थित हुआ था! नवजनवादी क्रान्ति मानने वाले कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी इस तथाकथित “राष्ट्रीय पूँजीपति वर्ग” (छोटे मालिक, उद्यमी, दुकानदार आदि) के पीछे यह चिल्लाते हुए भाग रहे थे कि ‘हम तुम्हारे असली हिमायती हैं’, तो दूसरी ओर यह “राष्ट्रीय पूँजीपति वर्ग” भाजपा के तमाम स्वदेशी की बात करने वाले मंचों के पीछे यह कहते हुए भाग रहा था कि ‘तुम तो हमारे थे!’; मगर भाजपा देशी-विदेशी बड़े पूँजीपतियों के पीछे भाग रही थी कि ‘हम तुम्हारे असली नुमाइन्दे हैं!’ और यह देशी-विदेशी बड़ी पूँजी देश की मेहनत और कुदरत को खुले हाथों से लूटने के लिए भाग रही थी! मतलब पूरा दृश्य मज़ेदार था!
आज किसी फासीवाद-विरोधी पॉपुलर फ्रण्ट के लिए उदार पूँजीपति वर्ग या राष्ट्रीय पूँजीपति वर्ग के पीछे भागना ऐसा ही मज़ाकिया दृश्य उपस्थित कर सकता है। ये वर्ग आज अपने तरह से हर प्रकार की प्रतिक्रिया के साथ खड़े हैं और संकट के कारण पैदा होने वाली अनिश्चितता हर दिन उन्हें विभिन्न प्रकार के प्रतिक्रियावादियों की बाँहों में धकेल रही है। वे अपनी हर प्रकार की जनवादी सम्भावना से आज लगभग रिक्त हो चुके हैं और इस रूप में फासीवाद से लड़ने की शक्ति और पुंसत्व और कुछ भी नया पैदा करने की उर्वरता वे खो चुके हैं।
हमारे विचार में पिछले सात-आठ दशकों में और विशेष तौर पर पिछले पाँच दशकों में उदार पूँजीपति वर्ग और खाते-पीते मध्य वर्ग के चरित्र में कुछ बुनियादी बदलाव आये हैं और राष्ट्रीय पूँजीपति वर्ग इतिहास के रंगमंच पर अपनी ‘कैमियो’ भूमिका निभाकर प्रस्थान कर चुका है। हमारा मानना है कि भूमण्डलीकरण के दौर के परजीवी, सट्टेबाज़, खोखले और मरणासन्न इज़ारेदार पूँजीवाद के इस दौर में हमें एक नये रूप और नये अर्थ में मज़दूर वर्ग के संयुक्त मोर्चे की बात करनी चाहिए। नये रूप और नये अर्थ में इसलिए कि अब सामाजिक-जनवादी/सामाजिक फासीवादी ताक़तों के साथ फासीवाद-विरोध के कार्य में कोई रणनीतिक मोर्चा बनेगा, इसकी गुंजाइश कम ही है; आज उनके साथ मुद्दा-आधारित फासीवाद विरोधी मोर्चे बन सकते हैं, मगर कोई दीर्घकालिक फासीवाद-विरोधी मोर्चे में भाकपा, माकपा आदि जैसी ताक़तों को शामिल करना पूरे उद्देश्य को ही बेकार कर देगा। लेकिन निश्चित तौर पर ऐसे फासीवाद-विरोधी मोर्चे में समाज के तमाम जेनुइन और जुझारू जनवादी, प्रगतिशील व सेक्युलर तत्वों को शामिल करने की पुरज़ोर कोशिश की जानी चाहिए। आज ऐसे किसी मोर्चे के अभाव में ये तत्व या तो निराश हैं या फिर विकल्पहीनता में सामाजिक-जनवादियों व संशोधनवादियों की प्रतीकात्मक कवायदों का हिस्सा बनते हैं। लेकिन अगर मज़दूर वर्ग का फासीवाद-विरोधी संयुक्त मोर्चा खड़ा किया जाय तो इन तत्वों को साथ लिया सकता है।
हमें जिस प्रकार के मज़दूर वर्ग के संयुक्त मोर्चे की आज फासीवाद के प्रतिरोध हेतु ज़रूरत है उसमें कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी शक्तियों का एकजुट होना एक अहम ज़रूरत है। इसके अतिरिक्त विशेष तौर पर अनौपचारिक क्षेत्र व असंगठित क्षेत्र के विराटकाय मज़दूर वर्ग को फासीवाद के विरुद्ध एकजुट करने की आवश्यकता है; दूसरी सबसे बड़ी आवश्यकता है भारत के विशाल निम्न मध्यवर्ग को एकजुट करना और उन्हें फासीवाद के हत्थे न चढ़ने देना; याद रहे कि इस निम्न मध्यवर्ग को एक अच्छा-ख़ासा हिस्सा अर्द्धमज़दूर जैसा ही है और उसकी नैसर्गिक एकता खाते-पीते मध्यवर्ग के साथ नहीं बल्कि मज़दूर वर्ग के साथ बनती है। तीसरा अहम कार्य होगा जाति-विरोधी जुझारू जनसंघर्षों को और साथ ही पितृसत्ता-विरोधी स्त्री संघर्षों को इस मोर्चे का अंग बनाना; आज इन संघर्षों की शक्ति और सम्भावनासम्पन्नता में वृद्धि हुई है और इन संघर्षों के नेतृत्व को सर्वहारा शक्तियों को अपने हाथ में लेकर उसे अम्बेडकरवादी राजनीति के जंजाल से निकालना चाहिए और साथ ही स्त्री संघर्षों को बुर्जुआ नारीवाद के गर्त से बाहर निकालना चाहिए। कभी भूलना नहीं चाहिए कि दलितों और स्त्रियों के भी सबसे जुझारू और लड़ाकू संघर्ष क्रान्तिकारी कम्युनिस्टों के नेतृत्व में हुए हैं न कि विभिन्न प्रकार के सुधारवादियों, व्यवहारवादियों, अम्बेडकरवादियों और बुर्जुआ नारीवादियों के नेतृत्व में। क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट शक्तियों को एक बार फिर से इन मोर्चों पर अपने वर्चस्व को स्थापित कर इन संघर्षों को एक सही क्रान्तिकारी दिशा में मोड़ने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन यह तो एक आम कार्यभार है जिस पर हर सूरत में कम्युनिस्टों को काम करना ही होगा। जब तक ऐसा नहीं भी होता है, तब तक भी ‘जेनुइन’ जाति-विरोधी संघर्षों और पितृसत्ता-विरोधी संघर्षों को फासीवाद-विरोधी मोर्चे में शामिल करना चाहिए। जो ईमानदार और जुझारू अराजकतावादी विचारधारा को मानने वाले लोग हैं (हालाँकि ऐसे समूह भारत में बिरले ही मिलते हैं!) वे भी फासीवाद-विरोधी संघर्ष के ज़्यादा टिकाऊ और सशक्त मित्र बन सकते हैं। लेकिन चूँकि ऐसे क्रान्तिकारी और सक्रिय अराजकतावादियों की परम्परा ही भारत में कमज़ोर है, इसलिए उनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता है। भारत में ज़्यादातर अराजकतावादी वस्तुतः निष्क्रिय उग्रपरिवर्तनवादी हैं; यानी बातें काफ़ी गर्म करते हैं, मगर व्यावहारिक तौर पर कुछ भी नहीं करते! विश्वविद्यालय परिसरों और अन्य कुलीन बौद्धिक दायरों से बाहर उनकी मौजूदगी नगण्य है। मगर फिर भी अगर ऐसे ‘जेनुइन’ अराजकतावादी समूह और संगठन हों जिनकी मज़दूर-वर्गीय कार्यदिशा हो, तो फासीवाद-विरोधी संयुक्त मोर्चे में उन्हें शामिल होना चाहिए।
इसके अलावा, एक क्षेत्र जिसमें कि क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट ताक़तें विशेष तौर पर कमज़ोर हैं, वह है ग्रामीण मज़दूर वर्ग (जिसमें कि खेतिहर और ग़ैर-खेतिहर मज़दूर दोनों ही शामिल हैं) के बीच अपने क्रान्तिकारी जनसंगठनों की मौजूदगी। यह फासीवाद-विरोधी मोर्चे के लिए आज विशेष तौर पर महत्वपूर्ण है। कुलक राजनीति के प्रस्थान के साथ फासीवाद ने गाँवों अपना मज़बूत वर्ग मित्र ढूँढ लिया है। अगर क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट ताक़तें गाँवों में अपने वर्ग मित्रों को साथ लेकर वर्ग संघर्ष में उतरने को तैयार नहीं हैं, तो तमाम किस्म की आदिम धारणाओं, वर्ग चेतना की कमी और जातिगत वर्चस्व के कारण ग्रामीण मज़दूरों का एक भी एक अच्छा-ख़ासा हिस्सा धनी काश्तकार किसानों और पूँजीवादी भूस्वामियों के संगठनों का पुछल्ला बनकर फासीवादियों के पैदल सैनिकों की संख्या ही बढ़ायेगा। यह क्रान्तिकारी मज़दूर आन्दोलन के लिए प्राणान्तक सिद्ध हो सकता है। इस बात को समझने में अब ज़्यादा देर नहीं की जा सकती; हमारे पास कतई वक़्त की कमी है।
जिन राजनीतिक ताक़तों और सामाजिक वर्गों को हम फासीवाद-विरोधी मज़दूर वर्ग के संयुक्त मोर्चे में शामिल करने की बात कर रहे हैं, वह आज समाज की भारी बहुसंख्या है। लेकिन इस बहुसंख्या को गोलबन्द और संगठित करने के लिए महज़ फासीवाद के इतिहास या उसकी सैद्धान्तिक परिभाषा को समझ लेना पर्याप्त नहीं होगा। हमें यह भी समझना होगा कि बीसवीं सदी में फासीवादी उभार की परिघटना आज इक्कीसवीं सदी में हूबहू दुहरायी नहीं जाने वाली है। फासीवादी उभार की विचारधारा और राजनीति में विश्व पूँजीवादी व्यवस्था और उसके संकट के चरित्र में आने वाले बदलावों के साथ जो बदलाव आये हैं, उन्हें समझना आज अनिवार्य है। इसके बिना, फासीवाद के प्रतिरोध के लिए मज़दूर वर्ग का क्रान्तिकारी आन्दोलन कोई रणनीति नहीं बना सकता है। मौजूदा पुस्तिका में फासीवादी उभार की परिघटना का विश्लेषण करते हुए हमने कुछ परिवर्तनों की ओर ध्यानाकर्षित करने का प्रयास किया था। मगर फिर भी हमें इस विश्लेषण में कुछ अहम छूटे हुए नुक्तों को जोड़ना मोदी सरकार और फासीवाद के इस नये उभार के समकालीन सन्दर्भ में ज़रूरी महसूस हुआ। ग़ौरतलब है कि यह पुस्तिका उस समय लिखी गयी थी जब कुछ अतिआशावादी निठल्ला वामपंथी और साथ ही कुछ क्रान्तिकारी वामपंथी फासीवाद को चुक गयी शक्ति क़रार दे रहे थे। हमने तब भी आग्रहपूर्वक कहा था कि ऐसा सोचना क्रान्तिकारी वाम की भारी भूल सिद्ध होगा। 2014 के लोकसभा चुनावों में फासीवादी शक्तियों की अभूतपूर्व जीत ने इस बात को सिद्ध भी किया। एक ऐसे दौर में हमने इस पुस्तिका के साथ यह पश्चलेख जोड़ा है और हम उम्मीद करते हैं कि इससे हम इस पुस्तिका में पेश अपनी समझदारी को और विस्तार के साथ व्याख्यायित कर पाये होंगे और साथ ही उसे विस्तार दे पाये होंगे।
(16 जुलाई, 2015)
‘मज़दूर बिगुल’ की सदस्यता लें!
वार्षिक सदस्यता - 125 रुपये
पाँच वर्ष की सदस्यता - 625 रुपये
आजीवन सदस्यता - 3000 रुपये
आर्थिक सहयोग भी करें!
 बुर्जुआ अख़बार पूँजी की विशाल राशियों के दम पर चलते हैं। मज़दूरों के अख़बार ख़ुद मज़दूरों द्वारा इकट्ठा किये गये पैसे से चलते हैं।
बुर्जुआ अख़बार पूँजी की विशाल राशियों के दम पर चलते हैं। मज़दूरों के अख़बार ख़ुद मज़दूरों द्वारा इकट्ठा किये गये पैसे से चलते हैं।
मज़दूरों के महान नेता लेनिन









