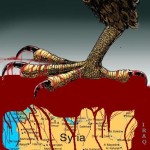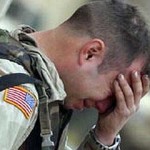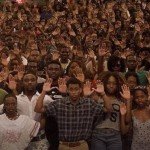अन्तर-साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा का अखाड़ा बना सीरिया
2016 में डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद की प्रमुख उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन और रिपब्लिकन पार्टी के ज़्यादातर नेता सीरिया के ऊपर “उड़ान प्रतिबंधित क्षेत्र” बनाने की तजवीज कर रहे हैं। लेकिन अमेरिकी सरकार के ज़्यादा सूझबूझ वाले राजनीतिज्ञ समझते हैं कि ऐसा करना ख़ुद अमेरिका के लिए घातक होगा क्योंकि “उड़ान प्रतिबंधित क्षेत्र” बनाने का मतलब होगा उन रूसी जहाज़ों को भी निशाना बनाना जो इस समय सीरिया में तैनात हैं, यानी रूस के साथ सीधे युद्ध में उलझना। लेकिन इस समय अमेरिका यह नहीं चाहता। फ़िलहाल वह सीरिया के तथाकथित ‘सेकुलर’ बागियों को मदद पहुँचाने तक ही सीमित रहना चाहता है। आर्थिक संकट की वजह से अमेरिका की राजनीतिक ताकत पर भी असर पड़ा है। इसलिए भी वह रूस के साथ सीधी टक्कर फ़िलहाल नहीं चाहता। अमेरिका की गिरती राजनीतिक ताकत का प्रत्यक्ष संकेत सयुंक्त राष्ट्र संघ की महासभा में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा का भाषण था। ओबामा ने अपने पहले भाषण में रूस की ओर से आई.एस.आई.एस के अलावा तथाकथित “सेकुलर” बागियों को भी मारने के लिए उसकी ज़ोरदार निंदा की। पुतिन ने भी जब अपनी बारी में सीरिया मामले पर अमेरिका की नीति की आलोचना की तो ओबामा ने अपने दूसरे भाषण में रुख बदलते हुए रूस के साथ बातचीत के लिए तैयार होने की बात कही। ओबामा ने कहा कि सीरिया के साथ किसी भी समझौते की शर्त राष्ट्रपति बशर अल-असद का अपने पद से हटना है लेकिन वह तब तक राष्ट्रपति बना रह सकता है जब तक कि इस मसले का कोई समाधान नहीं निकल आता। साथ ही ओबामा ने यह भी कहा कि नयी बनने वाली सरकार में मौजूदा बाथ पार्टी के नुमाइंदे भी शामिल हो सकते हैं। सीरिया से किसी भी तरह का समझौता नहीं करने की पोजीशन से लेकर अब उसके नुमाइंदों को नयी सरकार में मौका देने की बात करना साफ़ तौर पर अमेरिका की गिरती साख को दर्शा रहा है।