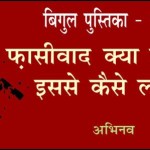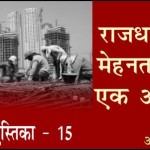कॉमरेड के ”कतिपय बुध्दिजीवी या संगठन” और कॉमरेड का कतिपय ”मार्क्सवाद”
आज के समय में असंगठित सर्वहारा वर्ग कोई पिछड़ी चेतना वाला सर्वहारा वर्ग नहीं है। यह भी उन्नत मशीनों पर और असेम्बली लाइन पर काम करता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह यह काम लगातार और किसी बड़े कारख़ाने में ही नहीं करता। उसका कारख़ाना और पेशा बदलता रहता है। इससे उसकी चेतना पिछड़ती नहीं है, बल्कि और अधिक उन्नत होती है। यह एक अर्थवादी समझदारी है कि जो मजदूर लगातार बड़े कारख़ाने की उन्नत मशीन पर काम करेगा, वही उन्नत चेतना से लैस होगा। उन्नत मशीन और असेम्बली लाइन उन्नत चेतना का एकमात्र स्रोत नहीं होतीं। आज के असंगठित मजदूर का साक्षात्कार पूँजी के शोषण के विविध रूपों से होता है और यह उनकी चेतना को गुणात्मक रूप से विकसित करता है। उनका एक अतिरिक्त सकारात्मक यह होता है कि वे पेशागत संकुचन, अर्थवाद, ट्रेडयूनियनवाद, अराजकतावादी संघाधिपत्यवाद जैसी ग़ैर-सर्वहारा प्रवृत्तियों का शिकार कम होते हैं और तुलनात्मक रूप से अधिक वर्ग सचेत होते हैं। इससे कोई इंकार नहीं कर सकता कि बड़े कारख़ानों की संगठित मजदूर आबादी के बीच राजनीतिक प्रचार की आज जरूरत है और इसके जरिये मजदूर वर्ग को अपने उन्नत तत्त्व मिल सकते हैं। लेकिन आज का असंगठित मजदूर वर्ग भी 1960 के दशक का असंगठित मजदूर वर्ग नहीं है जिसमें से उन्नत तत्त्वों की भर्ती बेहद मुश्किल हो। यह निम्न पूँजीवादी मानसिकता से ग्रसित कम्युनिस्ट क्रान्तिकारियों का श्रेष्ठताबोध है कि वे इस मजदूर को पिछड़ा हुआ मानते हैं।